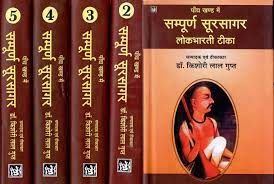“सूर-सागर” महाकवि सूरदास की प्रधान रचना है। सूर के जीवन की महानता और उनके काव्य का मूल्यांकन इसी महान् ग्रंथ द्वारा किया जा सकता है। ‘सूर-सागर’ का जो रूप इस समय उपलब्ध है उसे देखने से ज्ञात होता है कि ‘सूरसागर’ की कथा कुछ बिखरे रूप में श्रीमद्भागवत की ही भाँति स्कंधों में बँटी हुई है। पहले नौ स्कंधों और अंतिम दो स्कंधों का क्रम भागवत से बिलकुल मिलता है। ‘सूर-सागर’ में भागवत की सभी कथाओं का समावेश नहीं है और जितना है वह संक्षेप में किया गया है। कही कहीं पर साहित्यिक सौंदर्य लाने के लिए कथाओं में कुछ परिवर्तन भी कवि ने कर दिया है। नवें स्कंध में राम कथा पदों में गाई गई है और वह बहुत सुंदर काव्य है। दशम स्कंध के अतिरिक्त शेष कथा वर्णनात्मक चौपाइयों में लिखी गई है। सूर की कला का प्रदर्शन चौपाई-छंद में उतना सुंदर नहीं हो पाया जितना पदों में हुआ है। यह कथाएँ सुंदर न लिखी जाने पर भी कवि ने पुष्टिमार्ग के धार्मिक दृष्टिकोण से उन्हें लिखा है। श्रीमद्भागवत का भाषा में प्रचार करना वह अपना धर्म-कर्तव्य समझते थे। यह कथाएँ कवि ने अपनी और अपने साथियों की प्रेरणा से लिखी होंगी। ‘सूरसागर’ के दशम स्कंध के पूर्वार्ध में सुंदर वर्णनात्मक छंद मिलते हैं और यहाँ पर कहीं-कहीं कथाओं की पुनरुक्ति भी हो गई है। संभवतः कवि ने पहले इस समस्त ग्रंथ की रचना की है और बाद में जो सुंदर पद उन्होंने लिखे हैं उन्हें भी विषयानुकूल इसी ग्रंथ में रख दिया है। कुछ विद्वानों का मत है कि इस ग्रंथ में अन्य भक्त कवियों द्वारा लिखे हुए पद भी हैं। सूरदास ने खंडिता, फाग, मान आदि के जो नवीन प्रसंग लिए हैं उनका वर्णन कवि ने पदों में किया है। यह समस्त ग्रंथ सरल और मधुर ब्रजभाषा में लिखा हुआ है।
यदि साहित्यिक दृष्टि और सूरदास के महत्त्व को लेकर ‘सूर-सागर’ को देखा जाए तो ‘सूर-सागर’ के दशम् स्कध का पूर्वार्द्ध पुस्तक का सबसे महत्त्वपूर्ण भाग ठहराता है। यह भाग पदों में गाया गया है। इन पदों का पहला भाग कृष्ण की उन लीलाओं से सम्बन्धित है जिनमें उन्होंने असुरों का वध किया है। इन पदों में वर्णनात्मकता ही पाई जाती है। कवि की प्रतिभा का कोई चमत्कार नहीं दिखलाई देता। केवल कालिय-दमन और इंद्र-गर्व हरण की कुछ लीलाओं का वर्णन सुंदर है। इनके वर्णन में कवि की उच्चतम प्रतिभा का आभास मिलता है। इन कथाओं में सूरदास ने भागवत की कथाओं को ज्यों का त्यों नहीं दिया है। वरन् उनमें कलात्मक परिवर्तन किया है और उनमें सरस स्थल पैदा किए हैं। इन अलोकिक कथाओं के अतिरिक्त कृष्ण की अन्य लीलाओं में कवि ने कृष्ण की लौकिक लीलाओं का ही चित्रण किया है।
कृष्ण की जो लौकिक लीलाओं का चित्रण सूर ने किया हैं वह अमर है और उसी के आधार पर सूर को भाषा के पंडितों ने सूर्प की पदवी प्रदान की है। बाल-काल और किशोरावस्था संबंधी पद सूरदास ने अपनी मौलिक कल्पना के आधार पर लिखे हैं। इनमें भागवत से कवि ने कुछ नहीं लिया। कृष्णा का बाल-चित्रण और नन्दा, यशोदा का वात्सल्य वर्णन करने में कवि की अद्वितीय प्रतिभा प्रस्फुटित हुई है। किशोर कृष्ण की प्रेम-लीलाएँ भागवत पर कुछ अवश्य आधारित हैं परंतु उनमें भी कवि ने अपनापन पूर्ण रूप से भर दिया है। दान-लीला, मान, खंडिता, हिंडोला फाग और राधा की कल्पना यह सब सूर के मौलिक प्रसंग हैं। राधा का प्रथम मिलन, फिर वियोग और फिर मिलन यह कथा कवि ने बहुत विस्तार और सौंदर्य के साथ वर्णित की है। भागवत में तो कहीं राधा नाम भी नहीं मिलता।
‘सूर-सागर’ का भ्रमर गीत प्रसंग बहुत सुंदर है। भागवत् के भ्रमर गीत और सूर के भ्रमर गीत में आकाश-पाताल का अंतर है। भ्रमर गीत का आकार कवि ने शृंगार-शास्त्र के आधार पर खड़ा किया है। राधा-कृष्ण के प्रसंगों को लेकर कवि ने वंशी के उद्दीपन विभाव प्रस्तुत करके काफी लिखा है। वाग्वैदग्ध्य के सुंदर उदाहरण रूप-सौंदर्य और उद्धव के प्रसंगों में मिलते हैं। कवि ने मुरली और नेत्रों के प्रसंग में सुंदर कूटपद लिखे हैं।
इस प्रकार हमने देखा कि ‘सूर-सागर’ समस्त कथा भागवत से ली हुई होने पर भी उसमें मौलिकता का प्रभाव नहीं है। वल्लभाचार्य के कहने पर ही सूर-दास ने भागवत लीला का गान किया था। सूर के साहित्य में सरलता केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं है वरन् साहित्यिक सौंदर्य और प्रतिभा की भी इनमें कमी नहीं है। भ्रमर गीत, नेत्रों और मुरली के पदों में जो रूपक कवि ने प्रस्तुत किए हैं उनमें सुंदर साहित्य के दर्शन होते हैं और रीतिकाल की भीनी-भीनी महक आने लगती है। सूर ने विद्यापति की भाँति सरस पदों की रचना है, परंतु सूर की विशेषता यह है कि उसका आधार धर्म होते हुए भी उसमें विद्यापति के शृंगार से कम सरसता नहीं आ पाई। सूर ने शृंगार और रीति का आश्रय अवश्य लिया है परंतु अपने साहित्य को उनके अर्पण नहीं कर दिया है; वरन् उन्हें अपने साहित्यिक सौंदर्य में प्रभावोत्पादक बनाने के लिए प्रयोग किया है। मान और खंडिता के प्रसंग जो सूर ने लिए हैं वह लौकिक रूप में न लेकर आध्यात्मिक रूप में लिए हैं। यदि वह लौकिक रूप में लेते तो नायिका-भेद, अभिसार और परकीया जैसे रसोत्पादक विषयों को न छोड़ते। कवि ने काव्यशास्त्र का उपयोग भक्ति साहित्य में कोमलता, सरसता, माधुर्य और सौंदर्य लाने के लिए ही किया है।
सूर-सागर में राधा-कृष्ण के संयोग, रति-विलास इत्यादि का जो चित्रण मिलता है उनमें आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित करने का कवि ने प्रयत्न किया है। इसमें गीत-गोविंद की झलक आती है। सूर की गोपियों का आध्यात्मिक भावना के कारण शृंगार में कम विकास हो पाया है। सूर की गोपियाँ राधा के प्रति ईर्ष्या न करके उस पर मोहित होती हैं। यह शृंगार-काव्य की धारणा के विपरीत भाव है। ‘सूरसागर’ के यह पद फुटकर होते हुए भी कथा-बद्ध होकर चलते हैं और पाठक भी उनसे आनंद-लाभ तभी कर सकते हैं जब इसे प्रसंग से पढ़ें। इस प्रकार ‘सूर-सागर’ में गीतात्मकता और प्रबन्धा-त्मकता का ऐसा सम्मिश्रण मिलता है जैसे हिंदी के अन्य किसी काव्य में नहीं मिलता।
सूरसागर एक वृहद् ग्रंथ है परंतु इसे हम रामायण की भाँति महाकाव्य नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जीवन के विविध प्रसंगों और दृष्टिकोणों का स्पष्टीकरण नहीं मिलता। जीवन की विविध परिस्थितियों को भुलाकर केवल कुछ अंशों पर ही बल दिया गया है। परंतु जीवन के जिन भागों का चित्रण ‘सूर-सागर’ में हुआ है वह बहुत पूर्ण है। बाल चित्रण, संयोग और वियोग इन तीन जीवन की परिस्थितियों पर कवि ने इतना सुंदर लिखा है कि हिंदी का कोई अन्य कवि नहीं लिख पाया। इस प्रकार ‘सूर-सागर’ का महत्त्व हिंदी साहित्य में महान् है।