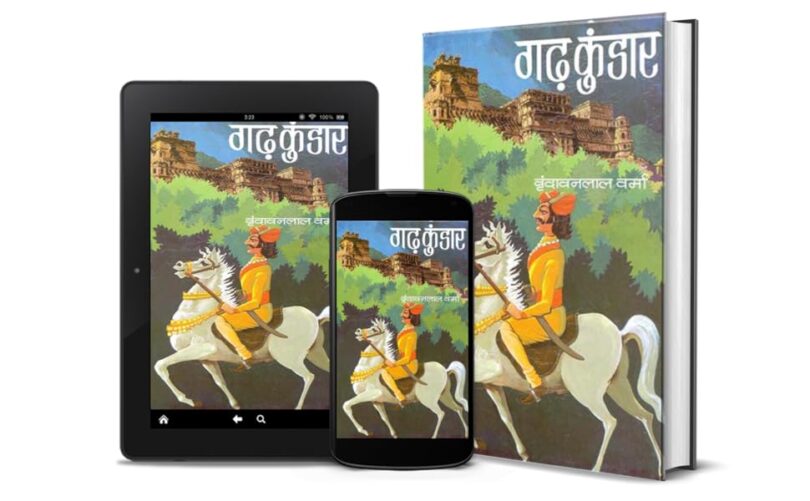वृंदावनलाल वर्मा जी के उपन्यासों में गढ़कुंडार ने विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की है, गढ़कुंडार में चौहदवीं शताब्दी के अंदर बुंदेलखंड में होने वाली राजनीतिक क्रांतियों का विवरण दिया हुआ है। वीरत्व के दुरुपयोग में किस प्रकार जुझौत के राजकुमार जूझ मरे, इसका चित्रण इस उपन्यास में है। सोहनपाल बुंदेला अपने द्वारा प्रवंचित होकर इधर इधर-उधर भटक रहा था। उसके साथ उसकी स्त्री पुत्र सहजेंद्र, पुत्री हेमवती, मंत्री और मंत्री पुत्र देवदत्त भी थे। खंगारों के राजा हुरमतसिंह के राजकुमार नागदेव ने हेमवती के सौंदर्य की कथा सुनी हुई थी। हरिचंदेल की गढ़ी में जब यह परिवार ठहरा हुआ था तो नागदेव की उनसे भेंट हुई और यहीं पर वह हेमवती पर पूर्ण रूप से आसक्त हो गया। नाग ने सोहनपाल को सहायता का आश्वासन दिया और सोहनपाल सपरिवार कुंडार चला गया। विष्णुदत्त पांडे कुंडार का शुभचिंतक ऋणदाता और उसका पुत्र अग्निदत्त नागदेव का परम मित्र था। इन सब के एक स्थान पर आ जाने से अग्निदत्त की बहन तारा दिवाकर को प्रेम करने लगी। अग्निदत्त और खंगार कुमारी मानवती में प्रेम था। मानवती का विवाह मंत्री गोपीचंद के पुत्र राजधर से ठहरा नाग ने समय पाकर हेमवती के सम्मुख अपना प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया परंतु अपने को जाति में ऊँचा समझने वाली राजकुमारी ने उसे ठुकरा दिया। जिस दिन मानवती का विवाह था उसी दिन रात्रि को अग्निदत्त अपनी बहन तारा का वेश बनाकर मानवती को भगाने के लिए उद्यत हुआ। दूसरी ओर नागदेव राजधर आदि को साथ ले हेमवती को उड़ा लेने के लिए तुल गए। दिवाकर की वीरता के कारण नाग को सफलता न मिल सकी। कुमारी को लेकर सहजेंद्र और दिवाकर कुंडार से भाग निकले। दूसरी ओर नाग ने अग्निदत्त को पहचान लिया और अंत में उसे कुंडार छोड़ना पड़ा। अग्निदत्त बुंदेलों से मिलकर बदला लेने को तैयार हुआ। बल और छल दोनों का प्रयोग किया गया। हुरमतसिंह के पास सूचना भेजी कि यदि वह सोहनपाल को सहायता का वचन दे दें तो वह अपनी पुत्री दे सकते हैं। विवाह का निश्चय हो गया और विवाह के दिन खंगार मदिरा मद में झूम उठे। जब वह नशे में मस्त थे तो बुंदेले उन पर टूट पड़े। खंगारों की शक्ति का सर्वनाश हो गया। मानवती की रक्षा करते हुए अग्निदत्त और पुण्यपाल मारे गए। सोहनपाल का मंत्री भी घायल हुआ। परंतु कुंडार पर उनका राज्य स्थापित हो गया। दिवाकर जो कि इस छल नीति का विरोधी था और बंदीगृह में पड़ा था, तारा उसे जाकर मुक्त कर देती और दोनों मिलकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। इस उपन्यास में हुरमतसिंह, नाग, सोहनपाल, धीर विष्णुदत्त, पुण्यपाल और सहजेंद्र इत्यादि ऐतिहासिक नाम हैं। सोहनपाल का अपना भाई द्वारा राज्य से निकाला जाना, विवाह आदि के प्रस्ताव, खंगारों पर मदिरा के नशे में आक्रमण करना और विजय इत्यादि करना ऐतिहासिक घटनाएँ हैं। इस उपन्यास की इस प्रकार की सभी घटनाएँ ऐतिहासिक हैं परंतु खंगार-वंश के विनाश के कारणों में मतभेद है। इस उपन्यास की प्रत्येक घटना को कल्पना का आश्रय देकर वर्मा जी ने सजीव और सुंदर बनाया है। ‘गढ़-कुंडार’ का विषय युद्ध और प्रेम है। युद्ध का जितना भी विवरण उपन्यास में आया है वह अधिकांश इतिहास से संबंधित है और रोमांचकारी प्रसंगों को वर्मा जी ने अपनी कल्पना के आधार पर प्रस्तुत किया है। नाग और हेमवती का प्रेम, अग्निदत्त और मानवती का प्रेम और तारा का दिवाकर से प्रेम इस प्रकार प्रेम की तीन धाराएँ वर्मा जी ने इस उपन्यास में प्रवाहित की है। नाग के प्रेम-स्वरूप बुंदेलों और खंगारों का युद्ध हुआ और खंगारों का सर्वनाश भी। एकपक्षीय प्रेम किस प्रकार बड़े से बड़े विनाश का कारण बन सकता है इसका यह ज्वलंत उदाहरण है। अग्निदत्त और मानवती का प्रेम दोनों पक्षों की ओर से होने पर भी मानवती के प्रेम में दुर्बलता है, दृढ़ता का अभाव है। अग्निदत्त प्रेम के उन्माद मे वेश बदलकर जाता है, अपमानित होता है, और मानवती मौन रह जाती है। यह साधारण लौकिक प्रेम है जिसमें आत्मसमर्पण की यथेष्ठ कमी दिखलाई देती है। अग्निदत्त ने तो विशुद्ध प्रेम की मर्यादा का भी उल्लंघन कर डाला है और प्रेम को दुबका चोरी का सौदा बना लिया है। दिवाकर और तारा का प्रेम आदर्श प्रेम है और दोनों पात्रों का चरित्र भी बहुत उज्ज्वल है। प्रेम दोनों पक्षों में समान रूप से उत्पन्न हुआ, पनपा और पूर्ति को प्राप्त हुआ। कर्त्तव्य-निष्ठता दोनों ओर समान है और पवित्रता भी। ‘गढ़कुंडार’ एक बड़ा उपन्यास है जिसमें कितनी ही घटनाओं का समावेश है, कुछ ऐतिहासिक और कुछ काल्पनिक। उपन्यास के प्रकरणों के नाम मुख्य पात्रों अथवा मुख्य घटनाओं के नाम पर दिए गए हैं। घटनाएँ जितनी भी इस उपन्यास में आई हैं वह सब सार्थक हैं और केवल उपन्यास का तुल बढ़ाने के लिए ही संगठित नहीं की गई हैं। घटनाओं का क्रम भी बहुत क्रमबद्ध और सुंदर है। इस उपन्यास में बुंदेलखंड के वातावरण का यथातथ्य चित्रण लेखक ने किया है। वर्मा जी ने कुछ बुंदेलखंड शब्दों का भी प्रयोग इस उपन्यास में किया है, जो उन शब्दों का सही अर्थ जानने वालों के नेत्रों के सम्मुख एक चित्र उपस्थित कर देते हैं।
यदि उपन्यास के अंत में वर्मा जी उन शब्दों की कुछ व्याख्या दे डालते तो पाठकों का पर्याप्त हित होता। जैसे ‘भरका और सड़ा’ शब्दों को पढ़कर उनका सही अर्थ समझ लेना सभी पाठकों के लिए बहुत कठिन है। ‘गढ़कुंडार में पात्रों का चरित्र चित्रण बहुत सजीव है और ‘वर्गीय पात्र तथा व्यक्तिगत पात्र’ दोनों ही प्रकार के चरित्रों को लेखक ने इसमें बहुत कलापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। बुंदेला और खंगार जातियों के प्रतिनिधि पात्र अपनी-अपनी जाति के गर्व की सभी विशेषताओं को लेकर उपन्यास में आए हैं। जाति-गौरव के सम्मुख यह पात्र मर मिटना पसंद करते हैं परंतु आन को बट्टा लगाना पसंद नहीं करते। बात की बात में रक्त वह निकलना और तलवारें खिंच जाना इनके लिए खेल है, मजाक है। बुंदेलखंडी गौरव की रक्षा के लिए ही हेमवती अग्निदत्त का प्रेम प्रस्ताव उस समय अस्वीकृत कर देती है जब कि वह और उसका समस्त परिवार, नाग का आश्रित है। इस प्रकार के वर्गीय पात्रों के प्रतीकस्वरूप हम सोहनपाल, पुण्यपाल, सहजेंद्र, हेमवती इत्यादि को ले सकते हैं। खंगारों में हुरमतसिंह यह अनुभव करता है कि वह बुंदेलों से कुछ नीचा है, इसीलिए स्थान-स्थान पर क्षत्रिय होने का दावा करता है। यह भी वर्गीयता का ही प्रमाण और उसकी विशेषता है कि वह अपने अंदर हलकापन अनुभव करता है। सोहनपाल, जबकि उसका आश्रित था, उस समय उसके घर पर आक्रमण करना, क्षत्रिय गुणों के विपरीत था। खंगारों का हलकापन इस कार्य से भी स्पष्ट हो जाता है। मानवती का प्रेम भी हलका है। खंगारों का मदिरा पीकर मस्त हो जाना और अपना सर्वनाश करा लेना भी उनके हलकेपन का ही द्योतक है। खंगारों में एक भी पात्र वर्मा जी को ऐसा नहीं जँचता जिसे कि वह पाठकों की सहानुभूति के योग्य बना डालते। व्यक्तिगत पात्रों में तारा और दिवाकर अपना विशेष स्थान रखते हैं और पुस्तक के अंत में जाकर तो वह पाठकों के विशेष आकर्षण के पात्र बन जाते हैं। इन दोनों का व्यक्तित्व बहुत ऊँचा और प्रबल है। उन पर किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का प्रभाव नहीं पड़ता और वह अपना जीवन-मार्ग स्वयं निर्धारित करते हैं। तारा त्याग की मूर्ति है और वह जातीय बंधनों से अपने को मुक्त करके दिवाकर को मुक्त कराती है। दिवाकर अपने पिता के विरुद्ध विचार रखकर कारावास की यातना सहन करना स्वीकार करता है परंतु अपने सिद्धांत से नहीं गिरता। दिवाकर अपने आदर्श का पक्का व्यक्ति है, जिसके भावुक हृदय में तारा के लिए महान् श्रद्धा और अगाध प्रेम है। तारा और दिवाकर का प्रेम विशुद्ध सात्विक और त्यागपूर्ण है। हरिचंदेल, अर्जुन कुमार और इब्न-करीम के चरित्रों का भी सुंदर विकास हुआ है। इस प्रकार उपन्यास के सभी पात्रों को लेखक ने पूर्ण विकास तक पहुँचाया है।
भारत के क्षत्रिय युग का खोखला मान अपमान, अहंकार और गौरव-गरिमा प्रवंचना की भावना का साकार चित्रण वर्मा जी ने गढ़कुंडार में किया है। व्यर्थ के जातीय अभिमान और गौरव में फँसकर मानव का रक्तपात करना और तलवारें लेकर जूझना इस इतिहास की आत्मा है। नाग का हेमवती के रूप पर रीझना स्वाभाविक ही है और अपना प्रस्ताव ठुकराए जाने पर उसे भगा ले जाने की भावना उसके हृदय में पैदा होना, खल-वृत्ति है। वह हेमवती को चोरों की भाँति हरण करने का प्रयत्न करता है। वह स्वयं विजातीय कन्या से प्रेम कर सकता है, उसे भगाने की बात भी सोच सकता है, और उसका सक्रिय प्रयत्न भी कर सकता है, परंतु अग्निदत्त और मानवती के प्रेम को सहन नहीं कर सकता। यह उसके चरित्र की सबसे बड़ी दुर्बलता है। नाग अग्निदत्त का अपमान कर डालता है और बाल-मिश्रता का भी ध्यान नहीं रखता। यदि नाग हेमवती को प्रेम कर सकता है तो क्या कारण है कि अग्नि-दत्त मानवती को प्रेम न कर सके। इस प्रकार इस उपन्यास में संकीर्ण और व्यापक दोनों प्रकार की मनोवृत्तियों को सजीव रूप दिया गया है। अग्निदत्त के रूप में प्रतिहिंसा का जो स्वरूप वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सुंदर, स्वाभाविक तथा यथार्थवादी है।
युद्धों का उपन्यास में अच्छा चित्रण है। दृश्य, संवाद और पानों की बनावट से विशुद्ध ऐतिहासिक बातावरण प्रस्तुत करने में वर्मा जी पूर्णरूपेण सफल हैं। उपन्यास के अंदर सभी चित्र बहुत सतर्कता मे किए गए हैं। यह उपन्यास वर्मा जी की हिंदी साहित्य को एक अमर देन है जिसने प्रथम होने पर भी स्थायी प्रभाव हिंदी के पाठकों पर डाला है। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य इस उपन्यास में मिलता है। इतिहास के साथ-साथ प्रेम के तीन सजीव स्वरूपों का जो चित्रण, वर्मा जी ने तीन धाराओं में प्रस्तुत किया है, वह बहुत आकर्षक है और पाठक के विशेष मनोरंजन का कारण बनता है। समस्त उपन्यास में न तो कहीं पर ऐतिहासिक तथ्यों से क्रम को ठेस लगने पाई है और न ही कठोर सत्य बनकर कहीं पर उपन्यास कोरा सूखा इतिहास मात्र बन गया है। कल्पना और सत्य को गलबहियाँ डालकर इस प्रकार नाटकीय ढंग से वर्मा जी ने चलाया है।