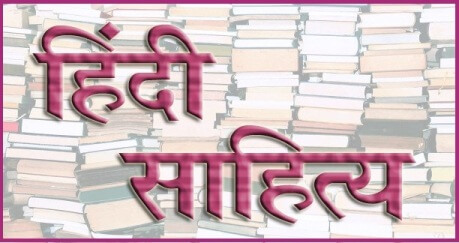साहित्य-साहित्य मानव के विचारों, भावनाओं और संकल्पों को संसार के प्रति भाषामय अभिव्यक्ति है। साहित्य वह है जिसमें अर्थ और हित दोनों निहित हों। शब्द और अर्थ, विचार और भाव दोनों का समन्वय जिस काव्य में हो वही साहित्य है। साहित्य को अंग्रेजी में लिटरेचर (Literature) और अरबी में ‘अदब’ कहते हैं। काव्य का स्थान साहित्य में बहुत ऊँचा है। साहित्य का हृदय और मस्तिष्क भी हम काव्य को कह सकते हैं।
काव्य के पक्ष-काव्य के दो पक्ष होते हैं, अनुभूत पक्ष और अभिव्यक्ति-पक्ष जिसे भाव पक्ष और कला पक्ष भी कहते हैं। काव्य में रागात्मकता, कल्पना बुद्धि और शैली का सामंजस्य होता है। कवि अपने काव्य में रागात्मकता को प्रधानता देता है क्योंकि उसके काव्य की आधारशिला अनुभूति है। कवि कल्पना द्वारा नये चित्र उपस्थित करता है और शैली द्वारा इन सब की अभि-व्यक्ति करता है शैली और रागात्मकता के संतुलन के लिए कवि बुद्धि का प्रयोग करता है। और इस प्रकार वह सफल काव्य का निर्माण कर पाता है।
काव्य की परिभाषा और आत्मा भरत मुनि और विश्वनाथ जी ने रस को काव्य की आत्मा माना है और दण्डी तथा मम्मट आचार्यों ने अलंकार को। हिंदी में आचार्य केशव ने दूसरे मत का प्रतिपादन किया है परंतु वह प्रणाली हिंदी में मान्य नहीं हुई। ‘काव्य प्रकाश’ के रचयिता मम्मटाचार्य ने ‘गुण-युक्त और दोषरहित रचना’ को काव्य कहा है, चाहे उसमें अलंकार न हों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रागात्मक तत्त्व को प्रधानता देकर लिखा है, “जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था ज्ञान-दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द-विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं।”
इस प्रकार हम काव्य की परिभाषा यह कहते हैं-“काव्य वह सरस रचना है जिसमें गुणों की प्रधानता और दोषों का अभाव हो। आवश्यकतानुसार ध्वनि और चमत्कार का भी प्रयोग उत्तम काव्य में होना चाहिए। रस वास्तव में काव्य की आत्मा है। काव्य के अंग-काव्य के आचार्यों और लेखकों ने काव्य के अनेकों भेद किए हैं। कवि अथवा लेखक अपनी अनुभूति के स्पष्टीकरण के लिए जिस मार्ग को भी अपनाता है, बस, वही काव्य का एक अंग बन जाता है। काव्य के प्रधानतया दो भेद माने गए हैं, विषय संबंधी (Subjective) जिसे गीतात्मक (Lyric) भी कह सकते हैं और दूसरा वस्तु संबंधी (Objective) जिसे प्रकथनात्मक (Narrative) कहते हैं। महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक रचनाएँ प्रकथनात्मक रचनाएँ हैं। जिस प्रकार पद्य क्षेत्र में महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक आते हैं उसी प्रकार गद्य-क्षेत्र में उपन्यास, कहानी और गद्य-काव्य आते हैं। गद्य का क्षेत्र पद्य की अपेक्षा अधिक व्यापक है इसलिए गद्य में उपन्यास, कहानी और गद्य-गीत के अतिरिक्त हमें निबंध, जीवनी इत्यादि इसके अन्य विभाग भी मिलते हैं। पद्य-क्षेत्र में इस प्रकार की रचनाएँ नहीं की जा सकती। काव्य के क्षेत्र में गद्य और पद्य सब समान रूप से आते हैं। महाकाव्य, खंडकाव्य, गद्य-गीत, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी और समालोचना के अतिरिक्त काव्य का एक और प्रधान विभाग नाटक रह जाता है। नाटक में गद्य और पद्य दोनों का सामंजस्य मिलता है। प्राचीन नाटकों में कविता की प्रधानता थी, तो वर्तमान नाटकों में गद्य की। काव्य के ऊपर दिए गए पदों के अतिरिक्त दो और भी भेद किए जाते हैं। भारतीय शास्त्रज्ञों ने काव्य-भेद श्रव्य-काव्य और दृश्य-काव्य किए हैं। श्रव्य काव्य के अंतर्गत केवल नाटक जिसे रूपक भी कहते हैं, आता है। नाटक ‘दृश्य’ और ‘श्रव्य’ दोनों के अंतर्गत समान रूप से आता है, क्योंकि इसका आनंद पढ़कर और रंगमंच पर देखकर दोनों ही प्रकार से प्राप्त होता है।
व्यक्ति प्रधान और विषय प्रधान जो ऊपर काव्य के दो भेद पश्चिमी विद्वानों ने निर्धारित किए हैं वह भी सदोष ही हैं, क्योंकि दोनों के बीच कोई निश्चित रेखा खींचना कठिन है। भावना, व्यक्ति और विषय को पृथक्-पृथक् करना कठिन कार्य है। इनका मेल इतना घनिष्ठ है कि पृथक्-पृथक् करने का प्रयास विडंबना मात्र है। कोई गीति काव्य ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका बाह्य संसार से कोई संबंध ही न हो और महाकाव्य कोई ऐसा नहीं लिखा जा सकता कि जिसमें कवि की आर्त आत्मा की भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई ही न जाती हो। इस प्रकार सीमा निर्धारित करने में केवल भाव की प्रधानता को ही महत्त्व दिया जाता है।
काव्य के आकार विषयक भेद और उनकी विशेषताएँ-आकार के आधार पर श्रव्य काव्य के तीन भेद किए जाते हैं-गद्य, पद्य और मिश्रित (चंपू)। दृश्य-काव्य में नाटक या रूपक आता है। पद्य में जहाँ संगीतात्मकता की विशेषता रहती है। वहाँ गद्य में चरित्र चित्रण और स्पष्टीकरण अधिक उत्तम रूप से किया जा सकता है। आकर्षण दोनों में किसी प्रकार कम नहीं होता। पद्य का आनंद लाभ जहाँ सब पाठक नहीं ले सकते वहीं गद्य में कहानी ने आज के युग में इतनी प्रधानता प्राप्त कर ली कि वह काव्य का सर्वप्रिय अंग बन गई है। इसका सबसे प्रधान कारण यही है कि कहानी और गद्य जीवन के अधिक निकट तक पहुँच सकते हैं। कविता जहाँ जीवन के गूढ़ रहस्य के उद्घाटन में अधिक सफल हो सकती है वहाँ उपन्यास और कहानी की साधारण नित्य के व्यवहार में आने वाली समस्याओं का स्पष्टीकरण इतने रोचक ढंग से कर सकते हैं कि पाठक उनमें अपनेपन का अनुभव करने लगता है।
प्रबंध-काव्य- प्रबंध-काव्य में तारतम्यता पाई जाती है, कथा लड़ीबद्ध रहती है, क्रम नहीं टूटता, जैसे— कामायनी।
मुक्तक-काव्य – मुक्तक-काव्य तारतम्यता, क्रमबद्धता और लड़ीबद्ध से मुक्त होकर चलता है स्वच्छंद, अबाध और मुक्त धाराओं में बिहारी सतसई, पल्लव, गूंजन, यामा, अनामिका, निशा निमंत्रण इत्यादि इसके उदाहरण है।
महाकाव्य – महाकाव्य प्रबंध-काव्य का भेद है, इसका विशाल आकार भावों की उदारता और जीवन की अनेकरूपता को लिए हुए रहता है। रामायण, कामायनी इत्यादि इसके उदाहरण हैं।
खंड-काव्य – खंड-काव्य भी प्रबंध काव्य का भेद है और इसमें जीवन के एक खंड विशेष पर कवि प्रकाश डालता है। जयद्रथ वध, पंचवटी इत्यादि इसके उदाहरण हैं।
इस प्रकार हमने काव्य का सूक्ष्म रूप से निरीक्षण करके देखा कि काव्य साहित्य का वह प्रधान अंग है कि जिसके अंतर्गत गद्य और पद्य की प्रबंध तथा मुक्तक सभी रचनाएँ आ जाती हैं। इन सभी रचनाओं की आत्मा ‘रस’ है और अलंकार, ध्वनि तथा चमत्कार उसके आकर्षण। आकर्षण और रस यही दोनों वस्तु काव्य को साहित्य का प्रधान अंग बनाऐं हुए हैं और यही काव्य की विशेषताएँ हैं। साहित्य के अंतर्गत जहाँ इतिहास, भूगोल, गणित इत्यादि सब आते हैं वहाँ काव्य के अंतर्गत केवल ललित साहित्य ही आता है।