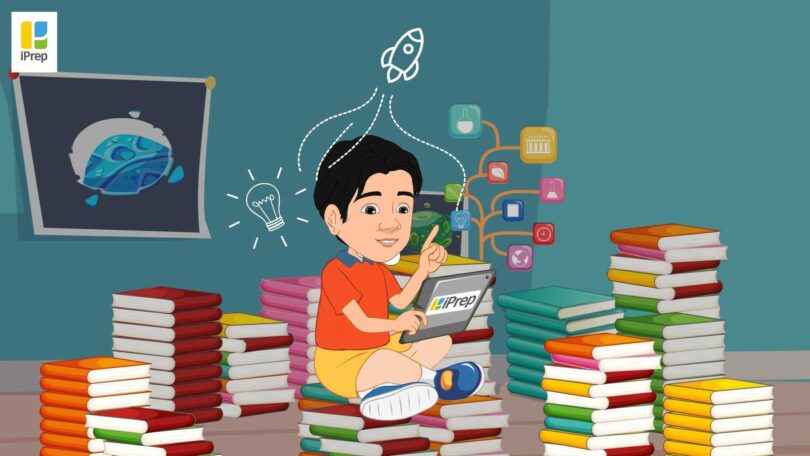संकेत बिंदु – (1) अध्ययन का महत्त्व (2) दार्शनिकों के विचार (3) अध्ययन से विवेक का जन्म और भय का अंत (4) अलौकिक ज्ञान और आनंद का स्रोत (5) अध्ययन सामग्री के अनंत रूप।
किसी विषय के सब अंगों अथवा गूढ़ तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, समझने के लिए और उस पर मनन करने के लिए अध्ययन का महत्त्वपूर्ण योगदान है। जैसे- ‘दर्शन’ को समझने में दर्शन-शास्त्र के अध्ययन का महत्त्व है। किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी विषय की सब बातों का ज्ञान, उपयोग, परिणाम, प्रभाव, मूल्य आदि की दृष्टि से औरों से बढ़कर समझे जाने में अध्ययन का महत्त्व है। जैसे – समाज की आर्थिक स्थिति का उपयोग, परिणाम, प्रभाव और मूल्य की दृष्टि से अर्थशास्त्र और वाणिज्य के अध्ययन का महत्त्वपूर्ण स्थान है।
अध्ययन से कुचिंताएँ मिट जाती हैं। संशय रूपी पिशाच भाग जाते हैं। मन में सद्भाव जाग्रत होकर परम शांति प्राप्त होती है। मनुष्य का मस्तिष्क परिष्कृत और हृदय सुसंस्कृत तथा मनोवृति उन्नत होती है।
दार्शनिक लेखक बेकन का विचार है, ‘इतिहास का अध्ययन मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। कविता वाग्विदग्ध बनाती है। गणित सूक्ष्म-चिंतक बनाता है। विज्ञान गंभीर- विचारक बनाता है। नीति-शास्त्र भी गंभीर बनाता है। तर्कशास्त्र और वक्तृत्व-कला तर्क- निपुण बनाती है।’
शरीर को पुष्ट करने के लिए जैसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, वैसे ही मस्तिष्क के विकास के लिए विभिन्न विषयों के अच्छे साहित्य का अध्ययन आवश्यक है। जितना ही हम अध्ययन करते हैं, उतना ही हमको अपने अज्ञान का आभास होता जाता है और अपनी अनभिज्ञता का बोध होता है। इसीलिए बेकन का सुझाव है ‘अध्ययन खंडन और असत्य सिद्ध करने के लिए न करो, न विश्वास करके मान लेने के लिए करो, बल्कि मनन और परिशीलन के लिए करो।’
सिसरो का मत है कि ‘प्रकृति की अपेक्षा अध्ययन से अधिक मनुष्य श्रेष्ठ बने हैं।’ डॉ. जानसन का कहना भी यही है, ‘दूसरी वस्तुएँ बल से छीनी जा सकती हैं अथवा धन से खरीदी जा सकती हैं, किंतु ज्ञान के कपाट केवल अध्ययन से ही खुलते हैं।’
अध्ययन भय की औषध है। प्रेम और प्रकाश की दृष्टि है। अज्ञान को दूर करने का साधन है। सत्य का साक्षात्कार करवाने का माध्यम है। आनंद, अलंकरण और योग्यता की पृष्ठभूमि है।
अध्ययन विवेक का जनक है, जो सभी प्रकार के कर्तव्यों में हमारा पथ-प्रदर्शन करता है। वह नीर-क्षीर की बुद्धि जागृत करता है। जीवन में सौंदर्य बिखेरता है, व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है।
अध्ययन का महत्त्व बताते हुए श्री कुलदीप नारायण लिखते हैं- ‘विविध विषयों की जानकारी होती है, अनुभव बढ़ता है। मनुष्य सभ्य और सुसंस्कृत होता हैं। समाज में प्रशंसा होती है, आदर-मान प्राप्त होता है। व्यक्तित्व उन्नत होता है। उचित-अनुचित का ज्ञान होता है। मानसिक विकास होता है। आत्मसंतोष तथा सुख की प्राप्ति होती है। मनोरंजन और मानसिक परिष्कार होता है। उच्च पद को ग्रहण कराता है। लोक में तो व्यक्ति का साथ देता है, परलोक में भी उसका साथी बनता है।‘
विश्व के विविध वाङ्मय, दर्शन-शास्त्र, विचारधाराएँ, सिद्धांत, साहित्य, कला, संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान अध्ययन के ही परिणाम हैं। इस परिणाम को ग्रहण करने के लिए भी अध्ययन की ही आवश्यकता है। अध्ययन के लिए चाहिए एकांत और एकाग्रचित्तता। एकांत में एकाग्रचित होकर जी चाहे तो वाल्मीकि के तपोवन में विचरिए या कालिदास के मेघ के साथ अलकापुरी का आनंद लूटिए। चाहे सूर के पदरूपी पंकजों पर भ्रमर बनकर मँडराते रहिए। चाहे तुलसी के ‘मानस’ में डुबकी लगाइए। चाहे शेक्सपियर के नाटकों में मानव प्रकृति को तलाशिए या मिल्टन की ज्ञान गंगा में अवगाहिए। अगणित ग्रंथों के महोदधि में जितना जितना गहरा पैठ सको, उतने ही मोती निकालते जाइए।
अध्ययन अलौकिक आनंद का स्रोत है, जिसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती। वह तो हृदय में अनुभव करने की वस्तु है। त्रैलोक्य का सौंदर्य और तीनों लोकों की संपदा उसके अंतर्गत ही रहती है। स्वाध्याय के आनंद-लोक में सत् और चित् का जब योग होता है तो सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है।
वर्तमान वैज्ञानिक युग में अध्ययन सामग्री अनंत है। सैंकड़ों समाचार-पत्र, सहस्त्रों पत्र-पत्रिकाएँ तथा पुस्तकों का तो अथाह भंडार भरा है, व्यक्ति किसका अध्ययन करे किसे छोड़े? वेंटवर्थ डिल्लन समझाते हैं, ‘Choose an author as you Choose a friend.’ अर्थात् जैसे मित्र का चयन करते हैं, उसी प्रकार लेखक का भी चयन करें। आचार्य चाणक्य सलाह देते हैं-
अनंतशास्त्रं बहुलाश्च विद्याः, अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च।
यत्सारभूतं तदुपासनीयं, हंसो यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्॥
शास्त्र अनेक हैं, विद्याएँ भी बहुत हैं, समय थोड़ा है, विघ्न भी बहुत हैं। अतएव जैसे हंस जल मिश्रित दूध में से दूध को ही ले लेता है, उसी प्रकार जो कुछ सार भूत हो, उसी को ग्रहण कर लेना चाहिए।
स्थानांग (प्राकृत ग्रंथ) का कहना है-
चत्तारि ए अवायणिज्जा
अविणीए, विगइपडिबद्धे, अविओसितपाहुडे, माई।
चार व्यक्ति शास्त्र-अध्ययन के अयोग्य हैं- अविनीत, चटोरा, झगड़ालू और धूर्त। मानव-मन में ज्ञान की ज्योति जगाकर उसे विवेकशील बनाने में अध्ययन का महत्त्व है। मानव सत्य का साक्षात्कार कर जीवन में सत्, चित् और आनंद की उपलब्धि कर सके, इसलिए अध्ययन महत्त्वपूर्ण है।