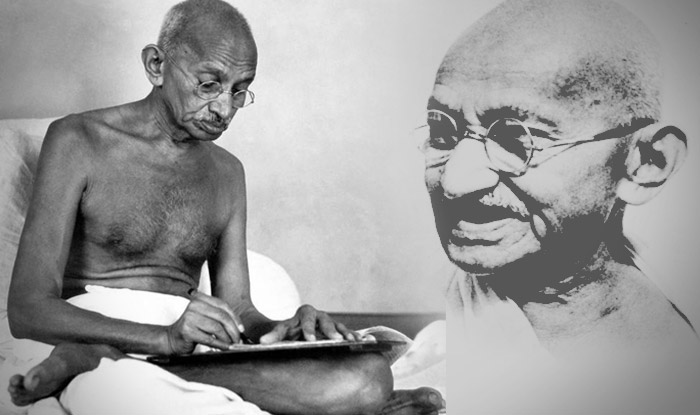आज का युग वादों का युग है, जिसमें गांधीवाद, प्रजातंत्रवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, पूँजीवाद, कम्यूनिज्मवाद, एकतंत्रवाद इत्यादि धाराओं में संसार की शासन व्यवस्थाएँ चल रही हैं। जिस प्रकार संसार के प्राचीन इतिहास में धार्मिक संघर्षों के कारण मानव सुख-चैन से नहीं सो सकता था और मध्ययुग में साम्राज्यवादियों की उथल-पुथल ने विश्व शांति को संकट में डाल दिया था, उसी प्रकार आज के युग में भी वादों का संघर्ष चल रहा है। धर्म की व्यवस्था संघर्ष के लिए न होकर शांति के लिए हुई थी परंतु परिणामस्वरूप कितना रक्तपात संसार में हुआ उन सबका उल्लेख करना यहाँ कठिन है। ठीक उसी प्रकार आज यह वाद भी अपने-अपने मूल में मानव जीवन की शांति के ही उच्चतम उद्देश्य की पूर्ति का सिद्धांत लेकर चलने का प्रदर्शन करते हैं परंतु उसका फल पारस्परिक विषमता, द्वेष, कलह और संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा।
इन वादों का जन्म कुछ देश और कालों की परिस्थितियों के फलस्वरूप हुआ है। दो वाद न तो एक देश में पनपे ही हैं और यदि दो वादों ने एक देश में जन्म भी लिया है तो काल और परिस्थितियों का परिवर्तन होना अनिवार्य है। जब-जब इन वादों ने किसी देश में जन्म लिया है तो उस समय उनका जन्म किसी भी प्राचीन व्यवस्था में सुधार के रूप में ही हुआ है। यह वाद सुधारात्मक होने से उस देश के नेताओं ने यह समझ लिया कि बस क्योंकि उस वाद ने उनके देश की समस्याओं का हल निकाल दिया इसलिए वही वाद समस्त संसार की समस्याओं का हल है, उसी मार्ग पर चलकर संसार को शांति प्राप्त हो सकती है। बस यहीं से शांति के स्थान पर संघर्ष की भावना का उदय होता है। आज संसार में जो कुछ भी संघर्षात्मक वातावरण मिल रहा है वह केवल इसलिए कि दो वादों में पारस्परिक तनाव है और प्रत्येक वाद अपने को संसार भर की समस्याओं का हल समझता है। रूस कम्यूनिज्म को मानव-समाज के लिए हितकर समझकर संसार भर में प्रचारित और प्रसारित करना चाहता है और अंग्रेज तथा अमरीकन प्रजातंत्रवाद को मानव समाज की समस्याओं का हल समझते हैं।
भारत की परिस्थिति इन तीनों देशों से भिन्न रही है। अमरीका अंग्रेजी के प्रभाव से मुक्त होकर प्रगति की ओर अग्रसर हुआ और रूस को अपने ही जोर से संघर्ष लेना पड़ा, परंतु भारत को विदेशी शासन से संघर्ष लेना था और उस संघर्ष में उसने जिस नीति को अपनाया उसे आज के राजनीतिज्ञ गांधीवाद के नाम से पुकारते हैं। गांधीवाद में महात्मा गांधी के विचार और उनके सिद्धांतों का दिग्दर्शन है। गांधीवाद के मूल में अहिंसा की भावना मिलती है और इसी अहिंसा के आधार पर गांधी जी ने अपने वाद का निर्माण किया है। अहिंसा की आत्मिक शक्ति द्वारा ही महात्मा गांधी ने संसार की प्रबलतम शक्ति से टक्कर ली। वह राजनीति में मन, कर्म और वचन की अहिंसा का समावेश करना चाहते थे और यही उन्होंने जीवनभर किया। उनकी राजनीति में छल के लिए स्थान नहीं था, कूटनीति के लिए स्थान नहीं था। उनका मत था कि हिंसा मानव को कायरता की ओर ले जाती है और अहिंसा प्रबलता की ओर, आत्म-शक्ति की ओर उनका दृढ़ विश्वास था कि स्वराज्य केवल अहिंसा की आत्मिक शक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
गांधीवाद का प्रधान गुण यह है कि वह बुराई करने वाले का शत्रु नहीं वह उस मूल बुराई का शत्रु है। पापों को पाप से मुक्त करके गांधीवाद उसे सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता है। अंग्रेजों से संघर्ष लेते हुए भी अंग्रेज-जाति के प्रति महात्मा गांधी के मन में कभी कटुता नहीं आई। गांधीवाद में विश्व प्रेम की भावना निहित है। अहिंसापूर्वक असहयोग करना ही गांधीवाद का प्रधान अस्त्र है। जिसके सम्मुख न तो तोप चल सकती है न किसी प्रकार की शारीरिक और भौतिक शक्ति।
गांधीवाद में राजनैतिक और आध्यात्मिक तत्त्वों का समन्वय मिलता है, बस यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह आध्यात्मिक तत्त्व से मुक्त होकर कोरे राजनीति के क्षेत्र में अवतीर्ण हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक ही सीमित हो गया है। भगवान से प्रेरित होकर आत्मा की शुद्धि करना गांधीवाद के लिए नितांत आवश्यक है। गांधीवाद में साम्प्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं। इसी समस्या का हल करने में महात्मा गांधी ने अपने जीवन का बलिदान दे दिया।
गांधीवाद में घरेलू धंधों का पक्षपात और बड़ी-बड़ी कलों के प्रति उदासीनता मिलती है। गांधी जी का मत था कि मशीनें मानव को बेकारी ओर घसीटती हैं। गांधी जी ने कहा भी है, “लाखों जीवित मशीनों को बेकार बनाकर निर्जीव मशीनों का प्रयोग करना मानव जाति के प्रति अनर्थ करना है।” इसलिए गांधी जी ने चर्खा संघ की स्थापना करके खद्दर को प्रोत्साहन दिया गांधी जो हस्तकला और ग्रामोन्नति के पक्षपाती थे वह भारत की आर्थिक उन्नति के मूल में ग्रामोद्योग को मानते थे।
गांधीवाद में साम्राज्यवाद और पूँजीवाद के विपरीत भावना प्रबल रूप से मिलती है। गांधी जी पूँजीपतियों द्वारा भोग-विलास और जनता के धन का अपव्यय करना महन नहीं कर सकते थे। इस प्रकार के आचरण को वह ‘चोरी’ कहते थे। गांधीवाद पूँजीवाद को मिटाना नहीं चाहता था परंतु उनको केवल कोषाध्यक्ष के रूप में देखना चाहता था।
शिक्षा के क्षेत्र में गांधीवाद के अंतर्गत मौलिक शिक्षा (Basic Educaition) आती है। मौलिक शिक्षा द्वारा गांधी जी भारत से अविद्या और दरिद्रता को भगाना चाहते थे। साथ ही गांधीवाद में छुआ-छूत और पारस्परिक घृणा के लिए कहीं पर स्थान नहीं है। गांधी जी ने हरिजन आंदोलन किया और उसके द्वारा हिंदू जाति को खंडखंड होने से बचाया। गांधीवाद ने पाश्चात्य-सभ्यता का विरोध और भारतीय सभ्यता के मूल में भारत और भारतीय समाज की मुक्ति का समावेश किया है। गांधीवाद में राजनीति, धर्म, समाज सभी कुछ आ जाते हैं। भारत के सभी क्षेत्रों पर गांधीवाद का प्रभाव हुआ है। साम्यवाद या मार्क्सवाद किसी न किसी रूप में आज संसार भर में फैला हुआ है। इटली, जर्मनी और जापान में इसका घोर विरोध हुआ परंतु इसकी प्रगति को वह न रोक सके। साम्यवाद समाजवाद की तीव्र प्रगति का दूसरा नाम है। भारत में भी आज का इसका प्रभाव स्थान-स्थान पर दिखाई देता है। संभावना गांधीवाद में भी मिलती है, परंतु अंतर केवल इतना ही है कि गांधीवाद का मूल स्रोत अहिंसा से जन्म लेकर चलता है और साम्यवाद में बोल्शेविज्म और हिंसा को भी अपनाया जा सकता है। समाजवाद में शासक का कर्तव्य है कि राष्ट्र की संपत्ति का सम विभाजन करे और राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ-न-कुछ काम पर लगाए। साम्यवाद में व्यक्ति का राष्ट्र में एकीभाव होना आवश्यक है। साम्यवाद में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यतानुकूल कार्य दिया जाता है। इस व्यवस्था में कोई निठल्ला नहीं बैठ सकता। राष्ट्र का कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति को भूखा, नंगा या किसी अभाव को अनुभव करता हुआ न देखे। कार्ल मार्क्स ने सर्वप्रथम पूँजीवाद के विरुद्ध इस बाद को जन्म दिया। मार्क्स ने संसार भर के श्रमजीवी समुदायों को संगठित करने का प्रयत्न किया। साम्यवाद पूँजीपतियों और निठल्लों का कट्टर शत्रु हैं और हड़ताल इसका प्रधान अस्त्र है। साम्यवाद के इस हड़ताल वाले प्रधान अस्त्र को कुछ अवसरों पर गांधीवाद ने भी अपनाया है और उससे गांधीवादी आंदोलनों को बल भी मिलता है। भारत में साम्यवादी नेताओं ने गांधीवादी अस्त्रों को भी अपनाया है और उसके द्वारा अपने आंदोलनों में बल प्राप्त किया है। इस वाद का प्रधान प्रचार संसार में लेनिन और ट्राटस्की द्वारा किया गया। पूँजीपति सत्ताओं ने इस शक्ति को रोकने का भरसक प्रयत्न किया है परंतु वह इसे रोकने में बराबर असफल रही हैं और वही संघर्ष आज भी चल रहा है। साम्यवाद की समस्या मानव जीवन के मूल में निहित है इसलिए इसका हल इतनी सुगमता से नहीं हो सकता। यूरोप में रूस के अतिरिक्त अन्य देशों में साम्यवाद का प्रचार हुआ। प्रारंभ में इटली में मुसोलिनी और चीन में च्यांगकाई शेक ने इसे कुचल दिया परंतु आज चीन में साम्यवाद का आधिपत्य है। फ्रांस में 1939 में महायुद्ध के पश्चात् साम्यवाद का लीडर मानशरब्लम एक बार वहाँ का शासक बन गया।
कुछ व्यक्ति साम्यवाद को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। उनका मत है कि साम्यवाद के मूल में ईर्ष्या और द्वेष की भावना निहित है। प्रतिशोध लेने के लिए यह पागल मनोवृत्ति से काम लेते हैं। इसमें संदेह नहीं कि साम्यवाद श्रेणी-युद्ध को जन्म देकर मानव संघर्ष की ओर असर करता है। गांधीवाद संघर्ष से मानव को खींचकर शांति की ओर ले जाता है, तृप्ति की ओर ले जाता है और साम्यवाद मानव में आवश्यकताओं का उदय करके उसे संघर्ष-मूलक बनाता है। साम्यवाद मानव की स्वतंत्र प्रवृत्तियों के मार्ग में बाधक बन जाता है। मानव मानव न रहकर एक मशीन का पुर्जा बन जाता है और अपनी स्वतंत्र सत्ता का सर्वनाश करके रोटी और कपड़े के ही चक्कर में फँस जाता है। वहाँ आत्मा निष्ठुर हो जाती है, मस्तिष्क स्वार्थी हो जाता है और बल द्वारा अपहरण की भावना से प्रेरित होकर मानव युद्ध और संघर्ष की ओर अग्रसर हो जाता है। साम्यवाद की भावना अपने पूर्ण विकास पर पहुँचकर एकतंत्रवाद का ही दूसरा रूप बन जाती है। इस प्रकार गांधीवाद और साम्यवाद के मूल तत्त्वों में आकाश-पाताल का अंतर है। यहाँ दोनों के मूल तत्त्वों का स्पष्टीकरण हमने इसलिए किया है कि विद्यार्थी दोनों को न समझ कर एकता की भावना का कभी-कभी समावेश दोनों में करने लगते हैं। गाँधीवाद बुद्धि-पक्ष के साथ हृदय-पक्ष का सामंजस्य करके चलता है और साम्यवाद कोरा बुद्धिपक्ष वादी है। गांधीवाद में प्राचीन के प्रति सद्भावना, सहानुभूति और सम्मान है तथा साम्यवाद में प्राचीनता के प्रति घृणा, असम्मान और उपेक्षा है। साम्यवादी कलवादी है और गांधीवाद मानववादी बस यही दोनों का मूल अंतर है। आने वाले भविष्य में जनता की रुचि साम्यवाद की ओर है, इसमें कोई संदेह नहीं परंतु भारत की वर्तमान परिस्थितियों में साम्यवाद कहाँ तक उसकी समस्याओं का हल निकाल सकता है यह प्रश्न विचारणीय है। पराधीनता के गहन गर्त से भारत को उबारकर जो वाद वर्तमान परिस्थिति तक लाया है वही भारत की समस्याओं का सही हल खोज सकता है क्योंकि भारत-राष्ट्र की गिरावटों के मूल तत्त्वों को उसी ने भली प्रकार अध्ययन किया और समझा है।