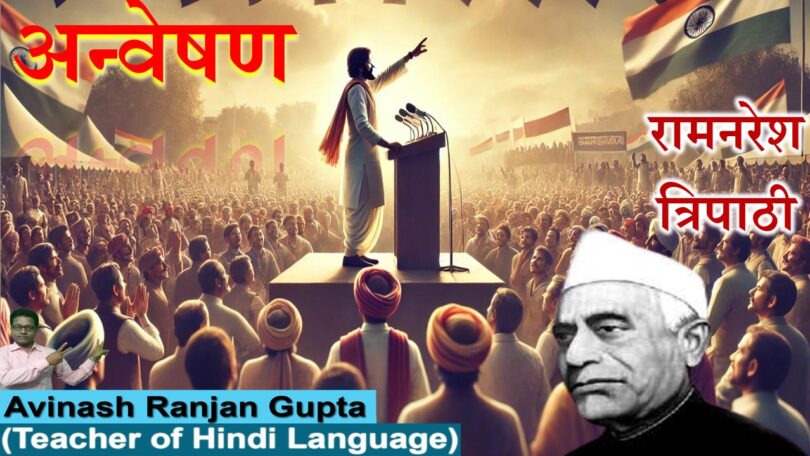अन्वेषण
मैं ढूँढता तुझे था जब कुंज और वन में,
तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में,
तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था।
मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में।
मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वारा पर तू,
मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में।
बन कर किसी के आँसू मेरे लिए बहा तू,
मैं देखता तुझे था माशूक के बदन में।
दुख से रूला-रूलाकर तुने मुझे चिताया,
मैं मस्त हो रहा था तब हाय! अंजुमन में।
बाजे बजा-बजाकर मैं था तुझे रिझाता,
तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में।
मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर,
उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में।
तू बीच में खड़ा था बेबस गिरे हुओं के,
मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में?
हरिश्चंद्र और ध्रुव ने कुछ और ही बताया,
मैं तो समझ रहा था तेरा प्रताप धन में।
तेरा पता सिकन्दर को मैं समझ रहा था।
पर तू बसा हुआ था फ्ररहाद कोहकन में
क्रीसस की “हाय” में था करता विनोद तू ही,
तू ही विहँस रहा था “महमूद” के सदन में।
प्रहलाद जानता था तेरा सही ठिकाना,
तूही मचल रहा था सुहराब पील-तन में।
कैसे तुझे मिलूँगा जब भेद इस कदर है?
हैरान होके भगवन। आया हूँ मैं सरन में।
तू रूप है किरन में सौन्दर्य है सुमन में,
तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में।
ज्ञान हिन्दुओं में, ईमान मुसलिमों में,
विश्वास क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में।
हे दीनबन्धु। ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू,
देखूँ तुझे-दृगों में, मन में तथा बचन में।
कठिनाइयों, दुखों का इतिहास ही सुयश है,
मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में।
दुख में न हार मानूँ, सुख में तुझे न भूलूँ
ऐसा प्रभाव भर दे, मेरे अधीर मन में।
रामनरेश त्रिपाठी (1881-1962) मैथिली शरण गुप्त की ‘भारत भारती’ की भाषा और अभिव्यक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए थे। इसी प्रभाव के फलस्वरूप उन्होंने खड़ीबोली में लिखना शुरू किया था। उन्होंने राष्ट्रप्रेम की कविताएँ लिखीं। इन्होंने कविता के अलावा उपन्यास, नाटक आलोचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखीं। इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं- मिलन, स्वप्न, पथिक तथा मानसी। इनमें ‘मानसी’ फुटकर कविताओं का संग्रह है और शेष तीनों कृतियाँ प्रेमाख्यानक खंडकाव्य हैं। रामनरेश त्रिपाठी ने लोक गीतों के चयन के लिए सारे देश का भ्रमण किया। इनकी कविताओं के मुख्यतः दो विषय हैं- देशभक्ति और निर्धन जनता के प्रति सहानुभूति। उनकी कविताओं में राजभक्ति का अभाव तो है ही, तत्कालीन शासन व्यवस्था के प्रति तीव्र व्यंग्य भी परिलक्षित होता है।
कविता परिचय
पंडित रामनरेश त्रिपाठी की कविता ‘अन्वेषण’ परतंत्र भारत में आमजन में देश भक्ति अथवा राष्ट्र प्रेम की भावना उद्बुद्ध करना इसका मुख्य ध्येय था। इस संदर्भ में रामनरेश त्रिपाठी के महत्त्व को आप समझ सकते हैं। भारतीय प्रकृति, खेत, खलिहान, संपदा, इतिहास, संस्कृति एवं इतिहास – पुरुषों की स्मृति एवं प्रशस्ति में लिखी गई कविताओं में कवि की अनन्यता को भी आप रेखांकित कर सकते हैं। आपने यह भी समझा कि युगीन परिवेश में भटके लोगों को कवि ने किस खूबी से सन्मार्ग दिखाया और पथ-प्रदर्शक की भूमिका निभाई है।
01
मैं ढूँढता तुझे था जब कुंज और वन में,
तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में,
तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था।
मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में।
मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वारा पर तू,
मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में।
बन कर किसी के आँसू मेरे लिए बहा तू,
मैं देखता तुझे था माशूक के बदन में।
शब्दार्थ –
ढूँढता – खोजता
कुंज – बाग़, उपवन
वन – जंगल
खोजता – तलाश करता
दीन – निर्धन, गरीब
वतन – देश, स्थान
आह – करुण पुकार, दुखभरी आवाज़
पुकारता – बुलाता
संगीत – संगीत, मधुर ध्वनि
भजन – ईश्वर की स्तुति में गाया जाने वाला गीत
दुखियों – दुखी, पीड़ित लोग
द्वार – दरवाज़ा
बाट जोहना – प्रतीक्षा करना
चमन – बाग़, बगीचा
बन कर – रूप धारण करके
आँसू – अश्रु, दुख या खुशी की बूँदें
माशूक – प्रेमिका, प्रियजन
बदन – शरीर
संदर्भ और प्रसंग –
उपर्युक्त पंक्तियों में कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने यह कहना चाहा है कि मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को न खोजकर बाहर वन और उपवन में खोजता रहता है, जबकि परमात्मा स्वयं दीन-दुखियों के लोक में मानव की खोज करता रहता है।
व्याख्या –
कवि कहते हैं कि परमात्मा किसी गरीब दुखी की आह में बसते हैं, जब वह हमसे मदद की गुहार लगाते हैं, जबकि हम उन्हें संगीत भजन के माध्यम से याद करते रहते हैं। परमात्मा जब दुखियों के दरवाजे पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम अपने मानव होने का परिचय देंगे और गरीबों की मदद करेंगे तब हम उसकी प्रतीक्षा किसी बगीचे या उपवन में कर रहे थे। परमात्मा किसी के आँसू में करुणा का प्रतिरूप बनकर हमारे समक्ष प्रकट हुए, जबकि मनुष्य उसे प्रेमिका के शरीर में देख रहा था। कहना न होगा कि कवि लैला-मजनू के प्रेम प्रसंग की ओर संकेत कर रहे हैं, जबकि परमात्मा का मानव के प्रति प्रेम अशरीरी और अलौकिक है। कवि का ऐसा मानना है कि परमात्मा हमें हमसे अधिक प्रेम करते हैं। उसे स्वयं के भीतर अन्वेषित (खोजा) किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर हमें उन्हें किसी स्थान विशेष पर खोजने जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। वह इस सृष्टि के अणु-अणु में विद्यमान है। उसके लिए आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पंक्तियाँ यह संदेश देती है कि परमात्मा की सच्ची खोज बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर की संवेदनाओं और करुणा में होती है। वह गरीबों, पीड़ितों, दुखियों की मदद में है, न कि केवल धार्मिक कर्मकांडों और सौंदर्य में।
विशेष –
- उपर्युक्त पंक्तियों का साम्य निम्नलिखित पंक्तियों से देखा जा सकता है- “मोको कहाँ
ढूँढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे।”
- कवि ने ‘बाट जोहना’ कहावत का प्रयोग सुंदर तरीके से किया है।
- कवि ने तत्सम शब्दों के साथ विदेशज शब्दों का कहीं-कहीं मेल कराया है, जो द्विवेदी युग की काव्य-भाषा विषयक शुष्कता से उन्हें किंचित पृथक ठहराता है।
- इसके अलावा पूरी कविता में अंत्यानुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है।
02
दुख से रूला-रूलाकर तुने मुझे चिताया,
मैं मस्त हो रहा था तब हाय! अंजुमन में।
बाजे बजा-बजाकर मैं था तुझे रिझाता,
तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में।
मैं था विरक्त तुझसे जग की अनित्यता पर,
उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में।
तू बीच में खड़ा था बेबस गिरे हुओं के,
मैं स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरण में?
शब्दार्थ –
दुख – पीड़ा, कष्ट
रूला-रूलाकर – बहुत अधिक रुलाकर, दुख देकर
चिताया – ध्यान दिलाया, जागरूक किया
मस्त – आनंद में डूबा हुआ
हाय! – अफ़सोस, दुख का भाव
अंजुमन – सभा, समाज, महफ़िल
बाजे – संगीत वाद्ययंत्र
रिझाना – खुश करना, लुभाना
पतितों – गिरे हुए लोग, नैतिक रूप से कमजोर लोग
संगठन – समूह, समाज
विरक्त – संसार से विमुख, संन्यासी भाव में
अनित्यता – नश्वरता, अस्थिरता
उत्थान – ऊँचाई, सुधार
पतन – गिरावट, नैतिक पतन
बेबस – असहाय
गिरे हुए – पराजित, दुखी लोग
स्वर्ग – स्वर्गलोक, आनंदमय स्थान
चरण – पैर (ईश्वर के प्रति श्रद्धा का प्रतीक)
संदर्भ और प्रसंग –
उपर्युक्त पंक्तियों में कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने यह कहना चाहा है कि मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को न खोजकर बाहर वन और उपवन में खोजता रहता है, जबकि परमात्मा स्वयं दीन-दुखियों के लोक में मानव की खोज करता रहता है।
व्याख्या –
उपर्युक्त पंक्तियों में कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने यह कहना चाहा है कि दुख में रुला- रुलाकर परमात्मा ने ही मानव को जागृत किए रखा है जबकि मनुष्य तब अपनी मजलिस जुटाने में व्यस्त था अर्थात् तरह-तरह के दावतों और महफिलों की ख्वाइशें पाले हुए था। यह मानव को करुणा के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रश्न भी है। मानव जब वाद्य यंत्रों को बजा-बजाकर परमात्मा को प्रसन्न करने की जुगत भिड़ा रहा था, तब परमात्मा पतितों-दलितों के त्राण में जुटे हुए थे। मानव जब जग की अस्थिरता या क्षणभंगुरता के प्रति उदासीनता का अनुभव कर रहा था, तब भी परमात्मा उनके पतन के मध्य उत्थान के बारे में सोच रहे थे। परमात्मा जब जीवन में हारे हुए लोगों के बीच आशा की किरण बनकर आविर्भूत हुए थे, तब भी मानव उसके स्वर्ग में होने की उम्मीद कर रहा था। वह यही सोच रहा था कि स्वर्ग में कैसे उस तक पहुँचा जाए या कि स्वर्ग को कहाँ खोजा जाए।
विशेष:
- ‘बाजे बजा-बजाकर’ में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है।
- ‘बजा-बजाकर’ में पुनरुक्तिप्रकाश अलंकार की छटा दर्शनीय है।
- उपर्युक्त पंक्तियों में कवि का इहलौकिक दृष्टिकोण दर्शनीय है।
- कवि ने तत्सम शब्दों के साथ विदेशज शब्दों का कहीं-कहीं मेल कराया है, जो द्विवेदी युग की काव्य-भाषा विषयक शुष्कता से उन्हें किंचित पृथक् ठहराता है।
- इसके अलावा पूरी कविता में अंत्यानुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है।
03
हरिश्चंद्र और ध्रुव ने कुछ और ही बताया,
मैं तो समझ रहा था तेरा प्रताप धन में।
तेरा पता सिकन्दर को मैं समझ रहा था।
पर तू बसा हुआ था फरहाद कोहकन में
क्रीसस की “हाय” में था करता विनोद तू ही,
तू ही विहँस रहा था “महमूद” के सदन में।
प्रहलाद जानता था तेरा सही ठिकाना,
तूही मचल रहा था सुहराब पील-तन में।
शब्दार्थ –
हरिश्चंद्र – सत्य और त्याग के लिए प्रसिद्ध राजा
ध्रुव – भक्ति और अडिग निष्ठा के प्रतीक बालक
प्रताप – प्रभाव, महिमा
धन – संपत्ति, ऐश्वर्य
सिकंदर – महान विजेता (Alexander the Great)
फरहाद – प्रेम और बलिदान के प्रतीक पात्र (प्रसिद्ध प्रेमी, जिसने अपनी प्रेमिका शीरीं के लिए पहाड़ काटा)
कोहकन – पहाड़ काटने वाला (फरहाद के संदर्भ में)
क्रीसस – एक अत्यंत धनी राजा, जिसने बाद में अपनी दौलत खो दी और दुखी हुआ
हाय – आह, दुःख भरी पुकार
विनोद – आनंद, खेल
विहँस – मुस्कुराना, हँसना
महमूद – महमूद गजनवी, एक प्रसिद्ध आक्रमणकारी राजा
सदन – महल, निवास
प्रह्लाद – ईश्वर के प्रति निष्ठा और भक्ति के प्रतीक (हिरण्यकश्यप के पुत्र, जिन्होंने ईश्वर में विश्वास रखा)
ठिकाना – निवास स्थान
मचलना – व्याकुल होना, अधीर होना
सुहराब – एक महान योद्धा (फिरदौसी के शाहनामे का पात्र)
पील-तन – हाथी जैसा मजबूत शरीर, योद्धा का प्रतीक
संदर्भ और प्रसंग –
उपर्युक्त पंक्तियों में कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने यह कहना चाहा है कि मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को न खोजकर बाहर वन और उपवन में खोजता रहता है, जबकि परमात्मा स्वयं दीन-दुखियों के लोक में मानव की खोज करता रहता है।
व्याख्या –
उपर्युक्त पंक्तियों में कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने यह कहना चाहा है कि राजा हरिश्चंद्र और ध्रुव की कथा यह संदेश देती है कि सत्य और निस्वार्थ भक्ति से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। उसकी अनुकंपा को धन-संपदा से जोड़कर देखना अनुचित है। लेकिन मानव ईश्वर की कल्पना विश्व विजेता सिकंदर की तरह करता है, जबकि ईश्वर तो फरहाद की तरह पहाड़ खोदकर नहर निकालने को ही श्रेयस्कर समझ रहा था। परमात्मा यीशू की ‘हाय’ में विद्यमान था क्योंकि उन्होंने सारे संसार का अपराध स्वयं में धारण कर लिया, जबकि उन्हें शूली पर चढ़ा दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने संसार के सारे अपराधों को क्षमा कर दिया। परमात्मा ही इस संसार रूपी स्तुत्य सदन में विहँस रहा था। कवि का यह भी मानना है कि महमूद जब पृथ्वीराज को अपने साथ बंदी बनाकर ले गया था तब पृथ्वीराज चौहान के रूप में आप ही शौर्य प्रदर्शन कर रहे थे। कवि यह कहना चाहते हैं कि भक्त प्रहलाद परमात्मा का सही ठिकाना जानते थे क्योंकि परमात्मा उनके मन में ही थे। इसके अलावा परमात्मा ही सुहराब जो एक महान योद्धा (फिरदौसी के शाहनामे का पात्र) थे उसके तन में बसते थे क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने युद्ध किया था। कहना न होगा कि कवि यह संकेत कर रहे हैं कि परमात्मा हमारे मन में ही विद्यमान हैं। यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध है तो वह हमारे समीप ही हैं।
विशेष –
- कवि ने तत्सम शब्दों के साथ विदेशज शब्दों का कहीं-कहीं मेल कराया है, जो द्विवेदी युग की काव्य-भाषा विषयक शुष्कता से उन्हें किंचित पृथक् ठहराता है।
- उपर्युक्त पंक्तियों का साम्य निम्नलिखित पंक्तियों से देखा जा सकता है- “मोको कहाँ ढूँढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे।”
- इसके अलावा पूरी कविता में अंत्यानुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग का भी हुआ है।
- सिकंदर, क्रीसस और महमूद जैसे ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से यह बताया गया है कि केवल विजय, धन, और महलों में ईश्वर नहीं रहता, बल्कि वह फरहाद के बलिदान, प्रह्लाद की भक्ति और सुहराब की वीरता में भी बसता है।
04
कैसे तुझे मिलूँगा जब भेद इस कदर है?
हैरान होके भगवन। आया हूँ मैं सरन में।
तू रूप है किरन में सौन्दर्य है सुमन में,
तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में।
ज्ञान हिन्दुओं में, ईमान मुसलिमों में,
विश्वास क्रिश्चियन में, तू सत्य है सुजन में।
शब्दार्थ –
भेद – अंतर, मतभेद
कदर – सीमा, हद
हैरान – आश्चर्यचकित
भगवन – ईश्वर
सरन (शरण) – आश्रय, शरण
रूप – सौंदर्य, स्वरूप
किरण – रोशनी, प्रकाश की किरण
सौन्दर्य – सुंदरता
सुमन – फूल
प्राण – जीवन
पवन – हवा, वायु
विस्तार – फैलाव, अनंतता
गगन – आकाश
ज्ञान – विद्या, सत्य की समझ
हिन्दू – हिंदू धर्म को मानने वाले
ईमान – सच्चाई, धार्मिक निष्ठा
मुसलिम – इस्लाम धर्म को मानने वाले
विश्वास – श्रद्धा, भरोसा
क्रिश्चियन – ईसाई धर्म को मानने वाले
सत्य – सच, ईमानदारी
सुजन – सज्जन व्यक्ति, नेक इंसान
संदर्भ और प्रसंग –
उपर्युक्त पंक्तियों में कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने यह कहना चाहा है कि मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को न खोजकर बाहर वन और उपवन में खोजता रहता है, जबकि परमात्मा स्वयं दीन-दुखियों के लोक में मानव की खोज करता रहता है।
व्याख्या –
उपर्युक्त पंक्तियों में कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने यह कहना चाहा है कि जब इस संसार में इतना भेद-वैषम्य है तो ईश्वर की शरण में जाने के अलावा और कहाँ जाया जा सकता है। ईश्वर रूप-किरण है। वही सुमन के सौंदर्य में बसता है। वह प्राण वायु के समान है तथा आकाश के समान अनंत है। वही हिंदुओं की चेतना, मुसलमानों का ईमान, ईसाइयों का विश्वास और सुजन अर्थात् सज्जनों का सत्य है।
कवि कहते हैं कि जब इतने भेदभाव (मतभेद, जात-पात, सांप्रदायिकता) हैं, तो वह ईश्वर से कैसे मिल सकते है? इस उलझन में वह थककर ईश्वर की शरण में आ गए हैं। यह भेदभाव केवल धार्मिक या सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मौजूद असमानताओं और पूर्वाग्रहों की ओर भी इशारा करता है। ईश्वर प्रकाश की किरण रूप में, फूलों में सौंदर्य, हवा में जीवन और आकाश में विस्तार के रूप में मौजूद हैं। इसका अर्थ है कि ईश्वर केवल मंदिर, मस्जिद, चर्च में सीमित नहीं है, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुसलमानों में, विश्वास ईसाइयों में और सत्य सज्जनों में है। इसका अर्थ है कि हर धर्म में कुछ न कुछ अच्छाई है और सभी धर्मों के मूल सिद्धांत मिलकर ईश्वर के स्वरूप को दर्शाते हैं।
विशेष –
- कवि ने तत्सम शब्दों के साथ विदेशज शब्दों का कहीं-कहीं मेल कराया है, जो द्विवेदी युग की काव्य-भाषा विषयक शुष्कता से उन्हें किंचित पृथक् ठहराता है।
- उपर्युक्त पंक्तियों का साम्य निम्नलिखित पंक्तियों से देखा जा सकता है-
“दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय।”
- इसके अलावा पूरी कविता में अंत्यानुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है।
05
हे दीनबन्धु। ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू,
देखूँ तुझे-दृगों में, मन में तथा बचन में।
कठिनाइयों, दुखों का इतिहास ही सुयश है,
मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में।
दुख में न हार मानूँ, सुख में तुझे न भूलूँ
ऐसा प्रभाव भर दे, मेरे अधीर मन में।
शब्दार्थ –
हे दीनबंधु – हे गरीबों और दुखियों के मित्र (ईश्वर का संबोधन)
प्रतिभा – ज्ञान, दिव्य दृष्टि, विशेष योग्यता
प्रदान – देना, प्रदान करना
दृग – नेत्र, आँखें
मन – हृदय, आत्मा
बचन (वचन) – शब्द, वाणी
कठिनाइयाँ – मुश्किलें, समस्याएँ
दुख – पीड़ा, कष्ट
इतिहास – बीती घटनाएँ
सुयश – महानता, सफलता की प्रसिद्धि
समर्थ – सक्षम, योग्य
सहन – सहना, झेलना
हार मानना – पराजय स्वीकार करना
प्रभाव – शक्ति, असर
अधीर – बेचैन, अस्थिर
संदर्भ और प्रसंग –
उपर्युक्त पंक्तियों में कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने यह कहना चाहा है कि मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को न खोजकर बाहर वन और उपवन में खोजता रहता है, जबकि परमात्मा स्वयं दीन-दुखियों के लोक में मानव की खोज करता रहता है।
व्याख्या –
कवि परमात्मा, जो गरीब नवाज है, से यह प्रार्थना करते हैं कि वह उसे ऐसी प्रतिभा प्रदान करें कि कवि उसे (परमात्मा को) अपने मन, वचन और अपनी आँखों में बसा लें। कवि यह वरदान माँगते हैं कि वह कष्ट सहन करने में सक्षम बने क्योंकि जिसने जीवन में कठिनाइयाँ और दुख नहीं देखा, वह छोटी-सी समस्याओं से भी घबरा जाते हैं। कवि यह इच्छा रखते हैं कि परमात्मा उसके अधीर मन को ऐसा बना दें कि वह दुख में कभी न हारे और सुख में भी परमात्मा को याद करें। आलोच्य पंक्तियों में कवि ने ईश्वर को लेकर किए जाने वाले अंधविश्वास और बाह्याचारों का विरोध किया है।
विशेष –
- कवि ने तत्सम शब्दों के साथ विदेशज शब्दों का कहीं-कहीं मेल कराया है, जो द्विवेदी युग की काव्य-भाषा विषयक शुष्कता से उन्हें किंचित पृथक् ठहराता है।
- यह कविता आत्मबल, धैर्य और ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने की प्रार्थना है।
- यह संदेश देती है कि हमें कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सहने की शक्ति माँगनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे चरित्र को महान बनाता है।
यह कविता लोक कला की शक्ति को प्रकट करती है।
सभ्य समाज लोक कला से दूरी रखना चाहता है, मगर उसकी शक्ति से अप्रभावित नहीं रह सकता है।
आज भी लोक धुन पर आधारित गीतों को व्यापक लोकप्रियता मिलती है। कई बार तो शहरी समाज जानता भी नहीं है कि वह जिस धुन को पसंद कर रहा है उसके मूल में कोई लोक धुन है।
25, 24 और 21 मात्राओं की तीन-तीन पंक्तियों के क्रम से इस कविता का निर्माण हुआ है। पूरी कविता में तीन-तीन पंक्तियों के कुल तीन चरण हैं।
केदारनाथ अग्रवाल ने लोक जीवन के संगीत की शक्ति को मनोहर रूप में व्यक्त किया है। उनका ख्याल है कि प्रकृति के करीब रहने वाला जन-जीवन अपने स्वभाव से इतना आत्मीय होता है कि वह दूसरों के मन तक पहुँचने की अपार क्षमता रखता है।
लोकगीत का महत्त्व
भारत में कई लोकगीत अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं, जो विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों में अपनी अलग पहचान रखते हैं। ये गीत जीवन, प्रेम, प्रकृति, पर्व, संघर्ष, भक्ति और विरह के भावों को व्यक्त करते हैं।