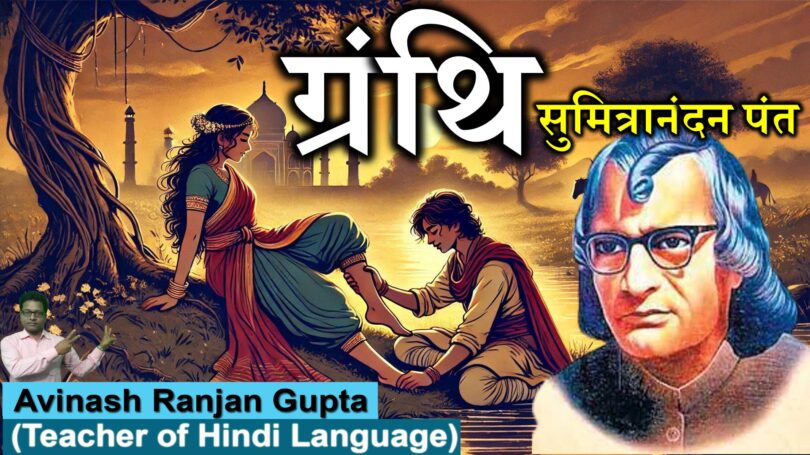पंत जी की प्रारंभिक रचनाएँ हैं – ‘ग्रंथि’, ‘वीणा’ और ‘पल्लव’। परंतु ‘ग्रंथि’, ‘उच्छ्वास’ और ‘आँसू’ एक ही प्रेम-काव्य के तीन खंड समझे जाएँगे। ‘ग्रंथि’ में इस खंड-काव्य की कथावस्तु मिलेगी, ‘उच्छ्वास’ और ‘आँसू’ में प्रेम के दुखांत होने पर भावुकताप्रधान प्रलाप। इन तीनों रचनाओं का ऐतिहासिक महत्त्व भी है। अब तक व्यक्तिगत रूप से दुख-सुख, मिलन-वियोग की कहानी हिंदी में किसी भी कवि ने नहीं लिखी थी। बाद में ‘मिलन’ और ‘पथिक’ जैसे प्रेम-काव्य सामने आए। प्रेम का भावुकता-प्रधान रोमांटिक रूप इन्हीं तीन कविताओं द्वारा पहली बार हिंदी में उपस्थित हुआ और पाठक उसमें बह गए। यह प्रेम-कथा किसी भी प्रकार विचित्र और असाधारण नहीं कही जा सकती। इसकी महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि कवि ने एक प्रणयगाथा को संक्षिप्त, रोचक तथा सरस अभिव्यक्ति दी है।
‘ग्रंथि’ कविता की कथा का प्रणयगाथा इस प्रकार है : उस समय कवि किशोर थे। संध्याकालीन प्राकृतिक सुषमा में सम्मोहित नायक नाव में सरोवर की सैर कर रहे थे, अचानक किसी भँवर में पड़ कर उनकी नौका डूब जाती है। जब उनकी आँखें खुली तो उन्होंने देखा, एक पर्वतीय बालिका की जंघा पर उनका सिर है और वह सेवोपचार कर रही है। यहीं से प्रथम दर्शन वाले प्रेम का प्रारंभ हो गया है। इस प्रेम के विकास की कथा ही ‘ग्रंथि’ की कथा है। किसी सामाजिक कारण से प्रेमी-प्रेमिका परिणय सूत्र में नहीं बँध सकते थे। कदाचित् प्रेमिका किसी कारणवश प्रेमी पर संदेह भी करने लगती है। इसी से इस प्रेम का अंत हो जाता है। इस थोड़े-से कथानक के आधार पर कवि ने भावुकता का रंगमहल खड़ा करने का प्रयत्न किया है। कवि की आँखों के सामने ही उसकी प्रेमिका का किसी अन्य से ग्रंथि बंधन हो गया। इस पर कवि कहते हैं –
हाय! मेरे सामने ही प्रणय का
ग्रंथिबंधन हो गया, वह नव कमल
मधुप सा मेरा हृदय लेकर, किसी
अन्य मानस का विभूषण हो गया !
पाणि ! कोमल पाणि ! निज बंधूक की
मृदु हथेली में सरल मेरा हृदय
भूल से यदि ले लिया था, तो मुझे
क्यों न वह लौटा दिया तुमने पुनः?
प्रणय की पतली अँगुलियाँ क्या किसी
गान से विधि ने गढ़ीं? जो हृदय को
याद आते ही, विकल संगीत में
बदल देतीं हैं भुला कर, मुग्ध कर!
‘उच्छ्वास’ की कुछ पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि प्रेमी प्रेमिका के बीच में व्यवधान लाने वाला कारण संदेह था। इसी से कवि कहते हैं-
मर्म-पीड़ा के हास!
रोग का है उपचार,
पाप का भी परिहार,
है देह सन्देह, नहीं है
इसका कुछ संस्कार।
हृदय की है यह दुर्बल हार!
कवि ने अनेक सुंदर उक्तियों के सहारे संदेह को धिक्कारा है परंतु कविता की महत्ता उस प्रकृति-वीथिका में है जिसमें कवि ने अपनी कथा-वस्तु को सजाया है। पर्वत प्रदेश की क्षण-क्षण परिवर्तित प्रकृति के बीच कवि के प्रेम ने जन्म लिया। बाह्य प्रकृति की तरह ही बालिका उसकी मनोरमा मित्र बन गई, परंतु यह मित्रता अधिक दिनों तक निभ नहीं सकी। सन्देह ने उसका अंत कर दिया और कवि एक जीवित समाधि बन गया।
इस प्रकार हम देखते हैं कि। ‘उच्छ्वास’, ‘आँसू’ और ‘ग्रंथि’ एक ही शृंखला की तीन कड़ियाँ हैं।
‘वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान
बहकर चुपचाप आँखों से, निकली होगी कविता अनजान।
– यह कवि ने स्वयं लिखा है। उसकी रचनाएँ इस तथ्य को चरितार्थ करती हैं।
इस संक्षिप्त प्रणय-गाथा को पंत जी ने एक वचन उत्तम पुरुष में लिखा है। स्वानुभूतिपरक उक्तियों, भावात्मकता और अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता देखकर कतिपय आलोचकों का यह मत है कि ‘ग्रंथि’ केवल काल्पनिक नहीं, अपितु इसमें कवि के वैयक्तिक जीवन की वास्तविकता अभिव्यक्त हुई है। डॉ. नगेन्द्र ने उक्त मत की आलोचना इस प्रकार की है – “बहुतों से सुना कि ग्रंथि पंत जी के अपने अनुभव पर आधृत है, उसमें उन्होंने अपनी प्रणय-कहानी लिखी है। वास्तव में इस लेख का लेखक कवि के आंतरिक जीवन के इतने निकट नहीं है कि इस विषय में कुछ निश्चयपूर्वक कह सके और न किसी के व्यक्तिगत जीवन की चर्चा श्लाघ्य है। हाँ, इतना अवश्य प्रतीत होता है कि उनकी ‘उच्छ्वास’, ‘आँसू’ और ‘ग्रंथि’ – ये तीन कविताएँ किसी विशेष प्रेरणा भार से दबकर लिखी हुई हैं और इनमें आत्म जीवन संबंधी कुछ स्पर्श अवश्य है।” वास्तव में यह कवि के यौवन काल की रचना है। उस काल में प्रेम-सौंदर्य आदि के प्रति आकर्षण स्वाभाविक हो सकता है।
किंतु साहित्य जगत् में प्रत्येक कृति व्यक्ति-विशेष के जीवन तक सीमित नहीं रहती। अतः ‘ग्रंथि’ का अध्ययन करते हुए हमें पंत जी के रूप-सौंदर्य को प्रमुखता देनी चाहिए। खंड काव्य का-सा कथानक लेकर भी पंत ने उसे गीति काव्य के रूप में चित्रित करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है।
वह मधुर मधु मास था, जब गंध से
मुग्ध होकर झूमते थे मधुप दल;
रसिक पिक से सरस तरुण रसाल थे,
अवनि के सुख बढ़ रहे थे दिवस-से।
जानकर ऋतुराज का नव आगमन
अखिल कोमल कामनाएँ अवनि की
खिल उठी थीं मृदुल सुमनों में
कई सफल होने को अवनि के ईश से।
शब्दार्थ –
मधुमास, ऋतुराज = वसंत। मुग्ध = मोहित। रसिक = रस लेने वाला। तरुण = युवक। अवनि = पृथ्वी। मृदुल = कोमल।
प्रसंग –
‘ग्रंथि’ की प्रणय-गाथा को प्रारंभ करने से पूर्व कवि पंत ने उसे प्राकृतिक सौंदर्य की भूमिका देने के लिए वसंत के सौंदर्य का चित्रण करते हुए उसकी प्रभावोत्पादकता और सरसता को शब्दों में उतारते हुए लिखते हैं।
व्याख्या –
ऋतुराज वसंत का समय था, जब खिले पुष्पों की सुगंधि में मग्न होकर भ्रमरों के झुंड झूमते हुए फूलों पर मँडराते रहते थे। मंजरियों की सुगंधि से आम्रवृक्ष अपनी सरसता फैला रहे थे, उसी आम्रवृक्ष पर कोयल के रसपूर्ण गीत गूँज रहे थे। सुगंधि, सुंदरता, मृदुता से संपूर्ण विश्व का सुख उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा था। जिस प्रकार वसंत ऋतु में दिन बड़े हो जाते हैं। विकसित पुष्पों को देखकर कवि कल्पना करता है कि ऋतुराज वसंत का आगमन सुनकर विश्व की सभी इच्छाएँ, कामनाएँ अथवा आकांक्षाएँ अनेक कोमल फूलों में खिल उठीं थीं। फूलों के खिलने में पृथ्वीवासी सभी लोगों की इच्छाएँ इसी प्रकार व्यक्त हो रही थीं, मानो संसार का ईश्वर उन्हें सफल बना दे।
विशेष –
(1) पंत को प्रकृति का कोमल और सुकुमार कवि माना जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, अपितु प्रेम भावना भरित मनों का भी संकेत किया है, जो अपनी स्वाभाविकता और सरसता के कारण अत्यधिक आकर्षक हो गए हैं, जिस प्रकार प्रकृति का यह उद्दीपन रूप स्थान-स्थान पर बाधक हो जाता है, उसी के कारण प्रेमी युगलों के मन में भी इसी प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। आम्र वृक्षों की सरसता, कोयल की मधुरता, फूलों का खिलना और उन पर भ्रमरों का मँडराना यह सभी मिलकर किसी के मन में अपने प्रियतम से मिलने की भावना जाग्रत करते हैं जो अत्यंत स्वाभाविक है।
(2) भाषा स्वर माधुर्य और लाक्षणिक वैचित्र्य से वातावरण और भावात्मकता की सफल सृष्टि करने में सक्षम है।
(3) अलंकार –
(i) ‘मधुर मधुमास’, ‘रसिक पिक से सरस’ – अनुप्रास।
(ii) ‘अवनि के दिवस – से’ – उपमा।
(iii) ‘मृदुल सुमनों में’ – श्लेष।
(iv) ‘अखिल कोमल कामनाएँ अवनि की’ – विशेषण विपर्यय।
रुचिरतर निज कनक किरणों को तपन
चरम गिरि को खींचता था कृपण सा,
अरुण आभा में रँगा था वह पतन
रज कणों सी वासनाओं से विपुल।
अचिरता से सहज आभूषित हुई
कीर्ति कितनी हैं नहीं छिपतीं अहा!
सांध्य महिमा सी, प्रभा अवसान से,
वाम वर्द्धित अल्पता में, तिमिर में।
तरणि के ही संग तरल तरंग से
तरणि डूबी थी हमारी ताल में;
सांध्य निःस्वन से गहन जल गर्भ में
था हमारा विश्व तन्मय हो गया।
बुद्बुदे जिन चपल लहरों में प्रथम
गा रहे थे राग जीवन का अचिर,
अल्प पल, उनके प्रबल उत्थान में
हृदय की लहरें हमारी सो गई॥
शब्दार्थ –
रुचिरतर = रुचि के अनुसार, सुंदर होता हुआ। कनक = स्वर्णिम। कृपण = कंजूस। अरुण = लाल। आभा = प्रकाश। पतन = गिरना। रजकणों = धूलि, कण। विपुल = पर्याप्त। तरणि= सूर्य; नौका। निःस्वन = शब्द रहित। तन्मय = मग्न। अचिर = क्षणिक।
प्रसंग –
वासंती वैभव और मादक वातावरण में नायक जल-विहार करने गया तो उसे प्राकृतिक सौंदर्य सुषमा के साथ जीवन की स्थिति का भी आभास मिलने लगा। अस्ताचलगामी सूर्य की स्वर्णिम रश्मियों और जल में उठने वाले बुलबुलों में जीवन की क्षणिकता का अनुभव करते-करते नायक की नौका भी उस अगाध जल में निमग्न हो गई, उस समय का दृश्य और अपनी मनः स्थिति का चित्रण करते हुए कवि लिखते हैं –
व्याख्या –
अस्ताचलगामी सूर्य पर्वत के सर्वोच्च शिखर को दिनभर तपाने के पश्चात् अपनी स्वर्णिम किरणों को इस प्रकार समेट रहा था जैसे कोई कंजूस व्यक्ति अपने बिखरे हुए धन को संचित करता है। उस समय का दृश्य लालिमा के रंग में रंगा हुआ था। प्रत्येक कण उस समय स्वर्णिम आभा में रंगा हुआ था। जिस प्रकार रजोगुण प्रधान वासनाओं का आधिक्य आकर्षक होकर भी अंततोगत्वा पतनोन्मुख होता है उसी प्रकार सूर्य भी अस्त हो रहा था। ऐसे समय में ही एक चंचल लहर की चोट खाकर सूर्यास्त के साथ ही नायक की नौका भी उस तालाब में डूब गई। संध्याकाल की उस निस्तब्धता में नायक का संपूर्ण संसार उस गहरे जल में डूब गया। कुछ समय पूर्व लहरों के उत्थान-पतन में उठने वाले बुलबुले जीवन की क्षणिकता के गीत गा रहे थे, थोड़े समय में ही उनके प्रबल आघात से केवल नौका ही नहीं, अपितु नायक के मन की भावलहरियाँ भी सो गई वह पूर्णतया मूर्च्छित हो गया।
विशेष –
(1) प्रस्तुत पद्यांश में कवि पंत ने प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने के साथ-साथ उपदेशात्मकता की भी अभिव्यक्ति की है। अस्ताचलगामी सूर्य को कंजूस का रूप देकर जहाँ दृश्य की वास्तविकता को उभारा गया है, उसी प्रकार वासनाओं की विपुलता का पतनोन्मुख होना भी स्वाभाविक रूप में चित्रित हुआ है। नौका के डूबने का दृश्य चित्रित करते हुए मानवीय भावनाओं का संकेत देने में कवि ने अपने काव्य-कौशल का परिचय दिया है।
(2) भाषा माधुर्य और प्रसाद गुण युक्त है। रूप और ध्वनि के सादृश्य में सक्षम होने के कारण इसकी प्रभावात्मकता बढ़ गई है।
(3) अलंकार –
(i) ‘रुचिरतर कृपण-सा’ – उपमा।
(ii) ‘रजकणों-सी विपुल’ – उपमा।
(iii) ‘रजकणों-सी’ – श्लेष।
(iv) ‘तरणि ताल में’ – यमक।
जब विमूर्च्छित नींद से मैं था जगा
(कौन जाने, किस तरह?) पीयूष-सा
एक कोमल समव्यथित नि:श्वास था
पुनर्जीवन सा मुझे तब दे रहा।
मधुप बाला का मधुर मधु मुग्ध राग
पद्मदल में संपुटित था हो चुका,
काम्य उपवन में प्रथम जब था खिला
प्रणय पद्म कुमुद कली के साथ ही।
शीश रख मेरा सुकोमल जाँघ पर,
शशि कला सी एक बाला व्यग्र हो
देखती थी म्लान मुख मेरा, अचल,
सदय, भीरु, अधीर, चिन्तित दृष्टि से।
शब्दार्थ —
पीयूष = अमृत। समव्यथित = समान व्यथा से युक्त। पुनर्जीवन = दुबारा जीवन मिलना। संपुटित = हथेली की अंजलि। व्यग्र = बेचैन। म्लान = उदास। सदय = दयायुक्त। प्रणय = प्रेम। पद्म कुमुद कली = कमल की कली। भीरु = कायर, डरपोक।
प्रसंग –
‘ग्रंथि’ के प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि ने उस समय का चित्रण किया है जब नायक की मूर्च्छा दूर हुई और उसने अपने को किसी की कोमल जंघा पर पड़े हुए देखा था। नौका डूबने के पश्चात् नायक और नायिका के मिलन का दृश्य प्रस्तुत करते हुए कवि लिखते हैं –
व्याख्या –
जब मूर्च्छा टूटी तो नायक को ऐसा प्रतीत हुआ जैसा वह एल लंबी नींद से जगा हो। वह अपने आप में विस्मित था कि वह कहाँ है और कैसे वहाँ पहुँचा है? चिंता और विस्मय में भरे नायक को महसूस हुआ कि किसी का अमृत के समान जीवनदायी और सहानुभूति एवं संवेदना से युक्त किसी के कोमल श्वास जैसे उसे जीवन-दान दे रहे हैं। वह आँखें खोलता है और देखता है कि चंद्रकला के समान एक अनुपम सुंदरी अपनी कोमल जाँघ पर उसका सिर रखे हुए उसकी ओर अत्यंत व्यग्रता से देख रही थी। वह स्थिर दृष्टि से नायक का उदास मुख निहार रही थी, उसकी दृष्टि में दया, भय, व्याकुलता और चिंता का अद्भुत समन्वय हो रहा था।
विशेष –
(1) प्रस्तुत पद्यांश अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इसमें कवि की भावात्मकता तथा कलात्मकता का उत्कर्ष पाठक को विमुग्ध करने में पूर्णतया समर्थ है।
(2) नौका डूबने के पश्चात् नायक तो जैसे अपना जीवन खो चुका था। इस पद्यांश में उसकी मूर्च्छा टूटने के साथ ही जो दृश्य प्रस्तुत किया गया है, वह भावोत्कर्ष की दृष्टि से प्रभावशाली है। मृत्यु मुख से निकलते हुए किसी की सहानुभूति, दया एवं भावनामय संसर्ग पाकर एक सहज आनंद और उत्सुकता जगाने में यह पूर्णतया सफल है।
(3) भारतीय प्रेम गाथाओं में प्रायः नायक और नायिका के मिलन तथा प्रेमोत्कर्ष में समुद्र अथवा नदी की घटना को विशेष महत्त्व दिया जाता है। पंत ने प्राचीन परंपरा को ही नवीनता के आवरण में व्यक्त किया है। जिससे कथानक की भावात्मकता अधिक प्रभावी हो गई है।
(4) नायिका के सौंदर्य तथा उसके मन में उठने वाले विविध भावों को पंत जी ने बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। ‘समव्यथित नि:श्वास’ में व्यथा-युक्त निराशा की अभिव्यक्ति है और अचल, सदय, भीरु, अधीर नायिका के भावों के प्रवाह और शांत चेष्टाओं का मूर्तिकरण कर दिया गया है।
(5) ‘जाँघ’ शब्द में ग्राम्यत्व दोष है।
(6) अलंकार –
(i) ‘पीयूष-सा’ – उपमा।
(ii) ‘पुनर्जीवन सा’ – उपमा।
(iii) ‘शशिकला-सी’ – उपमा।
इंदु पर, उस इंदु मुख पर साथ ही
थे पड़े मेरे नयन, जो उदय से,
लाज से रक्तिम हुए थे; पूर्व को
पूर्व था, पर वह द्वितीय अपूर्व था !
बाल रजनी सी अलक थी डोलती
भ्रमित हो शशि के वदन के बीच में;
अचल, रेखांकित कभी थी कर रही
प्रमुखता मुख की सुछवि के काव्य में।
शब्दार्थ –
इन्दु = चंद्रमा। रजनी = संध्या। अलक = लट। भ्रमित = भटकी हुई। रक्तिम = लाल। पूर्व अद्भुत। सुछवि = सुंदर छवि। वदन = शरीर। शशि = चंद्रमा। रेखांकित = रेखा से युक्त।
प्रसंग – प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नायक द्वारा नायिका के प्रथम दर्शन का चित्र प्रस्तुत किया है। मूर्च्छा हट जाने के पश्चात् नायक नायिका की सदय, भीरु और आतुर दृष्टि को देखकर अपने को पुनर्जीवित समझता है। जिससे सहानुभूति मिली उस जीवन-दात्री की ओर देखता है तो उसे सौंदर्य का पूर्व रूप दिखाई दिया। उस समय पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हो रहा था। कवि नायिका और चंद्रमा के सौंदर्य की तुलना करता है।
व्याख्या –
मूर्च्छा समाप्त होने पर नायक नायिका के चंद्रमा के समान सुंदर मुख को देखने लगता है। पूर्व दिशा में उदय होने वाले चंद्रमा और नायिका के चेहरे में उसे बहुत समानता दिखाई देती है। उदय होता हुआ चंद्रमा लालिमा से युक्त था और नायिका लज्जा के कारण रक्ताभ हो रही थी। पूर्व दिशा के चंद्रमा की अपेक्षा प्रस्तुत चंद्रमा उसे अपूर्व लगता है। जिस प्रकार चंद्रमा के चारों ओर सांध्यकालीन अंधकार फैला हुआ था, जिसमें चंद्रमा का सौंदर्य द्विगुणित हो रहा था, उसी प्रकार नायिका के मुख-चंद्र में एक लट लहरा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अलक सौंदर्य के महत्त्व की कई गुणा वृद्धि कर रही थी। जिस प्रकार किसी काव्य में रेखांकित शब्दों का महत्त्व बढ़ जाता है, वैसे ही नायिका की मुख-सौंदर्य की अलक से अभिवृद्धि हो रही थी।
विशेष –
(1) प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वातावरण की स्वाभाविकता और भावात्मकता की समन्वित सृष्टि की है। कविता के पहले छंद में नौका डूबने का उल्लेख था, सांध्यकालीन वातावरण का विकसित रूप इस पद्यांश के प्रथम शब्द ‘इन्दु’ से ही ध्वनित हो जाता है।
(2) सांध्यकालीन चंद्रमा तथा नायिका के सौंदर्य को ध्वनित करने के लिए कवि ने कालिमा, लालिमा, अलक तथा लज्जा को क्रमशः प्रस्तुत करते हुए सौंदर्य को काव्यात्मक भावात्मकता प्रदान की है।
(3) लहराती हुई अलक से सौंदर्य की वृद्धि का प्रयोग परंपरागत होकर भी अधिक प्रभावात्मक है।
(4) अलंकार –
(i) पूर्व को पूर्व था – यमक।
(ii) बाल रजनी-सी – उपमा।
(iii) पूर्व था अपूर्व था – व्यतिरेक।
देख रति ने मोतियों की लूट यह,
मृदुल गालों पर सुमुखि के लाज से
लाख सी दी त्वरित लगवा, बंद कर
अधर विद्रुम द्वार अपने कोष के ।
वह स्पृहा संकोच का सुंदर समर
अधर कंपित कर, कपोलों पर युगल
एक दुर्बल लालिमा में था बहा;
(विश्व विजयी प्रेम ! औ’ यह भीरुता !)
सुभग लगता है गुलाब सहज सदा,
क्या उषामय का पुनः कहना भला?
लालिमा ही से नहीं क्या टपकती
सेब की चिर सरसता, सुकुमारता?
पद नखों को गिन, समय के भार को
जो घटाती थी भुलाकर, अवनितल
खुरच कर, वह जड़ पलों की धृष्टता
थी वहाँ मानो छिपाना चाहती।
शब्दार्थ –
सुमुखि = सुंदर। स्पृहा – चाह। विद्रुम – लाल कली। कपोलों – गालों। तरुण = युवा। सुभग = सुंदर। उषामय = प्रभातकालीन। सुकुमारता = कोमलता। अवनि तल = पृथ्वी।
प्रसंग –
प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के सौंदर्य और सौकुमार्य का वर्णन करते हुए पंत जी ने प्रेम भावनाजन्य लज्जा तथा संकोच की कुछ क्रियाओं का चित्रण किया है, जिसमें कवि की सूक्ष्म दृष्टि एवं उनकी विधायिनी कल्पना का परिचय मिलता है।
व्याख्या –
सुंदर, मोहक, सुकुमार और यौवन भारभरित नायिका के कपोलों पर पड़ने वाले सीप जैसे गढ़ों का संकेत करते हुए नायक कहते हैं कि सौंदर्य-सागर के भँवर के समान इन गढ़ों में किसके नौका रूपी नेत्र आकर अटक नहीं जाते। सागर अथवा नदी में पड़ने वाले भँवर में यदि कोई नौका घिर जाए तो वह बाहर नहीं निकल पाती, अपितु उसी में भटक कर डूब जाती है। नौका अपने बोझ की अधिकता से डूबती है और नेत्र सौंदर्य-भार से दबकर उसी में खो जाते हैं। गुलाब अपनी सहज सुंदरता में आकर्षक होता है किंतु प्रभातकालीन गुलाब की शोभा कुछ और ही होती है। जिस प्रकार सेब की लालिमा उसकी सरसता का परिचय देती है उसी प्रकार लज्जा की लालिमा में यौवन और सौंदर्य की सरसता और सुकुमारता का परिचय मिल जाता है।
नायिका की मनःस्थिति का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि वह अपने पदनखों से पृथ्वी को खुरचती हुई समय की दीर्घता को भुलाने का प्रयास कर रही थी। वियोग की घड़ियाँ जो व्यतीत नहीं होतीं उनको मिटाने या कम करने के साथ वह अपनी पलकों की घृष्टता भी छिपाने का जो बरबस प्रयास करती है नायक को देखने के लिए ऊपर उठना चाहती हैं।
विशेष –
(1) शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करने वालों ने नायिका की गाल पर गड्ढे पड़ने को उत्तम सौंदर्य का लक्षण माना है।
(2) नौका और नयन दोनों का विमोहित होकर निमग्न हो जाने का वर्णन सादृश्य के कारण स्वाभाविक और प्रभावी बन गया है।
(3) नायिका के संकोच, लज्जा तथा उत्सुकता आदि भावों को प्रकट करने के लिए कवि ने परंपरागत रूप को अपनाया है। नायिका का शील, मर्यादा, संकोच आदि उसे मुखर नहीं बनाता, वह अपनी भावनाओं को छुपाने का उपक्रम करती है, उसी का सहज चित्रण पंत जी ने किया है।
(4) अलंकार –
(i) इन गढ़ों में सौंदर्य के दृष्टान्त।
(ii) क्या उषामय कहना भला – भेदकातिशयोक्ति।
(ii) पद नखों छिपाना चाहती – उत्प्रेक्षा।
इंदु की छबि में, तिमिर के गर्भ में,
अनिल की ध्वनि में, सलिल की वीचि में,
एक उत्सुकता विचरती थी, सरल
सुमन की स्मिति में, लता के अधर में।
निज पलक, मेरी विकलता, साथ ही
अवनि से, उर से मृगेक्षिणि ने उठा,
एक पल, निज स्नेह श्यामल दृष्टि से
स्निग्ध कर दी दृष्टि मेरी दीप सी।
शब्दार्थ –
इंदु – चंद्रमा। तिमिर = अंधकार। अनिल = वायु। सलिल = जल। वीचि = लहर। उत्सुकता = अधीरता। स्मिति मुस्कान। मृगेक्षिणि = मृगाक्षी, मृग जैसी आँखों वाली। स्निग्ध = चिकनी।
प्रसंग –
प्रस्तुत पद्यांश में प्राकृतिक सौंदर्य तथा नायिका के सौंदर्य में भावात्मक संबंध स्थापित करते हुए कवि ने नायक की उत्सुकता तथा नायिका की प्रेमाकुलता का चित्रण किया है। नायिका लज्जावनत थी, नायक उसे निहार रहा था, उसे लगा कि जैसे संपूर्ण प्रकृति भी उसी के समान नायिका को देखने के लिए समुत्सुक है।
व्याख्या –
संपूर्ण प्रकृति में नायिका को देखने की उत्सुकता व्याप्त थी। स्वयं नायिका संकोचवश धरती की ओर देख रही थी किंतु उसके चंद्रमुख की सुंदरता में, जो घने केशांधकार में घिरा हुआ था, मादक श्वासों की कोमल ध्वनि में, आँखों में लहराते हुए प्रेमाश्रमों की लहरों में, फूलों जैसे कोमल अधरों की मुसकान तथा लता के समान कोमल शरीर में उत्सुकता व्याप्त थी। नायिका के समान नायक भी पूर्ण तन्मयता से देख लेना चाहता था, ऐसे समय में उस मृगनयनी ने अपनी पलकों को ऊपर उठाकर नायक की ओर देखा। उस एक पल के दृष्टि-निक्षेप ने नायक की व्याकुलता को समाप्त करने के साथ ही अपनी प्रेमभरी दृष्टि से नायक के जीवन-दीप की लौ को जीवन-दान देकर उसकी चमक को बढ़ा दिया।
विशेष –
(1) प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति तथा मानव के रागात्मक संबंध की सृष्टि की है। चिरकाल से मानव प्रकृति को अपनी ही भावनाओं के अनुकूल देखता आया है, उसी के अनुसार नायक चंद्रमा, अंधकार, वायु, जल, पुष्पलता आदि में अपनी ही भावना का प्रतिबिम्ब देखता है।
(2) प्रस्तुत पद्यांश की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कवि ने लज्जाभारभरित नायिका की भावनाओं की अभिव्यक्ति और उसके सौंदर्य का दिग्दर्शन कराने के लिए प्राकृतिक उपमानों का सुंदर चयन किया है। इंदु मुख, तिमिर-केश जाल, अनिल श्वास, सलिल आँखों की चमक, सुमन-मुख, लता-शरीर आदि नारी-सौंदर्य की अभिवृद्धि करने वाले परंपरागत उपमान हैं। इनमें रूप और गुण-सादृश्य का निर्वाह करने में पंत जी को पूर्ण सफलता मिली है।
(3) अलंकार –
(i) निज पलक दीप-सी – यथासंख्य
(ii) स्नेह, स्निन्ध – श्लेष
(iii) सरल सुमन की स्मिति – अनुप्रास
(iv) दृष्टि मेरी दीप-सी – उपमा
(v) श्यामल दृष्टि – विरोधाभास
प्रथम केवल मोतियों को हंस जो
तरसता था, अब उसे तर सलिल में
कमलिनी के साथ क्रीड़ा की सुखद
लालसा पल पल विकल थी कर रही।
प्रेमियों का कौश सा कोमल हृदय
कोटि-कर सौंदर्य के कृश हाथ में
सहज ही दब कर, नवल आसक्ति से
फूल उठता है पुनः उन्मत्त हो !
रसिक वाचक ! कामनाओं के चपल,
समुत्सुक, व्याकुल पगों से प्रेम की
कृपण वीथी में विचर कर, कुशल से
कौन लौटा हैं हृदय को साथ ला ?
शब्दार्थ –
कमलिनी = कमल का छोटा फूल। लालसा = इच्छा। कौश = कुशद्वीप, रेशमी वस्त्र। कृश = कमज़ोर। उन्मत्त = पागल। चपल = चंचल। कृपण = कंजूस। वीथी = मार्ग। विचर = घूमना।
प्रसंग – प्रस्तुत पद्यांश में कवि पंत ने प्रेमी मन की आकांक्षा तथा प्रेम-मार्ग पर चलने वालों की परिस्थिति का चित्रण किया है। नायक कभी केवल नायिका का सौंदर्य देखना चाहते थे किंतु निकट संपर्क से उसकी विकसित भावनाओं को व्यक्त करते हुए कवि ने कहा है-
व्याख्या –
प्रेमानुभूति जागने से पूर्व जो हंस केवल मोती चुगना चाहता था, उसे केवल सरोवर में से उदात्त मूल्यों को पाने की आकांक्षा थी, किंतु नायिका के सौंदर्य तथा अनुरागमयी दृष्टि पाने के पश्चात् उसके मन में गहरे जल में कमलिनी के समान केवल नायिका से सुखदायी क्रीड़ा करने की लालसा बढ़ती है। प्रेम रंग में ज्यों-ज्यों वह निमग्न होता है, उसकी लालसा भी बढ़ती जाती है। अपनी मनःस्थिति को देखकर नायक प्रेमी-जनों, रसिक- पाठकों को संबोधन करते हुए पूछता है कि क्या कोई व्यक्ति कामनाओं के चंचल, उत्सुकता भरे पैरों से चलकर प्रेम-पंथ के सँकरे मार्ग से अपना हृदय लेकर कुशलता से लौटा है। प्रेम-मार्ग तो केवल एक ओर ही जाता है। सच्चा प्रेमी उस पथ पर चलता है तो वापिस नहीं लौट पाता; भले ही उसका जीवनांत हो जाए।
विशेष –
(1) प्रस्तुत पद्यावतरण में प्रेम के मनोवैज्ञानिक विकास का चित्रण किया गया है। रूप-सौंदर्य से प्रेम की उत्पत्ति, सहानुभूति तथा निकट संपर्क से प्रणय की परिपक्वता और अंत में प्रेम की स्थितियों का इसमें सरस प्रतिपादन हुआ है।
(2) नायक के लिए ‘हंस’ उपमान भी सार्थक है। नीर-क्षीर विवेचन की शक्ति रखने वाला हंस सात्विक होकर भी ज्ञानी माना जाता है। मोतियों जैसे उदात्त जीवन मूल्य पाना उसका लक्ष्य रहता है, किंतु प्रेम का संसर्ग पाकर उसकी रागात्मकता अपने प्रिय में पूर्णतया समर्पित हो जाती है।
(3) अंतिम पंक्तियों में यह भी ध्वनि प्राप्त हो जाती है कि प्रेम-पथ तलवार की धार के समान है, जहाँ किसी की कामना पूर्णतया सफल नहीं होती। परिणाम निराशा में ही फलीभूत होता है।
(4) अलंकार –
(i) कोटि-कर – अनुप्रास
(ii) पल-पल – पुनरुक्ति प्रकाश।