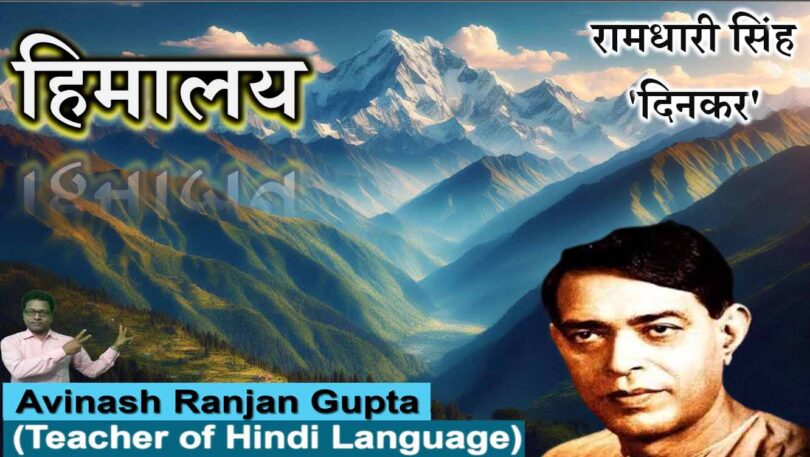हिमालय
मेरे नगपति! मेरे विशाल!
साकार, दिव्य, गौरव विराट्!
पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल!
मेरी जननी के हिम-किरीट!
मेरे भारत के दिव्य भाल!
मेरे नगपति! मेरे विशाल!
युग-युग अजेय, निर्बन्ध, मुक्त,
युग-युग गर्वोन्नत, नित महान
निस्सीम व्योम में तान रहा
युग से किस महिमा का वितान?
कैसी अखंड यह चिर-समाधि?
यतिवर! कैसा यह अमर ध्यान?
तू महाशून्य में खोज रहा?
किस जटिल समस्या का निदान?
उलझन का कैसा विषम जाल?
मेरे नगपति! मेरे विशाल!
ओ मौन तपस्या-लीन यती!
पल भर को तो कर दृगुन्मेष!
रे! ज्वालाओं से दग्ध विकल,
है तड़प रहा पद पर स्वदेश!
सुख -सिंधु, पंचनद, ब्रह्मपुत्र,
गंगा-यमुना की अमिय-धार
जिस पुण्यभूमि की ओर बही
तेरी विगलित करुणा उदार।
जिसके द्वारों पर खड़ा क्रान्त
सीमापति! तू ने की पुकार
‘पददलित इसे करना पीछे
पहले ले मेरा सिर उतार।’
उस पुण्यभूमि पर आज तपी,
रे! आन पड़ा संकट कराल
व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे,
डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल।
मेरे नगपति! मेरे विशाल!
कितनी मणियाँ लुट गयीं, मिटा
कितना मेरा वैभव अशेष!
तू ध्यान-मग्न ही रहा, इधर
वीरान हुआ प्यारा स्वदेश।
कितनी द्रुपदा के बाल खुले,
कितनी कलियों का अंत हुआ?
कह हृदय खोल चित्तौर यहाँ
कितने दिन ज्वाल-वसंत हुआ?
पूछे, सिकताकण से हिमपति,
तेरा वह राजस्थान कहाँ?
वन-वन स्वतंत्रता-दीप लिए
फिरने वाला बलवान कहाँ?
तू पूछ, अवध से राम कहाँ?
वृंदा! बोलो, घनश्याम कहाँ?
ओ मगध! कहाँ मेरे अशोक?
वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ?
पैरों पर ही है पड़ी हुई
मिथिला भिखारिणी सुकुमारी,
तू पूछ, कहाँ इसने खोयीं
अपनी अनन्त निधियाँ सारी?
री कपिलवस्तु! कह बुद्धदेव
के वे मंगल उपदेश कहाँ?
तिब्बत, इरान, जापान, चीन
तक गये हुए सन्देश कहाँ?
वैशाली के भग्नावशेष से
पूछ; लिच्छवी-शान कहाँ?
ओ री उदास गण्डकी! बता,
विद्यापति कवि के गान कहाँ?
तू तरुण देश से पूछ अरे!
गूँजा कैसा यह ध्वंस-राग?
अम्बुधि-अन्तस्तल-बीच छिपी
यह सुलग रही है कौन आग?
प्राची के प्रांगण -बीच देख,
जल रहा स्वर्ण-युग-अग्नि ज्वाल,
तू सिंहनाद कर जाग तपी!
मेरे नगपति! मेरे विशाल!
रे! रोक युधिष्ठिर को न यहाँ,
जाने दे उनको स्वर्ग धीर!
पर, फिरा हमें गाण्डीव -गदा,
लौटा दे अर्जुन -भीम वीर।
कह दे शंकर से आज करें,
वे प्रलय-नृत्य फिर एक बार
सारे भारत में गूँज उठे,
‘हर-हर-बम’ का फिर महोच्चार।
ले अंगड़ाई उठ, हिले धरा,
कर निज विराट स्वर में निनाद,
तू शैल-राट् हुंकार भरे,
फट जाय कुहा, भागे प्रमाद।
तू मौन त्याग कर सिंहनाद,
रे तपी! आज तप का न काल,
नवयुग -शंख-ध्वनि जगा रही
तू जाग, जाग, मेरे विशाल!
दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। दिनकर की प्राथमिक शिक्षा गाँव से पूरी हुई। वे हाई स्कूल की परीक्षा मोकामाघाट से उत्तीर्ण हुए। उसके बाद वे पटना चले आए और पटना कॉलेज से इतिहास विषय में बी.ए. ऑनर्स की परीक्षा पास की। उन्होंने कई तरह की सरकारी और प्राइवेट नौकरी की। वे कुलपति के पद पर भी रहे और सांसद भी।
दिनकर में राजनीतिक चेतना प्रखर थी जिसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं में खूब हुई है। उनपर गाँधीवाद का गहरा प्रभाव पड़ा, हालाँकि वे गाँधीवाद के प्रति असहमति दर्ज करनेवाली कविताएँ भी एक दौर में लिख चुके थे। वे जवाहरलाल नेहरू के निकट थे, मगर ‘परशुराम की प्रतीक्षा’ की कविताओं में उनके शासनकाल की आलोचना भी दिखाई पड़ती है। ‘संस्कृति के चार अध्याय’ के लिए ‘साहित्य अकादमी’ और ‘उर्वशी’ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से वे सम्मानित हुए।।
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु 24 अप्रैल, 1974 में हुई थी।
काव्य कृतियाँ
रेणुका (1935), हुंकार (1938), रसवन्ती (1939), द्वंद्वगीत (1940), कुरूक्षेत्र (1946), सामधेनी (1947), बापू (1947), इतिहास के आँसू (1951), रश्मिरथी (1952), दिल्ली (1954), नीम के पत्ते (1954), नील कुसुम (1955), चक्रवाल (1956), सीपी और शंख (1957), उर्वशी (1961), परशुराम की प्रतीक्षा (1963), हारे को हरिनाम (1970), रश्मिलोक (1974)
गद्य कृतियाँ
मिट्टी की ओर 1946 अर्धनारीश्वर 1952, रेती के फूल 1954, संस्कृति के चार अध्याय 1956, पन्त – प्रसाद और मैथिलीशरण 1958, वेणुवन 1958 धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1969 लोकदेव नेहरू 1965, शुद्ध कविता की खोज 1966, साहित्य- मुखी 1968, राष्ट्रभाषा आंदोलन और गांधीजी 1968, हे राम! 1968, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1970, भारतीय एकता 1971, मेरी यात्राएँ 1971, दिनकर की डायरी 1973, चेतना की शिला 1973।
‘हिमालय’ शीर्षक कविता रामधारी सिंह दिनकर के काव्य-संग्रह ‘हुंकार’ (1938) से ली गई है। इस कविता में दिनकर ने हिमालय को संबोधित करके राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी कुछ बातों को व्यक्त किया है। कविता की अपील यह है कि भारत आज दुर्दशा को प्राप्त हो गया है, ऐसी स्थिति में देश की गौरवशाली परंपरा को याद करने की जरूरत है।
‘हिमालय’ शीर्षक कविता में भारतीय आख्यान और इतिहास की वीरता से जुड़े प्रसंगों को याद किया गया है। ‘हुंकार’ (1938) में संगृहीत इस कविता का संदर्भ स्वतंत्रता आंदोलन है अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते के अलावा क्रांतिकारी मार्ग को अपनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी सक्रिय थे। इस धारा का अपना महत्त्व है। भारतीय जनमानस का एक बड़ा हिस्सा इस रास्ते पर चलनेवालों को सम्मान की दृष्टि से देखता था। इन लोगों की शहादत को नायकत्व का दर्जा प्रदान किया जाता था। दिनकर ने इसी धारा की भावनाओं को इस कविता में सांस्कृतिक शब्दावली के द्वारा व्यक्त किया है।
हिमालय -सप्रसंग व्याख्या
01
मेरे नगपति! मेरे विशाल!
साकार, दिव्य, गौरव विराट्!
पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल!
मेरी जननी के हिम-किरीट!
मेरे भारत के दिव्य भाल!
शब्दार्थ
नगपति – पर्वतों का राजा, हिमालय
विशाल – बहुत बड़ा, व्यापक
साकार – मूर्त रूप में, प्रत्यक्ष रूप से
दिव्य – अलौकिक, पवित्र
गौरव – सम्मान, प्रतिष्ठा
विराट – अत्यंत विशाल, महान
पौरुष – पुरुषार्थ, वीरता
पुंजीभूत – संचित, इकट्ठा हुआ
ज्वाल – अग्नि, प्रचंडता
किरीट – मुकुट, ताज
भाल – मस्तक, माथा
संदर्भ और प्रसंग
‘हिमालय’ शीर्षक कविता रामधारी सिंह दिनकर के काव्य-संग्रह ‘हुंकार’ (1938) से ली गई है। इस कविता में दिनकर ने हिमालय को सम्बोधित करके राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी कुछ बातों को व्यक्त किया है। कविता की अपील यह है कि भारत आज दुर्दशा को प्राप्त हो गया है, ऐसी स्थिति में देश की गौरवशाली परंपरा को याद करने की जरूरत है। हमारे देशवासियों ने पहले भी विपरीत परिस्थितियों में कड़ा संघर्ष किया है। इस कविता में हिमालय को भारत के गौरव का प्रतीक मानकर आह्वान किया गया है। यह आह्वान प्रत्यक्ष रूप से तो हिमालय से है, मगर आंतरिक अर्थ में देशवासियों से है।
व्याख्या –
इन पंक्तियों में कवि दिनकर कहते हैं कि हे मेरे नगपति! तुम दुनिया भर के पर्वतों में सबसे ऊँचे हो! तुम विशाल हो! विराटता और दिव्यता के तुम साकार रूप हो! तुम हमारे देश के लिए विराट गौरव हो! आगे की पंक्तियों में दिनकर ने हिमालय की विशिष्टताओं को बताने के लिए कई तरह की भावनात्मक कल्पना का उपयोग किया है। ऐसे बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से वे राष्ट्रीयता की भावना को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि हे हिमालय! तुम पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल हो अर्थात् पौरुष के समग्र रूप की कल्पना यदि की जाए तो वह तुम्हारी तरह का ही होगा! तुम मेरी भारतमाता के मस्तक पर बर्फ के मुकुट की तरह सुशोभित हो! तुम मेरे देश के दिव्य ललाट की तरह मालूम पड़ते हो।
02
मेरे नगपति! मेरे विशाल!
युग-युग अजेय, निर्बन्ध, मुक्त,
युग-युग गर्वोन्नत, नित महान
निस्सीम व्योम में तान रहा
युग से किस महिमा का वितान?
शब्दार्थ
अजेय – जिसे जीता न जा सके
निर्बन्ध – बिना बंधन के, स्वतंत्र
मुक्त – आज़ाद, स्वाधीन
गर्वोन्नत – गर्व से ऊँचा उठा हुआ
निस्सीम – जिसकी कोई सीमा न हो
व्योम – आकाश, गगन
वितान – विस्तार, फैलाव
व्याख्या
इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम युगों-युगों से अपराजित हो, बंधनहीन हो, मुक्त हो और मुक्ति के प्रतीक भी हो, तुम युगों-युगों से गौरव के साथ खड़े हो, तुम महानता के शाश्वत रूप हो! आज भी तुम इस सीमाहीन आकाश में अपनी महिमा का आवरण तानते जा रहे हो! तुमसे मेरी यहीं असहमति है। दिनकर इसके बाद हिमालय से जो बातें कह रहे हैं उनका सारांश यही है कि भारत की आज की अवस्था के अनुसार तुम्हें कुछ कदम उठाने की जरूरत है। ऐसा कहकर दिनकर इस कविता में हिमालय को भारत की विशाल जनता का प्रतिनिधि बना देते हैं।
03
कैसी अखंड यह चिर-समाधि?
यतिवर! कैसा यह अमर ध्यान?
तू महाशून्य में खोज रहा?
किस जटिल समस्या का निदान?
उलझन का कैसा विषम जाल?
शब्दार्थ
अखंड – टूटा न हो, संपूर्ण
चिर-समाधि – अनंत ध्यान, स्थायी ध्यान
यतिवर – श्रेष्ठ तपस्वी, महान संत
अमर – जिसका कभी नाश न हो
ध्यान – मन लगाना, ध्यानावस्था
महाशून्य – बहुत बड़ा खाली स्थान, ब्रह्मांड
जटिल – कठिन, उलझा हुआ
समस्या – कठिनाई, उलझन
निदान – हल, समाधान
उलझन – परेशानी, समस्या
विषम – कठिन, कठिनाई से भरा
जाल – जाली, घेरेबंदी
व्याख्या
दिनकर जी कहते हैं कि भारत आज पराधीन है, मगर तुमने तो अखंड समाधि ले रखी है। यह चिर-समाधि किस लिए? हे यतिवर! तुम्हारा ध्यान तो टूट ही नहीं रहा है, यह अमर ध्यान किस लिए? ऐसा लगता है तुम आज की समस्याओं का समाधान सिर उठाकर आकाश के महाशून्य में तलाश रहे हो! मगर समस्या तो तुम्हारे पदतल में फैली भारत भूमि पर है। इस भारत-भूमि की समस्याओं से भी ज्यादा जटिल किसी समस्या का समाधान तुम महाशून्य में खोज रहे हो क्या? मगर ऐसी स्थिति दिखाई तो नहीं देती। निश्चित रूप से समस्या इस धरती पर है, आकाश में नहीं तुम्हें देखकर लगता है कि तुम किसी गहरी उलझन में फँसे हो!
04
मेरे नगपति! मेरे विशाल!
ओ मौन तपस्या-लीन यती!
पल भर को तो कर दृगुन्मेष!
रे! ज्वालाओं से दग्ध विकल,
है तड़प रहा पद पर स्वदेश!
शब्दार्थ
तपस्या-लीन – ध्यान में मग्न
यती – तपस्वी, संन्यासी
दृगुन्मेष – आँखें खोलना
ज्वालाओं – आग की लपटें
दग्ध – जला हुआ, पीड़ित
विकल – बेचैन, परेशान
स्वदेश – अपना देश, मातृभूमि
व्याख्या
कवि दिनकर जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि मेरे विशाल नगपति, तुम मौन रहकर तपस्या में लीन रहनेवाले संन्यासी की तरह मालूम पड़ते हो मेरा निवेदन है कि आज तुम्हें पल भर के लिए ही सही, मगर अपनी आँखें खोल देनी चाहिए। तब तुम देख पाओगे कि तुम्हारे कदमों पर पड़ा यह महान देश आज विविध विपत्तियों की आग में जल रहा है। तुम यह भी देख पाओगे कि भारतवासी किन-किन मुसीबतों से ग्रस्त होकर तड़प रहे हैं।
05
सुख -सिंधु, पंचनद, ब्रह्मपुत्र,
गंगा-यमुना की अमिय-धार
जिस पुण्यभूमि की ओर बही
तेरी विगलित करुणा उदार।
जिसके द्वारों पर खड़ा क्रान्त
सीमापति! तू ने की पुकार
‘पददलित इसे करना पीछे
पहले ले मेरा सिर उतार।’
शब्दार्थ
सिंधु – समुद्र
पंचनद – पाँच नदियों का समूह (पंजाब)
अमिय – अमृत, जीवनदायक
पुण्यभूमि – पवित्र भूमि
विगलित – बहता हुआ, पिघला हुआ
करुणा – दया, सहानुभूति
द्वारों – दरवाजे
क्रान्त – क्रांति करने वाला
सीमापति – सेना का नायक
पददलित – पैरों से कुचला हुआ
व्याख्या
कवि कहते हैं कि हे गिरिराज हिमालय! तुमने इस देश को बहुत कुछ दिया है। सिंधु जैसी विशाल नदी से भारत की भूमि को सिंचित किया है। पंजाब की पाँचों नदियाँ (सतलज, झेलम, चनाब, रावी और व्यास), ब्रह्मपुत्र, गंगा-यमुना आदि की अमृतमय जलधारा को तुमने भारत को ऐसे प्रदान किया है मानो तुम्हारी करुणा पिघल कर भारत को आशीष दे रही है। तुम युगों-युगों से भारत की सीमा पर सीमापति की तरह खड़े हो। जब भी किसी ने सीमा को पार कर आतंकित करने की कोशिश की, तब तुमने गर्जना की कि पहले मुझसे टकराओ तब इस पवित्र भूमि में प्रवेश करो!
06
उस पुण्यभूमि पर आज तपी,
रे! आन पड़ा संकट कराल
व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे,
डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल।
मेरे नगपति! मेरे विशाल!
कितनी मणियाँ लुट गयीं, मिटा
कितना मेरा वैभव अशेष!
तू ध्यान-मग्न ही रहा, इधर
वीरान हुआ प्यारा स्वदेश।
शब्दार्थ
संकट करालय – संकट का घर, भारी मुसीबत
व्याकुल – चिंतित, परेशान
सुत – संतान, बेटा
डस – डंक मारना, नुकसान पहुँचाना
चतुर्दिक – चारों ओर
विविध – विभिन्न
व्याल – साँप, दैत्य
मणियाँ – बहुमूल्य रत्न
लुट – चोरी, हानि
वैभव – समृद्धि, ऐश्वर्य
अशेष – जिसका अंत न हो
ध्यान-मग्न – ध्यान में डूबा हुआ
वीरान – उजड़ा हुआ
स्वदेश – अपना देश
व्याख्या
कवि इन पंक्तियों में भारत की आर्थिक दुर्दशा का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हे तपस्वी! उसी पुण्य भूमि पर आज भयानक संकट आ खड़ा हुआ है। तुम्हारी संतानें व्याकुल होकर तड़प रही हैं। उन पर चारों तरफ से सर्प रूपी अनेक कठिनाइयाँ हँस रही हैं। हमारे देश की अकूत संपत्ति लूट कर विदेश भेज दी गई। हमारा वैभव कभी समाप्त होनेवाला नहीं था, मगर उसे भी लूट लिया गया। तुम इन सब बातों से बेखबर होकर ध्यान में लीन रहे और हमारा प्यारा देश वीरान कर दिया गया।
07
कितनी द्रुपदा के बाल खुले,
कितनी कलियों का अंत हुआ?
कह हृदय खोल चित्तौर यहाँ
कितने दिन ज्वाल-वसंत हुआ?
पूछे, सिकताकण से हिमपति,
तेरा वह राजस्थान कहाँ?
वन-वन स्वतंत्रता-दीप लिए
फिरने वाला बलवान कहाँ?
तू पूछ, अवध से राम कहाँ?
वृंदा! बोलो, घनश्याम कहाँ?
ओ मगध! कहाँ मेरे अशोक?
वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ?
शब्दार्थ
द्रुपदा – महाभारत की एक पात्र (द्रौपदी)
बाल खुले – अपमानित होना
कलियाँ – फूल, युवा लड़कियाँ
अंत – समाप्ति
चित्तौर – चित्तौड़गढ़ (राजस्थान का प्रसिद्ध किला)
ज्वाल-वसंत – अग्निकाल, विनाशकारी समय
सिकताकण – रेत के कण
हिमपति – बर्फ का स्वामी, हिमालय
राजस्थान – भारत का एक राज्य
स्वतंत्रता-दीप – आज़ादी का दीपक
अवध – अयोध्या का पुराना नाम
राम – भगवान राम
वृंदा – वृंदावन
घनश्याम – श्रीकृष्ण
मगध – प्राचीन भारत का एक राज्य
अशोक – महान सम्राट
चंद्रगुप्त – चंद्रगुप्त मौर्य
व्याख्या
कवि इन पंक्तियों में गिरिश्रेष्ठ से कहते हैं कि मैं कितनी समस्याएँ गिनवाऊँ? अब तक न जाने स्त्री पर अत्याचार की कितनी घटनाएँ घटित हो गईं हैं। महाभारत में तो एक द्रौपदी के बाल खुले थे, आज न जाने ऐसी कितनी वारदातें हो चुकी हैं और हो रही हैं। न जाने कितने बच्चे-बच्चियों को अत्याचार की बलिवेदी पर मौत मिल चुकी है। चितौड़ से पूछ लो कि उसके जौहर की घटनाएँ अब हर जगह घटित हो रही हैं। हे हिमपति! मेरी बातों पर विश्वास न हो तो, बालू के कणों से बनी उस विराट भूमि से पूछो कि तुम्हारा वह गौरवशाली राजस्थान अब किस हालत में है? उसी राजस्थान के उदयपुर में महाराणा प्रताप हुए थे, जिन्होंने जंगल में जीवन बिताना मंजूर किया मगर अपनी स्वतंत्रता के दीपक को बुझने नहीं दिया! जरा पूछना ऐसे बलवान अब कहाँ हैं? तुम दूसरी जगहों का हाल-चाल भी पूछ सकते हो! कोई फर्क नहीं मिलेगा। सबकी दुर्दशा समान है। तुम अयोध्या से पूछो कि तुम्हारे राम कहाँ चले गए? वृन्दावन से पूछो कि कृष्ण कहाँ चले गए? हे मगध! मेरे प्रियदर्शी अशोक और महान सम्राट चंद्रगुप्त कहाँ चले गए? क्या इस गौरवशाली अतीत की कोई निशानी आज मौजूद है? नहीं। आज केवल हताशा है।
08
पैरों पर ही है पड़ी हुई
मिथिला भिखारिणी सुकुमारी,
तू पूछ, कहाँ इसने खोयीं
अपनी अनन्त निधियाँ सारी?
री कपिलवस्तु! कह बुद्धदेव
के वे मंगल उपदेश कहाँ?
तिब्बत, इरान, जापान, चीन
तक गये हुए सन्देश कहाँ?
वैशाली के भग्नावशेष से
पूछ; लिच्छवी-शान कहाँ?
ओ री उदास गण्डकी! बता,
विद्यापति कवि के गान कहाँ?
शब्दार्थ
मिथिला – जनकपुर (सीता की जन्मभूमि)
भिखारिणी – भीख माँगने वाली
सुकुमारी – कोमल, सुंदर लड़की
अनन्त निधियाँ – अपार संपत्तियाँ
कपिलवस्तु – गौतम बुद्ध का जन्मस्थान
बुद्धदेव – भगवान बुद्ध
मंगल उपदेश – कल्याणकारी शिक्षाएँ
तिब्बत, इरान, जापान, चीन – देशों के नाम
संदेश – सूचना, शिक्षा
वैशाली – लिच्छवी गणराज्य की राजधानी
भग्नावशेष – खंडहर
लिच्छवी – एक प्राचीन भारतीय गणराज्य
गण्डकी – नेपाल में बहने वाली नदी
विद्यापति – मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि
गान – गीत
व्याख्या
कवि कहते हैं कि अगर तुम्हें दूर जाने की इच्छा नहीं है तो तुम्हारे पैरों के नजदीक मिथिला की भूमि है, उसी से पूछो कि आज वह सुकुमारिणी एक भिखारिणी की तरह लग रही है। उसका हाल-चाल पूछो कि उसने अपनी अनंत निधियाँ कहाँ खो दी हैं? जवाब तो सबका यही है कि इस दरिद्रता का कारण अंग्रेजों का साम्राज्य है। पूरा भारत हिंसा और दमन से पटा हुआ है। हे कपिलवस्तु! तुम्हीं बताओ कि गौतम बुद्ध के मंगलमय उपदेश आज कहाँ चले गए? एक समय था कि उनके उपदेश तिब्बत, ईरान, जापान, चीन इत्यादि देशों तक प्रसारित हो गए थे। भारत से चले हुए ये उपदेश आज भारत में ही सुनाई नहीं पड़ रहे हैं। बुद्ध ने शांति के उपदेश दिए थे, मगर आज भारत में ही उसकी कमी हो गई है। चारों तरफ अशांति का साम्राज्य फैला हुआ है। एक जमाना था कि वैशाली में लिच्छवियों का लोकतान्त्रिक गणराज्य था। मगर आज सब धूल-धूसरित हो चुका है। अब तो हमारा पुराना साहित्य भी देखने-सुनने को नहीं मिलता है। जिस गंडकी नदी के किनारे विद्यापति के गीतों की धूम मची रहती थी, वहाँ आज उदासी छायी हुई है।
09
तू तरुण देश से पूछ अरे!
गूँजा कैसा यह ध्वंस-राग?
अम्बुधि-अन्तस्तल-बीच छिपी
यह सुलग रही है कौन आग?
प्राची के प्रांगण-बीच देख,
जल रहा स्वर्ण-युग-अग्नि ज्वाल,
तू सिंहनाद कर जाग तपी!
मेरे नगपति! मेरे विशाल!
रे! रोक युधिष्ठिर को न यहाँ,
जाने दे उनको स्वर्ग धीर!
पर, फिरा हमें गाण्डीव -गदा,
लौटा दे अर्जुन -भीम वीर।
कह दे शंकर से आज करें,
वे प्रलय-नृत्य फिर एक बार
सारे भारत में गूँज उठे,
‘हर-हर-बम’ का फिर महोच्चार।
शब्दार्थ
तरुण देश – युवा राष्ट्र
ध्वंस-राग – विनाश की ध्वनि
अम्बुधि – समुद्र
अन्तस्तल – आंतरिक भाग
सुलग रही – जल रही
अग्नि ज्वाल – आग की लपट
सिंहनाद – शेर की दहाड़, गर्जना
युधिष्ठिर – महाभारत के धर्मराज
गाण्डीव – अर्जुन का धनुष
गदा – भीम का हथियार
अर्जुन-भीम वीर – पांडवों के योद्धा
शंकर – भगवान शिव
प्रलय-नृत्य – तांडव नृत्य
हर-हर-बम – शिवजी का जयघोष
व्याख्या
कवि दिनकर जी कहते हैं कि यह ठीक है कि तुम तक ये बातें अभी नहीं पहुँची हैं। मगर यह देश तरुणाई की अँगड़ाई ले रहा है। इस प्राचीन देश के भीतर से नई चेतना जन्म ले रही है। इस तरुण देश से तुम संवाद स्थापित करो! इनकी बातें सुनो कि ये तुम से क्या चाहते हैं। नई चेतना से युक्त इस देश से पूछो कि विध्वंस की यह कैसी ध्वनि सुनाई पड़ रही है? ऐसा लगता है कि समुद्र के भीतर कोई आग सुलग रही है। लगता है कि पूरा देश भीतर-भीतर क्रांति की तैयारी कर रहा है। पूरब दिशा में निकलता हुआ सूरज मानो स्वर्ण युग की अग्नि लेकर प्रज्वलित हो रहा है। ऐसे समय में हे मेरे नगपति! तुम अपनी तपस्या छोड़कर जाग जाओ! तुम अपने विराट रूप के साथ सिंहनाद करो! तुमसे अनुरोध है कि आज युद्धिष्ठिर को स्वर्गारोहण करने दो, उन्हें मत रोको! आज उनकी जरूरत नहीं है। आज हमें अर्जुन और भीम की जरूरत है। स्वर्गारोहण की घटना के क्रम में अर्जुन और भीम अपने गांडीव और गदा के साथ तुम्हारी खाइयों में गिर गए थे। आज उन्हें लौटा दो! अर्जुन को गांडीव के साथ और भीम को गदा के साथ! आज की कठिनाइयों से जूझने के लिए अर्जुन-भीम की जरूरत है, युद्धिष्ठिर की नहीं! तुम्हारे कैलाश पर्वत पर शंकर का वास है। उनसे कहो कि एक बार प्रलय-नृत्य कर दें! जो कुछ बुरा उसका विध्वंस हो जाए और एक बार फिर से पूरे भारत में ‘हर-हर -बम’ का जयघोष सुनाई पड़ जाए!
10
ले अंगड़ाई उठ, हिले धरा,
कर निज विराट स्वर में निनाद,
तू शैल-राट् हुंकार भरे,
फट जाय कुहा, भागे प्रमाद।
तू मौन त्याग कर सिंहनाद,
रे तपी! आज तप का न काल,
नवयुग -शंख-ध्वनि जगा रही
तू जाग, जाग, मेरे विशाल!
शब्दार्थ
हुंकार – गर्जना
कुहा – कोहरा
प्रमाद – आलस्य
नवयुग – नया युग
शंख-ध्वनि – विजय का उद्घोष
जगा – जागो
तपी – तपस्वी
जाग – उठो
व्याख्या
कवि दिनकर जी अंतिम बात यह कहते हैं कि तुम ध्यान छोड़ो! एक बार अँगड़ाई लो! तुम्हारी हल्की अँगड़ाई से भी यह पूरी धरती हिल जाएगी! आज तक तुम्हारी आवाज किसी ने नहीं सुनी हमारा अनुरोध है कि अपने विराट स्वर से अनुगूँज पैदा कर दो! हे पर्वतेश्वर! तुम्हारे हुंकार से धुंधलका फट जाएगा और प्रमाद दूर हो जाएगा! तुम्हारी एक छोटी-सी कोशिश भारत में नई चेतना का संचार कर देगी और विरोधियों के हौसले पस्त हो जाएँगे! तुम अपने मौन को त्याग दो! सिंहनाद करो! हे तपस्वी! आज तपस्या करने का समय नहीं है। नए युग की शंख-ध्वनि जगा रही है। हे मेरे विशाल! तुम जाग जाओ!
हिमालय को भारत की विराटता और वीरता का प्रतीक बताया गया है।
हिमालय को संबोधित यह कविता भारत के आख्यान और इतिहास से गर्व के प्रसंगों को प्रस्तुत कर रही है।
स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह कविता देशवासियों से पुनर्जागरण की अपील करती है।
इस कविता का निर्माण 16 मात्राओं की पंक्तियों से हुआ है।
स्वतंत्रता आंदोलन के समय केवल अहिंसा और सत्याग्रह से ही काम नहीं लिया गया था। ऐसे कई आंदोलन हुए थे जहाँ हिंसात्मक संघर्ष का सहारा लिया गया था। क्रांतिकारी विचारों में विश्वास रखनेवाले आंदोलनकारियों के प्रयासों का अपना महत्त्व है। यह कविता इसी प्रकार के संघर्षो का पक्ष ले रही है।