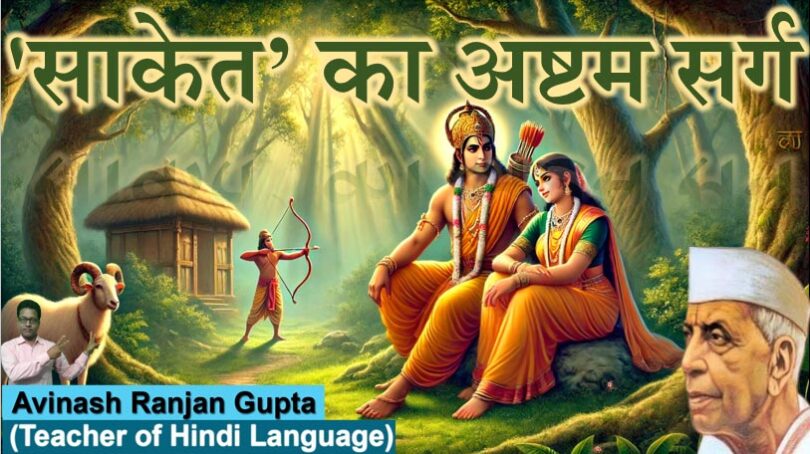‘साकेत‘ के चयनित अंश अष्टम सर्ग
निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
सम्राट स्वयं प्राणेश, सचिव देवर हैं,
देते आकर आशीष हमें मुनिवर हैं।
धन तुच्छ यहाँ,-यद्यपि असंख्य आकर हैं,
पानी पीते मृग-सिंह एक तट पर हैं।
सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
क्या सुन्दर लता-वितान तना है मेरा,
पुंजाकृति गुंजित कुंज घना है मेरा।
जल निर्मल, पवन पराग-सना है मेरा,
गढ़ चित्रकूट दृढ़-दिव्य बना है मेरा।
प्रहरी निर्झर, परिखा प्रवाह की काया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ,
अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ।
श्रमवारिविन्दुफल, स्वास्थ्यशुक्ति फलती हूँ,
अपने अंचल से व्यजन आप झलती हूँ॥
तनु-लता-सफलता-स्वादु आज ही आया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया॥
जिनसे ये प्रणयी प्राण त्राण पाते हैं
जी भर कर उनको देख जुड़ा जाते हैं।
जब देव कि देवर विचर-विचर आते हैं,
तब नित्य नये दो-एक द्रव्य लाते हैं॥
उनका वर्णन ही बना विनोद सवाया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया॥
किसलय-कर स्वागत-हेतु हिला करते हैं,
मृदु मनोभाव-सम सुमन खिला करते हैं।
डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं,
तृण तृण पर मुक्ता-भार झिला करते हैं।
निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा?
वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा।
कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा,
वन में ही तो ग्रार्हस्थ्य जगा है मेरा,
वह बधू जानकी बनी आज यह जाया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
फल-फूलों से हैं लदी डालियाँ मेरी,
वे हरी पत्तलें, भरी थालियाँ मेरी।
मुनि बालाएँ हैं यहाँ आलियाँ मेरी,
तटिनी की लहरें और तालियाँ मेरी।
क्रीड़ा-साम्राज्ञी बनी स्वयं निज छाया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
मैं पली पक्षिणी विपिन-कुंज-पिंजर की,
आती है कोटर-सदृश मुझे सुध घर की।
मृदु-तीक्ष्ण वेदना एक एक अन्तर की,
बन जाती है कल-गीति समय के स्वर की।
कब उसे छेड़ यह कंठ यहाँ न अघाया?
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
गुरुजन-परिजन सब धन्य ध्येय हैं मेरे,
ओषधियों के गुण-विगुण ज्ञेय हैं मेरे।
वन-देव-देवियाँ आतिथेय हैं मेरे,
प्रिय-संग यहाँ सब प्रेय-श्रेय हैं मेरे।
मेरे पीछे ध्रुव-धर्म स्वयं ही धाया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
नाचो मयूर, नाचो कपोत के जोड़े,
नाचो कुरंग, तुम लो उड़ान के तोड़े।
गाओ दिवि, चातक, चटक, भृंग भय छोड़े,
वैदेही के वनवास-वर्ष हैं थोड़े।
तितली, तूने यह कहाँ चित्रपट पाया?
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
आओ कलापि, निज चन्द्रकला दिखलाओ,
कुछ मुझसे सीखो और मुझे सिखलाओ।
गाओ पिक,मैं अनुकरण करूँ, तुम गाओ,
स्वर खींच तनिक यों उसे घुमाते जाओ।
शुक, पढ़ो,-मधुर फल प्रथम तुम्हीं ने खाया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
मैथिलीशरण गुप्त (1886-1964) द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। ‘जयद्रथ वध’ और ‘भारत भारती’ के प्रकाशन से लोकप्रियता के शिखर पर पहुँचे मैथिलीशरण गुप्त को 1930 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। उन्होंने प्राचीन आख्यानों को अपने काव्य का वर्ण्य विषय बनाकर उनके सभी पात्रों को एक नया अभिप्राय दिया है। जयद्रथवध, पंचवटी, सैरन्ध्री, बक संहार, द्वापर, नहुष, जयभारत, हिडिम्बा, विष्णुप्रिया, यशोधरा, साकेत एवं रत्नावली आदि रचनाएँ इसके उदाहरण हैं। ‘साकेत’ महाकाव्य है तथा शेष सभी काव्य खंड काव्य के अंतर्गत आते हैं।
गुप्त जी ने कुछ नाटक भी लिखे हैं। इन नाटकों में अनघ, तिलोत्तमा, चरणदास, विसर्जन आदि उल्लेखनीय हैं। खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा और जन-जन तक पहुँचाने में मैथिलीशरण गुप्त की भूमिका सबसे महत्त्वपूर्ण है। मैथिलीशरण गुप्त जी को साहित्य जगत् में ‘दद्दा’ नाम से संबोधित किया जाता है।
‘साकेत’ मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित एक महाकाव्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी गुप्त जी के साहित्यिक गुरु थे। उनकी प्रत्यक्ष प्रेरणा से ‘साकेत’ की रचना हुई है। इस महाकाव्य के केंद्र में उर्मिला है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध ‘कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता’ पढ़ने के बाद एक लंबे अरसे तक इस महाकाव्य की रचना में कवि ने अपने को नियोजित किया। ‘साकेत’ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह को अत्यंत मार्मिकता के साथ नवाँ सर्ग में अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त कैकैयी के चरित्र पर लगे कलंक पर नए सिरे से विचार करते हुए कवि ने उनके मातृत्व को चित्रित किया है। आपके लिए चुने गए अंश में सीता का वर्णन हुआ है। ध्यान दें कि कवि ने रामकथा की पुनरावृत्ति के उद्देश्य से ‘साकेत’ की रचना नहीं की है। आप देख पाएँगे कि इसमें कवि ने अपने समय की स्थितियों और चेतनाओं का भी समावेश किया है। आपका अध्येतव्य विषय ‘साकेत’ के अष्टम सर्ग से अवतरित किया गया है। इस सर्ग में सीता-राम के चित्रकूट का जीवन, भरत के साथ अयोध्यावासियों का राम को मनाना, कैकेयी का अनुताप, लक्ष्मण – उर्मिला का मिलन और अंत में राम की पादुका लेकर भरत के लौटने का प्रसंग वर्णित है।
01
निज सौध सदन में उटज पिता ने छाया,
मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया।
सम्राट स्वयं प्राणेश, सचिव देवर हैं,
देते आकर आशीष हमें मुनिवर हैं।
धन तुच्छ यहाँ-यद्यपि असंख्य आकर हैं,
पानी पीते मृग-सिंह एक तट पर हैं।
सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
शब्दार्थ –
निज – अपना
सौध सदन – महल
उटज – झोंपड़ी, कुटिया
छाया – बसेरा किया, निवास किया
राज भवन – महल
सम्राट – राजा, यहाँ श्रीराम के लिए प्रयोग किया गया है
प्राणेश – प्रिय, जीवनसाथी (सीता जी के लिए)
सचिव – मंत्री (लक्ष्मण के लिए)
देवर – छोटे भाई (लक्ष्मण के लिए)
आशीष – आशीर्वाद
मुनिवर – महान ऋषि-मुनि
तट – किनारा
मृग – हिरण
सिंह – शेर
लाभ – लाभ, फायदा
संदर्भ और प्रसंग –
प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिलीशरण गुप्त की रचना ‘साकेत’ के अष्टम सर्ग से ली गई हैं। ‘साकेत’ में गुप्तजी ने रामकथा को आधार बनाया है। इस कथा के माध्यम से वह आधुनिक युग की जरूरतों, परिस्थितियों और समस्याओं की अभिव्यक्ति और समाधान प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि राम-सीता और लक्ष्मण को अयोध्या लौटा लेने के लिए अयोध्या के निवासी भरत सहित चित्रकूट पहुँचे हुए थे तब राजरानी सीता को स्वावलंबी रूप में प्रस्तुत किया गया है। महलों के सुख साधनों को छोड़कर वन में आई सीता अपनी स्थिति से प्रसन्न और संतुष्ट है। राजभवन के भोग विलास की तुलना में वन का यह स्वच्छंद और प्रद्भत जीवन उसे भाने लगा है इसीलिए वह कहती हैं-
व्याख्या –
इस काव्यांश में सीता के माध्यम कवि ने यह बताया है कि माता सीता अपने पिता के महल में पली-बढ़ी हैं। उनका विवाह भी नरश्रेष्ठ राजा रामचंद्र जी से हुआ और विवाह के पश्चात् भी उनका जीवन महलों में ही बीत रहा था। पर वनवास के बाद आज उनकी ये झोंपड़ी ही उन्हें अधिक प्रिय लग रही हैं। राजा रामचंद्र जी जो एक सम्राट हैं, वन में एक साधारण कुटिया में निवास कर रहे हैं। लक्ष्मण उनके सचिव और देवर के रूप में सेवा कर रहे हैं। ऋषि-मुनि स्वयं आकर आशीर्वाद दे रहे हैं, जिससे यह कुटिया पवित्र और सम्मानित हो गई है। यहाँ सीता माता धन को तुच्छ और असंख्य आशीर्वाद को श्रेष्ठ मानती हैं। कवि यहाँ इस तथ्य को उजागर करते हैं कि असली आनंद भौतिक धन-संपत्ति में नहीं है, बल्कि संतोष में है। यहाँ तक कि जंगल में शेर और हिरण भी एक ही स्थान पर पानी पीते हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रेम और शांति का वातावरण सबको समान रूप से स्वीकार्य होता है। सीता माता को भी इस स्थान में रहने से लाभ ही हुआ है, क्योंकि यहाँ उन्हें वास्तविक आनंद और आत्मीयता प्राप्त हुई। यही कारण है कि उनकी कुटिया उन्हें राजमहल से भी अधिक प्रिय लगती है।
विशेष –
भौतिक सुख-संपत्ति से अधिक आत्मिक शांति और प्रेम महत्त्वपूर्ण हैं।
वास्तविक आनंद सांसारिक वैभव में नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष में है।
प्रेम और समर्पण से कोई भी स्थान राजमहल के समान आनंददायक हो सकता है।
खड़ी बोली कविता का सहज और सुंदर रूप इन पंक्तियों में मौजूद है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग है।
02
क्या सुंदर-लता-वितान तना है मेरा,
पुंजाकृति गुंजित कुंज घना है मेरा।
जल निर्मल, पवन पराग-सना है मेरा,
गढ़ चित्रकूट-दृढ़-दिव्य बना है मेरा
प्रहरी निर्झर, परिखा प्रवाह की काया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
शब्दार्थ –
सुंदर-लता-वितान – सुंदर बेलों (लताओं) की छतरी
तना – विस्तारित, फैला हुआ
पुंजाकृति – समूह के रूप में (घना स्वरूप)
गुंजित – गूंजता हुआ, मधुर ध्वनि से भरा
कुंज – वृक्षों और लताओं से ढका हुआ स्थान
जल निर्मल – स्वच्छ जल
पवन पराग-सना – फूलों के पराग से सुवासित हवा
गढ़ – किला, मजबूत स्थान
चित्रकूट – भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक और प्राकृतिक स्थल, जहाँ श्रीराम ने वनवास का समय बिताया
दृढ़ – मजबूत
दिव्य – अलौकिक, अद्भुत
प्रहरी – पहरेदार, रक्षक
निर्झर – झरना, जलप्रवाह
परिखा – किले के चारों ओर बनी हुई सुरक्षा हेतु जलधारा
प्रवाह की काया – प्रवाहित जल के रूप में बनी हुई
संदर्भ और प्रसंग –
प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिलीशरण गुप्त की रचना ‘साकेत’ के अष्टम सर्ग से ली गई हैं। ‘साकेत’ में गुप्तजी ने रामकथा को आधार बनाया है। इस कथा के माध्यम से वह आधुनिक युग की जरूरतों, परिस्थितियों और समस्याओं की अभिव्यक्ति और समाधान प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि राम-सीता और लक्ष्मण को अयोध्या लौटा लेने के लिए अयोध्या के निवासी भरत सहित चित्रकूट पहुँचे हुए थे तब राजरानी सीता को स्वावलंबी रूप में प्रस्तुत किया गया है। महलों के सुख साधनों को छोड़कर वन में आई सीता अपनी स्थिति से प्रसन्न और संतुष्ट है। राजभवन के भोग विलास की तुलना में वन का यह स्वच्छंद और प्रद्भत जीवन उसे भाने लगा है इसीलिए वह कहती हैं-
व्याख्या –
साकेत महाकाव्य की इन पंक्तियों में सीता जी प्रभु श्रीराम के वनवास काल में अपनी कुटिया के प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी आत्मिक महत्ता का वर्णन करती हैं। कवि ने दर्शाया है कि उनका वन-आवास किसी राजमहल से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रकृति की अनुपम छटा बिखरी हुई है। उनकी कुटिया के चारों ओर सुंदर बेलों की छतरी फैली हुई है। वहाँ वृक्षों का घना समूह है, जहाँ पक्षियों की चहचहाहट गूँज रही है। वहाँ स्वच्छ जलधाराएँ बह रही हैं और हवा फूलों की सुगंध से भरी हुई है। चित्रकूट पर्वत अपने मजबूत और दिव्य स्वरूप में इस स्थान को एक दुर्ग जैसा दृढ़ बना रहा है। पहरेदारों की जगह वहाँ के झरने बहकर रक्षा कर रहे हैं, और किले की परिखा की तरह प्रवाहित जल सुरक्षा प्रदान कर रहा है।
सीता के माध्यम से कवि ने यह संकेत दिया है कि उनका यह आश्रम किसी भव्य राजमहल से कम नहीं है। यहाँ प्राकृतिक आनंद, आत्मिक संतोष और दिव्य वातावरण मिलकर इसे स्वर्ग के समान बना देते हैं। यही कारण है कि श्रीराम को अपनी कुटिया किसी राजभवन से भी अधिक प्रिय लगती है।
विशेष –
भौतिक सुख-संपत्ति से अधिक प्राकृतिक और आत्मिक सौंदर्य महत्त्वपूर्ण होता है।
संतोष, प्रेम और शांति से कोई भी स्थान स्वर्ग के समान बन सकता है।
प्राकृतिक सौंदर्य, सादगी और आध्यात्मिकता जीवन को दिव्य बनाती हैं।
खड़ी बोली कविता का सहज और सुंदर रूप इन पंक्तियों में मौजूद है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग है।
03
औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ।
अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ।
श्रमवारिबिन्दुफल‘ स्वास्थ्यमुक्ति फलती हूँ,
अपने अंचल से व्यंजन आप झलती हूँ।
तनु-लता-सफलता-स्वादु आज ही आया,
मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया।
शब्दार्थ –
औरों के हाथों – दूसरों की सहायता से
नहीं पलती हूँ – आश्रित नहीं रहती, खुद पर निर्भर रहती हूँ
अपने पैरों पर खड़ी – आत्मनिर्भर होना
आप चलती हूँ – स्वयं आगे बढ़ना
श्रमवारिबिन्दुफल – परिश्रम (श्रम) के जल-बिंदुओं (पसीने) से प्राप्त फल
स्वास्थ्यमुक्ति फलती हूँ – स्वस्थ रहने और मुक्ति (सुख-समृद्धि) प्राप्त करने का फल देती हूँ
अंचल – वस्त्र का एक भाग, यहाँ आशय संरक्षण और देखभाल से है
व्यंजन – यहाँ पंखा (भोजन, पकवान नहीं)
झलती हूँ – प्रस्तुत करती हूँ, परोसती हूँ
तनु-लता – कोमल बेल (यहाँ शरीर और मन की कोमलता का प्रतीक)
सफलता – फलदायी होना, मेहनत का परिणाम मिलना
स्वादु – स्वादिष्ट
आज ही आया – आज ही साकार हुआ, आज ही मिला
संदर्भ और प्रसंग –
प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिलीशरण गुप्त की रचना ‘साकेत’ के अष्टम सर्ग से ली गई हैं। ‘साकेत’ में गुप्तजी ने रामकथा को आधार बनाया है। इस कथा के माध्यम से वह आधुनिक युग की जरूरतों, परिस्थितियों और समस्याओं की अभिव्यक्ति और समाधान प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि राम-सीता और लक्ष्मण को अयोध्या लौटा लेने के लिए अयोध्या के निवासी भरत सहित चित्रकूट पहुँचे हुए थे तब राजरानी सीता को स्वावलंबी रूप में प्रस्तुत किया गया है। महलों के सुख साधनों को छोड़कर वन में आई सीता अपनी स्थिति से प्रसन्न और संतुष्ट है। राजभवन के भोग विलास की तुलना में वन का यह स्वच्छंद और प्रद्भत जीवन उसे भाने लगा है इसीलिए वह कहती हैं-
व्याख्या –
सीता जी कहती हैं कि वन में मैं औरों के हाथों नहीं पलती यानी दास-दासियों की सेवा पर निर्भर नहीं हूँ बल्कि अपना काम स्वयं करती हूँ। अपने पैरों पर चलने का अर्थ है कि अब मैं स्वावलंबी हूँ। यहाँ पंखा झलने वाली दासियाँ नहीं हैं। इसीलिए मैं अपने आँचल से स्वयं अपने ऊपर पंखा झलती हूँ यह स्वावलंबन मेरे लिए बड़ा ही उपयोगी है क्योंकि श्रम करके जो पसीना बहाती हूँ उसका समुचित फल भी मुझे मिलता है। यानी परिश्रम करने के कारण मुझे स्वास्थ्य लाभ होता है। शारीरिक श्रम से मिलने वाले आनंद को मैंने आज ही जाना है। इसीलिए मुझे अपनी कुटिया में किसी तरह का अभाव नहीं महसूस होता बल्कि राजभवन जैसा ही आनंद मिलता है। यह कुटिया मेरे मन को राजभवन से भी अधिक भाती है क्योंकि इसने मुझे स्वावलंबी बनाया और मैं मन चाहा कार्य स्वयं कर सकती हूँ।
विशेष –
इन पंक्तियों में लेखक ने स्वावलंबन का महत्त्व बताया है जो गांधी युग की विशेषता है।
सीता के पारंपरिक देवी रूप की बजाय उसे मनुष्य रूप में प्रस्तुत किया गया है।
खड़ी बोली कविता का सहज और सुंदर रूप इन पंक्तियों में मौजूद है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग है।
04
जिनसे ये प्रणयी प्राण त्राण पाते हैं,
जो भरकर उनको देख जुड़ा जाते हैं।
जब देव कि देवर विचर -विचर आते हैं,
तब नित्य नये दो-एक द्रव्य लाते हैं।
उनका वर्णन ही बना विनोद सवाया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
शब्दार्थ –
प्रणयी प्राण – प्रियजनों का जीवन (यहाँ श्रीराम, सीता और लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त)
त्राण पाते हैं – रक्षा और शांति प्राप्त करते हैं
भरकर उनको देख – पूर्ण रूप से देखकर
जुड़ा जाते हैं – हृदय को ठंडक और सुकून प्रदान करते हैं
देव – यहाँ ऋषि-मुनि, संत और देवताओं के लिए प्रयुक्त
देवर – छोटे भाई (यहाँ लक्ष्मण के लिए प्रयुक्त)
विचर – विचार आते हैं – भ्रमण करते हुए आते हैं
नित्य – प्रतिदिन
नये दो-एक द्रव्य लाते हैं – कुछ नई वस्तुएँ (फल, जड़ी-बूटियाँ, आहार सामग्री) लाते हैं
वर्णन – विवरण, चर्चा
विनोद सवाया – आनंद को दोगुना करने वाला
संदर्भ और प्रसंग –
प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिलीशरण गुप्त की रचना ‘साकेत’ के अष्टम सर्ग से ली गई हैं। ‘साकेत’ में गुप्तजी ने रामकथा को आधार बनाया है। इस कथा के माध्यम से वह आधुनिक युग की जरूरतों, परिस्थितियों और समस्याओं की अभिव्यक्ति और समाधान प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि राम-सीता और लक्ष्मण को अयोध्या लौटा लेने के लिए अयोध्या के निवासी भरत सहित चित्रकूट पहुँचे हुए थे तब राजरानी सीता को स्वावलंबी रूप में प्रस्तुत किया गया है। महलों के सुख साधनों को छोड़कर वन में आई सीता अपनी स्थिति से प्रसन्न और संतुष्ट है। राजभवन के भोग विलास की तुलना में वन का यह स्वच्छंद और प्रद्भत जीवन उसे भाने लगा है इसीलिए वह कहती हैं-
व्याख्या –
इन पंक्तियों में सीता जी अपने वनवास में प्राप्त स्नेह, प्रेम और सहयोग का वर्णन कर रही हैं। वे बताती हैं कि उनका और उनके आराध्य श्रीराम जी का साथ देने के लिए रामानुज सदैव तत्पर रहते हैं। लक्ष्मण उनके जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे उन्हें संजीवनी मिलती है, जो अपने स्नेह और सेवा से उनके जीवन को आनंदमय बना देते हैं। जब देव या प्रियजन के रूप में लक्ष्मण आश्रम में आते हैं, तो वे कुछ आवश्यक वस्तुएँ भी अपने साथ लाते हैं, जिससे जीवन सरल और सुखद हो जाता है। यही सब चीजें उनके वनवास को भी राजमहल जैसा आनंदमय बना देती हैं। लक्ष्मण का यह सरल-सुलभ आचरण यहाँ की खुशियों को दुगुना कर देता है। सीता जी कहती हैं कि इन घटनाओं का वर्णन और स्मरण ही इतना आनंददायक होता है कि उनका वनवास भी राजमहल जैसा लगता है।
विशेष –
जीवन में स्नेह, प्रेम और आत्मीयता ही सबसे बड़ा संबल होते हैं।
छोटे-छोटे उपहार और देखभाल भी जीवन में बड़ी खुशी ला सकते हैं।
जब प्रियजन और संत-महात्मा जीवन में आते हैं, तो वे उसे और भी आनंदमय बना देते हैं।
आत्मनिर्भरता और संतोष से जीवन की कठिन परिस्थितियाँ भी मधुर बन सकती हैं।
खड़ी बोली कविता का सहज और सुंदर रूप इन पंक्तियों में मौजूद है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग है।
05
किसलय-कर स्वागत हेतु हिला करते हैं,
मृदु मनोभाव – सम सुमन खिला करते हैं।
डाली में नव फल नित्य मिला करते हैं
तृण तृण पर मुक्ता भार झिला करते हैं।
निधि खोले दिखला रही प्रकृति निज माया,
मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया।
शब्दार्थ –
किसलय-कर – कोमल नई पत्तियों के हाथ (यहाँ पत्तियों को हाथ के समान बताया गया है)
स्वागत हेतु हिला करते हैं – अतिथियों का स्वागत करने के लिए हलचल करते हैं (यानि पत्तियाँ हवा में हिलती हैं)
मृदु मनोभाव – कोमल भावनाएँ, प्रेम और सौम्यता
सम सुमन – फूलों के समान
खिला करते हैं – मुस्कुराते हैं, खिलते हैं (प्रेम और उल्लास का प्रतीक)
डाली में नव फल – शाखाओं पर नए-नए फल
नित्य मिला करते हैं – प्रतिदिन प्राप्त होते हैं
तृण तृण पर – हर घास के तिनके पर
मुक्ता भार – मोतियों का भार (यहाँ ओस की बूंदों के लिए प्रयोग किया गया है)
झिला करते हैं – चमकते हैं, झलकते हैं
निधि – खजाना, संपत्ति
खोले दिखला रही – अपने खजाने को प्रकट कर रही है
प्रकृति निज माया – प्रकृति अपनी अद्भुत सुंदरता और शक्ति को दिखा रही है
संदर्भ और प्रसंग –
उपर्युक्त कवितांश मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य ‘साकेत’ के अष्टम सर्ग से लिया गया है। राम-सीता और लक्ष्मण को अयोध्या लौटा लेने के लिए अयोध्या के निवासी चित्रकूट पहुँचे हुए हैं। कवि ने सीता के माध्यम से चित्रकूट की प्राकृतिक सुषमा का चित्रण किया है।
व्याख्या –
इन पंक्तियों में सीता जी चित्रकूट की रमणीय शोभा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि यहाँ नए और कोमल पत्ते स्वागत हेतु अपने हाथ हिलाया करते हैं। मनुष्य के कोमल मनोभाव प्रकट करने के लिए मानो फूल खिला करते हैं। चित्रकूट फलों से लदा हुआ है। इसलिए डाली में नित्य नए फल भरे रहते हैं। तृण-तृण पर ओस की बूँदें मुक्ता सदृश झिलमिलाते रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने अपना अमाप्य रत्न भंडार उन्मुक्त कर दिया है। वह अपनी माया से जड़-चेतन सबको मंत्रमुग्ध किए जा रही है। इसीलिए मुझे अपनी कुटिया में किसी तरह का अभाव नहीं महसूस होता बल्कि राजभवन जैसा ही आनंद मिलता है।
विशेष –
उपर्युक्त अंश की पहली पंक्ति में कवि ने मानवीकरण का सुंदर प्रयोग किया है।
प्रकृति की नैसर्गिक सुषमा का मनोरम चित्रण हुआ है।
मानव और प्रकृति के अभिन्न संबंध को भी इस पद से जाना जा सकता है।
सीता के पारंपरिक देवी रूप की बजाय उसे मनुष्य रूप में प्रस्तुत किया गया है।
खड़ी बोली कविता का सहज और सुंदर रूप इन पंक्तियों में मौजूद है।
किसलय, स्वागत, मृदु, तृण, मुक्ता, निधि, प्रकृति जैसे तत्सम शब्दों का प्रयोग है।
06
कहता है कौन कि भाग्य ठगा है मेरा?
वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा।
कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा,
वन में ही तो गार्हस्थ‘ जगा है मेरा।
वह वधु जानकी बनी आज यह जाया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
शब्दार्थ –
कहता है कौन – कौन कहता है
भाग्य ठगा है मेरा – मेरा भाग्य धोखा खा गया है (असफल या दुर्भाग्यशाली हूँ)
वह सुना हुआ भय – पहले से सुना गया डर
दूर भगा है मेरा – समाप्त हो गया, डर चला गया
कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा – अब मेरे हाथ से कुछ सार्थक कार्य हुआ है
वन में ही – जंगल में ही
गार्हस्थ’ – गृहस्थ जीवन, परिवारिक जीवन
जगा है मेरा – जाग्रत हुआ है, स्थापित हुआ है
वधु जानकी – पत्नी सीता (जानकी)
बनी आज यह जाया – अब माता बन चुकी हैं
संदर्भ और प्रसंग –
प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिलीशरण गुप्त की रचना ‘साकेत’ के अष्टम सर्ग से ली गई हैं। ‘साकेत’ में गुप्तजी ने रामकथा को आधार बनाया है। इस कथा के माध्यम से वह आधुनिक युग की जरूरतों, परिस्थितियों और समस्याओं की अभिव्यक्ति और समाधान प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि राम-सीता और लक्ष्मण को अयोध्या लौटा लेने के लिए अयोध्या के निवासी भरत सहित चित्रकूट पहुँचे हुए थे तब राजरानी सीता को स्वावलंबी रूप में प्रस्तुत किया गया है। महलों के सुख साधनों को छोड़कर वन में आई सीता अपनी स्थिति से प्रसन्न और संतुष्ट है। राजभवन के भोग विलास की तुलना में वन का यह स्वच्छंद और प्रद्भत जीवन उसे भाने लगा है इसीलिए वह कहती हैं-
व्याख्या –
इस अंश में कवि ने माता सीता की विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मबल और संतोष को व्यक्त किया है। सीता भाग्य को दोष देने के बजाय अपने श्रम और आत्मनिर्भरता पर विश्वास करती हैं। वे बताती हैं कि उनके जीवन में वास्तविक समृद्धि और संतोष वन में ही प्राप्त हुआ है। माता सीता कहती हैं कि पहले जो भय था कि वन में जीवन कितना कष्टमय होगा? अब वह है ही नहीं। अब मैंने अपने हाथों से काम करना सीख लिया है। वन में ही मैंने अपने गृहस्थ जीवन को सही मायनों में स्थापित किया है। राजरानी सीता का अब असल में वधू जानकी के रूप में जन्म हुआ है। यही कारण है कि उनकी साधारण कुटिया उन्हें राजमहल से भी अधिक प्रिय लगती है।
विशेष –
भाग्य को दोष देने के बजाय, अपने कर्म और मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए।
भय केवल एक भ्रम है, जो आत्मबल से समाप्त हो सकता है।
सच्ची समृद्धि बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि गृहस्थ जीवन के संतोष और प्रेम में होती है।
विपरीत परिस्थितियों में भी, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है।
07
फल-फूलों से हैं लदी डालियाँ मेरी,
वे हरी पत्तलें, भरी थालियाँ मेरी।
मुनि बालाएँ हैं यहाँ आलियाँ मेरी,
तटिनी की लहरें और तालियाँ मेरी।
क्रीड़ा – सामग्री बनी स्वयं निज छाया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
शब्दार्थ –
फल-फूलों से हैं लदी डालियाँ मेरी – मेरे आश्रम के पेड़ फलों और फूलों से भरे हुए हैं।
हरी पत्तलें – भोजन परोसने के लिए उपयोग की जाने वाली हरी पत्तियाँ (प्राकृतिक थालियाँ)
भरी थालियाँ मेरी – पत्तों से बनी थालियों में पर्याप्त भोजन उपलब्ध है।
मुनि बालाएँ – यहाँ रहने वाली तपस्विनी कन्याएँ (संन्यासी मुनियों की सेविकाएँ)
आलियाँ मेरी – आश्रम में आने-जाने वाली सहचरिणियाँ
तटिनी की लहरें – नदी की लहरें (जो मधुर संगीत की तरह प्रतीत होती हैं)
तालियाँ मेरी – नदी की लहरों का शोर तालियों के समान लगता है।
क्रीड़ा-सामग्री – खेल-कूद और आनंद के लिए उपलब्ध साधन
बनी स्वयं निज छाया – वृक्षों की छाया ही मनोरंजन का साधन बन गई है।
संदर्भ और प्रसंग –
प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिलीशरण गुप्त की रचना ‘साकेत’ के अष्टम सर्ग से ली गई हैं। ‘साकेत’ में गुप्तजी ने रामकथा को आधार बनाया है। इस कथा के माध्यम से वह आधुनिक युग की जरूरतों, परिस्थितियों और समस्याओं की अभिव्यक्ति और समाधान प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि राम-सीता और लक्ष्मण को अयोध्या लौटा लेने के लिए अयोध्या के निवासी भरत सहित चित्रकूट पहुँचे हुए थे तब राजरानी सीता को स्वावलंबी रूप में प्रस्तुत किया गया है। महलों के सुख साधनों को छोड़कर वन में आई सीता अपनी स्थिति से प्रसन्न और संतुष्ट है। राजभवन के भोग विलास की तुलना में वन का यह स्वच्छंद और प्रद्भत जीवन उसे भाने लगा है इसीलिए वह कहती हैं-
व्याख्या –
इन पंक्तियों में सीता जी अपने वनवास की प्राकृतिक संपन्नता और सौंदर्य का चित्रण कर रही हैं। वे बताती हैं कि उनके आश्रम में हर चीज़ सहज रूप से उपलब्ध है, जिससे उन्हें किसी भौतिक सुख-साधन की कमी महसूस नहीं होती। प्रकृति स्वयं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिससे उनकी कुटिया किसी राजमहल से कम नहीं लगती। उनके वनवास स्थल पर पेड़ फलों और फूलों से भरे हुए हैं, जिससे उन्हें भोजन की कोई कमी नहीं है अर्थात् यहाँ प्राकृतिक संपन्नता है। भोजन के लिए हरी पत्तलें उपलब्ध हैं, जो किसी भव्य थाली से कम नहीं लगतीं। संतों और प्रकृति की संगति के अतिरिक्त आश्रम में रहने वाली संन्यासी बालाएँ और नदी की लहरें उनका साथ देती हैं, जिससे जीवन संतोषप्रद लगता है। नदी की लहरें तालियों की तरह प्रतीत होती हैं, जो आनंद का अनुभव कराती हैं। खेल और विश्राम के साधन स्वरूप वृक्षों की छाया ही मनोरंजन और विश्राम का स्थान बन गई है।
विशेष –
संतोष और सरलता से जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है।
प्राकृतिक संसाधन भी उतने ही मूल्यवान हैं जितने भौतिक सुख-साधन।
साधारण जीवन में भी आनंद की अपार संभावनाएँ होती हैं, यदि हम संतुष्ट और प्रसन्न रहें।
प्रकृति ही सच्चा वैभव प्रदान करती है, जिससे साधारण कुटिया भी राजमहल जैसा प्रतीत होता है।
08
मैं पली पक्षिण विपिन कुंज – पिंजर की,
आती है कोटर-सदृश मुझे सुध घर की।
मृदु-तीक्ष्ण वेदना एक एक अन्तर की,
बन जाती है कल गीति समय के स्वर की।
कब उसे छेड़ यह कण्ठ यहाँ न अघाया?
मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया।
शब्दार्थ –
पली – पली-बढ़ी
पक्षिण – पक्षी (यहाँ स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है)
विपिन – जंगल, वन
कुंज – वृक्षों और लताओं से घिरा स्थान
पिंजर – पिंजरा
कोटर – पेड़ में बना हुआ खोखला स्थान, पक्षियों का प्राकृतिक घर
सुध – याद, स्मरण
मृदु-तीक्ष्ण वेदना – कोमल और तीव्र पीड़ा
अन्तर – हृदय, मन
कल गीति – मधुर गीत
समय के स्वर – समय के अनुसार उत्पन्न होने वाली ध्वनि
छेड़ – गाना, गूंजना
कण्ठ – गला, स्वर
अघाया – तृप्त हुआ, संतुष्ट हुआ
संदर्भ और प्रसंग –
प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिलीशरण गुप्त की रचना ‘साकेत’ के अष्टम सर्ग से ली गई हैं। ‘साकेत’ में गुप्तजी ने रामकथा को आधार बनाया है। इस कथा के माध्यम से वह आधुनिक युग की जरूरतों, परिस्थितियों और समस्याओं की अभिव्यक्ति और समाधान प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि राम-सीता और लक्ष्मण को अयोध्या लौटा लेने के लिए अयोध्या के निवासी भरत सहित चित्रकूट पहुँचे हुए थे तब राजरानी सीता को स्वावलंबी रूप में प्रस्तुत किया गया है। महलों के सुख साधनों को छोड़कर वन में आई सीता अपनी स्थिति से प्रसन्न और संतुष्ट है। राजभवन के भोग विलास की तुलना में वन का यह स्वच्छंद और प्रद्भत जीवन उसे भाने लगा है इसीलिए वह कहती हैं-
व्याख्या –
इन पंक्तियों में सीता स्वयं को एक पक्षिणी के रूप में देखती हैं, जो पहले महल (अयोध्या) में रहती थीं लेकिन अब जंगल (वनवास) में हैं। जिस तरह एक पक्षी जंगल के वृक्षों के कोटर में निवास करते हुए अपने पुराने घर (पिंजरे या महल) को याद करता है, उसी तरह सीता भी अयोध्या को याद करती हैं। सुख और दुख की स्मृतियाँ समय के साथ मिलकर उनके जीवन का संगीत बन जाती हैं। वे अपने हृदय की भावनाओं को गीतों के माध्यम से व्यक्त करती हैं और इससे उनका मन तृप्त होता है। इस आत्मसंतोष के कारण ही उनकी साधारण कुटिया भी उन्हें राजमहल के समान प्रतीत होती है।
विशेष –
भले ही परिस्थितियाँ बदल जाएँ, लेकिन स्मृतियाँ और भावनाएँ जीवन को संगीतमय बना सकती हैं।
जीवन के सुख-दुख को स्वीकार कर लेने से आत्मसंतोष प्राप्त होता है।
संगीत और अभिव्यक्ति से पीड़ा भी मधुरता में बदल जाती है।
जहाँ आत्मसंतोष और आनंद होता है, वहीं सच्चा वैभव होता है, चाहे वह कुटिया ही क्यों न हो।
09
गुरुजन-परिजन सब धन्य ध्येय हैं मेरे,
औषधियों के गुण-विगुण ज्ञेय हैं मेरे
वन-देव-देवियाँ आतिथेय हैं मेरे,
प्रिय संग यहाँ सब प्रेय श्रेय है मेरे।
मेरे पीछे ध्रुव धर्म स्वयं ही धाया,
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
शब्दार्थ –
गुरुजन-परिजन – शिक्षक और परिवारजन
धन्य – महान, पूजनीय, प्रशंसनीय
ध्येय – लक्ष्य, उद्देश्य
औषधियों के गुण-विगुण – औषधियों के लाभ और हानियों का ज्ञान
ज्ञेय – जानने योग्य, समझने योग्य
वन-देव-देवियाँ – जंगल में वास करने वाले देवता और देवियाँ
आतिथेय – आतिथ्य करने वाले, स्वागत करने वाले
प्रिय संग – प्रियजनों का साथ
प्रेय – प्रिय और मनभावन वस्तुएँ
श्रेय – शुभ और हितकारी चीजें
ध्रुव धर्म – अटल और शाश्वत धर्म
स्वयं ही धाया – स्वयं ही मेरे पीछे चला आया
संदर्भ और प्रसंग –
प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिलीशरण गुप्त की रचना ‘साकेत’ के अष्टम सर्ग से ली गई हैं। ‘साकेत’ में गुप्तजी ने रामकथा को आधार बनाया है। इस कथा के माध्यम से वह आधुनिक युग की जरूरतों, परिस्थितियों और समस्याओं की अभिव्यक्ति और समाधान प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि राम-सीता और लक्ष्मण को अयोध्या लौटा लेने के लिए अयोध्या के निवासी भरत सहित चित्रकूट पहुँचे हुए थे तब राजरानी सीता को स्वावलंबी रूप में प्रस्तुत किया गया है। महलों के सुख साधनों को छोड़कर वन में आई सीता अपनी स्थिति से प्रसन्न और संतुष्ट है। राजभवन के भोग विलास की तुलना में वन का यह स्वच्छंद और प्रद्भत जीवन उसे भाने लगा है इसीलिए वह कहती हैं-
व्याख्या –
चित्रकूट की शोभा और संपदा से सीता जी गद्गद् हैं। सीता अपने गुरुजनों और आत्मीय लोगों को धन्य समझती हैं जो उनके ध्येय में हैं। औषधीय गुणों से परिपूर्ण पेड़-पौधों को सीता पहचान चुकी हैं। वन के देवी-देवताओं की आतिथेयता से वे परम प्रसन्न हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सीता अपने पति के साथ हैं। इसलिए यहाँ उन्हें सब कुछ प्रिय और श्रेष्ठ लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि चित्त प्रसन्न हो तो मनुष्य को दुख कष्ट भी नहीं सालते। उसे सब कुछ प्रेममय और आनंदमय प्रतीत होता है। चित्रकूट के सघन वन में भी सीता अपने पति के साथ होने के कारण न केवल वह संतुष्ट हैं बल्कि परम प्रसन्न भी हैं। श्रीराम के साथ रहने का आशय है कि अटल धर्म भी उन्हीं का पीछा कर रहा है। इसीलिए सीता को धर्म-अधर्म की चिंता में चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? सीता कहती हैं अर्थात् कवि कहते हैं कि उन्हें अपनी कुटिया में किसी तरह का अभाव नहीं महसूस होता बल्कि राजभवन जैसा ही आनंद मिलता है।
विशेष –
इस पद में चित्रकूट पर्वत के औषधीय गुणवाले वृक्षों और लता – गुल्मों की प्रशंसा की गई है।
सीता के पारंपरिक देवी रूप की बजाय उसे मनुष्य रूप में प्रस्तुत किया गया है।
भारतीय परंपरा में विश्वास है कि पति के साथ पत्नी कहीं भी रहे तो उसे परम संतोष की प्राप्ति होती है।
खड़ी बोली का सहज और स्वाभाविक प्रयोग मिलता है।
लोकविश्वास है कि वन में रहने वाले सभी प्राणियों की रक्षा वनदेवी और वनदेवता करते हैं।
10
नाचो मयूर, नाचो कपोत के जोड़े।
नाचो कुरंग, तुम लो उड़ान के तोड़े।
गाओ दिवि, चातक चटक, भृंग भय छोड़े
वैदेही के वनवास वर्ष हैं थोड़े।
तितली, तूने यह कहाँ चित्रपट पाया?
मेरी कुटिया में राज-भवन मन भाया।
शब्दार्थ –
नाचो मयूर – नाचो मोर (यहाँ उल्लास और खुशी व्यक्त करने का संकेत)
नाचो कपोत के जोड़े – कबूतरों के जोड़े भी नृत्य करें (प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक)
नाचो कुरंग – हरिण (हिरण) नाचें
उड़ान के तोड़े – समूह में उड़ना
गाओ दिवि – गाओ, आकाश में रहने वाले पक्षियों (दिवि = स्वर्ग या आकाश)
चातक – एक विशेष पक्षी जो प्यासा होने पर केवल स्वाति नक्षत्र की बूंदों का इंतजार करता है
चटक – एक प्रकार का पक्षी (तोता या चिड़िया)
भृंग – भौंरा (जो फूलों के आसपास गूंजता रहता है)
भय छोड़े – डर को छोड़कर आनंदित हो
वैदेही – सीता माता (जनक की पुत्री होने के कारण ‘वैदेही’ कहा जाता है)
वनवास वर्ष हैं थोड़े – वन में बिताने के लिए वर्ष अब अधिक शेष नहीं हैं, वनवास जल्द समाप्त होगा
तितली – रंग-बिरंगी उड़ने वाली सुंदर कीट
चित्रपट – चित्रित पर्दा, रंगीन दृश्य (यहाँ प्रकृति की सुंदरता को चित्रपट कहा गया है)
पाया – प्राप्त किया, देखा
व्याख्या –
इस काव्यांश में माता सीता ने वन की प्राकृतिक सुंदरता और उसमें रहने वाले जीवों के उल्लासपूर्ण वातावरण का चित्रण किया है। माता सीता कहती हैं कि वन का वातावरण वन्यजीवों और पक्षियों को नृत्य और गायन करके आनंद मनाने के लिए प्रेरित करता है, स्वयं माता सीता भी यही चाहती हैं कि सभी सुखी और प्रसन्नवदन रहे क्योंकि माता सीता का वनवास अधिक समय तक नहीं रहेगा। सीता जी वन्य जीवों जैसे – मोर, कबूतर, हिरण, चातक, भौंरों से यही निवेदन करती हैं कि वे अपने-अपने तरीके से नृत्य और गान करें। यहाँ प्रकृति और उसके जीव-जंतु भी सीता के सुख-दुख के सहभागी प्रतीत होते हैं इसलिए सीता जी ने प्रकृति और उसके जीव-जंतुओं को उत्सव मनाने के लिए प्रेरित किया है। तितली की सुंदरता देखकर सीता मैया आश्चर्य करती हैं कि उसे इतनी अद्भुत प्राकृतिक छटा कहाँ मिली। यह सब दृश्य उनकी कुटिया को राजमहल से भी अधिक सुंदर बना देता है।
विशेष –
प्रकृति और उसके जीव-जंतु भी मानव के सुख-दुख के सहभागी होते हैं।
कठिन समय (वनवास) भी आनंदपूर्वक व्यतीत किया जा सकता है, यदि मन में संतोष और आशा हो।
प्राकृतिक सौंदर्य राजमहल से भी अधिक मनोहारी हो सकता है।
जीवन में हर परिस्थिति में खुशी ढूँढनी चाहिए, क्योंकि दुख भी अस्थायी होते हैं।
11
आओ कलापि निज चन्द्रकला दिखलाओ
कुछ मुझसे सीखो और मुझे सिखलाओ।
गाओ पिक, मैं अनुकरण करूँ, तुम गाओ,
स्वर खींच तनिक यों उसे घुमाते जाओ।
शुक पढ़ो – मधुर फल प्रथम तुम्हीं ने खाया,
मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया।
शब्दार्थ –
आओ कलापि – आओ, कोयल (कलापि = कोयल का दूसरा नाम)
निज चन्द्रकला दिखलाओ – अपनी सुंदर कलात्मकता (गायन या चातुर्य) दिखाओ
कुछ मुझसे सीखो और मुझे सिखलाओ – परस्पर ज्ञान साझा करें
गाओ पिक – गाओ कोयल (पिक = कोयल)
मैं अनुकरण करूँ – मैं तुम्हारी नकल करूँगा, तुम्हारा अनुसरण करूँगा
स्वर खींच तनिक – स्वर को थोड़ा खींचो (लंबा करो)
यों उसे घुमाते जाओ – स्वर को मधुर तरीके से मोड़ते जाओ
शुक पढ़ो – तोते, तुम पाठ पढ़ो (शुक = तोता, जो अक्सर सीखकर बोलता है)
मधुर फल – मीठा फल
प्रथम तुम्हीं ने खाया – पहले तुमने इसका स्वाद लिया
संदर्भ और प्रसंग –
प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिलीशरण गुप्त की रचना ‘साकेत’ के अष्टम सर्ग से ली गई हैं। ‘साकेत’ में गुप्तजी ने रामकथा को आधार बनाया है। इस कथा के माध्यम से वह आधुनिक युग की जरूरतों, परिस्थितियों और समस्याओं की अभिव्यक्ति और समाधान प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि राम-सीता और लक्ष्मण को अयोध्या लौटा लेने के लिए अयोध्या के निवासी भरत सहित चित्रकूट पहुँचे हुए थे तब राजरानी सीता को स्वावलंबी रूप में प्रस्तुत किया गया है। महलों के सुख साधनों को छोड़कर वन में आई सीता अपनी स्थिति से प्रसन्न और संतुष्ट है। राजभवन के भोग विलास की तुलना में वन का यह स्वच्छंद और प्रद्भत जीवन उसे भाने लगा है इसीलिए वह कहती हैं-क्या
व्याख्या –
इन पंक्तियों में सीता जी प्रकृति के पक्षियों को आमंत्रित कर रही हैं कि वे अपनी कला का प्रदर्शन करें और आपसी सीख-साझा करें। सीता जी कोयल से कहती हैं कि वह अपनी सुंदरता और मधुर गायन का प्रदर्शन करे। सीता जी कोयल से गाना सीखना चाहती हैं और उनका अनुकरण करना चाहती हैं, सीता जी उन्हें स्वर को कितने लंबे तक खींचना है और कब तथा कहाँ से मोड़ना है यह भी बतलाना चाहती हैं। वे तोते को सीखने और पढ़ने के लिए कहती हैं, क्योंकि तोते को दोहराने की क्षमता के लिए जाना जाता है। मीठे फलों का पहला स्वाद तोते को मिलता है, जैसे ज्ञान और अनुभव सबसे पहले वे प्राप्त करते हैं जो जिज्ञासु होते हैं। इस आत्मीय और ज्ञानवर्धक वातावरण में उनकी साधारण कुटिया भी राजमहल के समान आनंददायक प्रतीत होती है।
विशेष –
सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जीवन को सुंदर और सार्थक बनाती है।
प्रकृति से भी कला और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
आत्मिक संतोष और ज्ञान का वातावरण राजमहल से भी श्रेष्ठ होता है।
प्रकृति के साथ संवाद और आनंद मनुष्य के जीवन को संपूर्ण बना देता है।