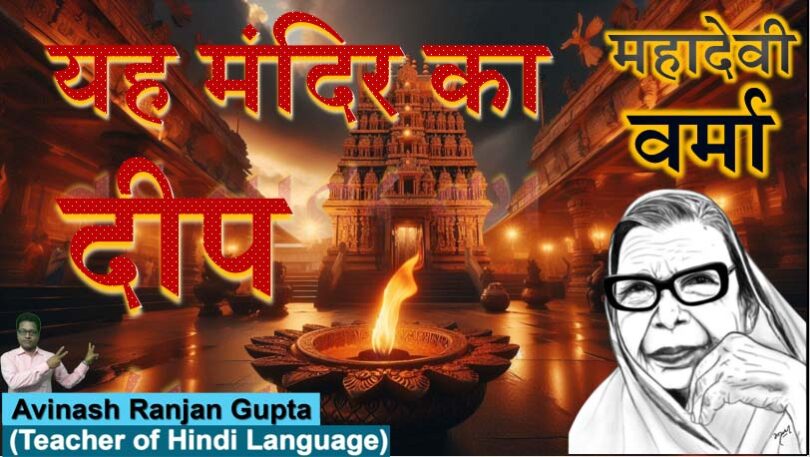यह मंदिर का दीप
यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो!
रजत शंख-घड़ियाल स्वर्ण वंशी-वीणा-स्वर,
गए आरती वेला को शत-शत लय से भर,
जब था कल कंठों का मेला,
विहँसे उपल तिमिर था खेला,
अब मंदिर में इष्ट अकेला,
इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो!
चरणों से चिह्नित अलिंद की भूमि सुनहली,
प्रणत शिरों के अंक लिए चन्दन की दहली,
झरे सुमन बिखरे अक्षत सित,
धूप-अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित
तम में सब होंगे अंतर्हित
सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो!
पल के मनके फेर पुजारी विश्व सो गया,
प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया
साँसों की समाधि-सा जीवन,
मसि-सागर का पंथ गया बन
रुका मुखर कण-कण का स्पंदन,
इस ज्वाला में प्राण-रूप फिर से ढलने दो!
झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी,
आज पुजारी बने, ज्योति का यह लघु प्रहरी,
जब तक लौटे दिन की हलचल,
तब तक यह जागेगा प्रतिपल,
रेखाओं में भर आभा-जल
दूत साँझ का इसे प्रभाती तक चलने दो!
महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी पढ़ाई-लिखाई इंदौर और इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग महिला विद्यापीठ में वे प्रधानाचार्या के पद पर कार्यरत रहीं। उनकी मृत्यु 1987 में हुई।
महादेवी वर्मा ने कविता के अलावा सशक्त गद्य भी लिखा था। उनकी गद्य रचनाएँ भाषा और विचार की दृष्टि से अत्यंत परिपक्व मानी जाती हैं। ‘शृंखला की कड़ियाँ’ के लेखों में उन्होंने स्त्री-मुक्ति के प्रश्नों को जिस स्तर पर उठाया था वह आश्चर्यजनक है। मैनेजर पाण्डेय ने इस पुस्तक को रेखांकित करते हुए लिखा है कि सिमोन द बोउवार की पुस्तक ‘द सेकेण्ड सेक्स’ के प्रकाशन से भी पहले महादेवी की यह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी और इसके लेख तो और भी पहले प्रकाशित हो चुके थे। महादेवी वर्मा ने ‘चाँद’ पत्रिका के ‘विदुषी अंक’ का सम्पादन 1935 में किया था। यह अंक हिंदी में हुए स्त्री-विमर्श की परंपरा में विशेष महत्त्व रखता है। यह अंक उस जमाने में आया था जब इस तरह के विषय पर सोच-विचार की प्रवृत्ति आम नहीं थी। महादेवी का वैचारिक गद्य लेखन महत्त्वपूर्ण है।
छायावाद और रहस्यवाद की कवि के रूप में महादेवी वर्मा का स्थान अक्षुण्ण है। उनके पाँच काव्य-संग्रहों की कविताओं में छायावादी-रहस्यवादी प्रवृत्तियाँ तो हैं ही, उनमें स्त्री की पीड़ा और मुक्ति के प्रसंग भरे पड़े हैं। इनमें पीड़ा का विवरण भी व्यक्तित्व की दृढ़ता को व्यक्त करने के लिए किया गया है। इनमें प्रेम और प्रेमी का जिक्र भी मुक्ति के प्रतीक के रूप में किया गया है। महादेवी कोरी भावुकता की कविताएँ नहीं लिखती हैं। उनकी कविताओं में वैचारिक दृढ़ता हमेशा बनी रही।
काव्य-कृतियाँ
नीहार (1930), रश्मि (1932), नीरजा (1935), सांध्यगीत (1936), दीपशिखा (1942), हिमालय (1963), सप्तपर्णा (अनूदित – 1966), प्रथम आयाम (1982), अग्निरेखा (1990)
गद्य-कृतियाँ
अतीत के चलचित्र (रेखाचित्र – 1941), शृंखला की कड़ियाँ (नारी-विषयक सामाजिक निबंध – 1942), स्मृति की रेखाएँ (रेखाचित्र – 1943), पथ के साथी (संस्मरण – 1956), क्षणदा (ललित निबंध – 1956), साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध (आलोचनात्मक – 1960), संकल्पिता (आलोचनात्मक – 1969), मेरा परिवार (पशु-पक्षियों के संस्मरण 1971), चिंतन के क्षण (1986)
संकलन
यामा (नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत का संग्रह / 1936), संधिनी (कविता-संग्रह / 1964), स्मृतिचित्र (गद्य-संग्रह – 1966), महादेवी साहित्य (भाग – 1 – 1969), महादेवी साहित्य (भाग – 2 – 1970), महादेवी साहित्य (भाग – 31970), गीतपर्व (कविता-संग्रह – 1970), स्मारिका (1971), परिक्रमा (कविता संग्रह – 1974), सम्भाषण (कविता-संग्रह 1975), मेरे प्रिय निबंध (निबंध – संग्रह – 1981), आत्मिका (कविता-संग्रह – 1983), नीलाम्बरा (कविता-संग्रह – 1983), दीपगीत (कविता-संग्रह – 1983)
यह मंदिर का दीप महादेवी वर्मा द्वारा सन् 1942 में लिखी गई थी जो इनकी काव्य संग्रह ‘दीप-शिखा’ में संग्रहित है। यह कविता एक मंदिर के दीप (दीपक) के माध्यम से भक्ति, शांति, और आस्था की भावना को प्रकट करती है। इसका मुख्य संदेश यह है कि भले ही आरती और पूजा की ध्वनियाँ समाप्त हो गई हों, दीपक की लौ जलती रहनी चाहिए, क्योंकि यह ईश्वर की उपस्थिति और साधना का प्रतीक है।
‘यह मंदिर का दीप’ कविता का उद्देश्य यह है कि हमें अपने काम को संकल्प की भावना के साथ करना चाहिए। प्रचार या प्रशंसा के लिए किया गया काम साधना की कोटि में नहीं आता है। कवयित्री कहती हैं कि समर्पित साधकों के कारण ही यह दुनिया संकल्प पूरे कर पाती है। सरल शब्दों में हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ एक और संदेश इस कविता में निहित है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं हमें उन्हें किसी भी तरह से कोई हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। यह मानवता के नियमों के विरुद्ध है। समाज में जब कोई सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश में लगा हुआ है तो हमें उसका सहयोग करते हुए उसके लक्ष्य को पाने में सहायता प्रदान करनी चाहिए परंतु लोग ईर्ष्या के कारण उसके रास्ते में रोड़े डालते रहते हैं। महादेवी जी की यह निजी अनुभूति भी रही है और अपने निजी अनुभवों से प्रेरित होकर उन्होंने इस कविता की रचना की है जिसमें लक्ष्य साधने वाले को मंदिर के दीप के साथ तुलना करके उसे पवित्रता की उत्तम कोटि तक पहुँचा दिया है।
यह मंदिर का दीप
01
यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो!
शब्दार्थ –
मंदिर – देवालय
दीप – दीया
नीरव जलने दो – खामोशी से अपना काम करने दो
प्रसंग –
‘यह मंदिर का दीप’ कविता में महादेवी वर्मा ने कहना चाहा है कि साधक को अपनी साधना करने दो! साधक प्रचार के लिए साधना नहीं करता है। वह किसी को दिखाने के लिए या प्रशंसा के लिए साधना नहीं करता है। वह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए साधना करता है। इस कविता में मंदिर के दीप को साधक का प्रतीक बनाया गया है।
व्याख्या –
महादेवी वर्मा कहती हैं कि यह मंदिर का दीपक है। इसे चुपचाप जलने दिया जाए। यह दीपक एक संकल्प के साथ जल रहा है। इसका संकल्प यह है कि मंदिर का इष्ट देव अँधेरे में न रहे। वह पूरी रात जलकर अपने देवता के घर में प्रकाश बनाए रखना चाहता है। इसका लक्षणार्थ यह है कि जीवन में जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए उद्यम कर रहा है उसे उद्यम करने दो। उसके रास्ते में किसी भी प्रकार की विघ्न-बाधा ईर्ष्यावश या इरादतन मत पैदा करो। मनुष्य ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है, वह इसे अपने कर्मों के माध्यम से प्रमाणित करना चाहता है और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता है। इसलिए उसे ऐसा करने दो।
02
रजत शंख-घड़ियाल स्वर्ण वंशी-वीणा-स्वर,
गए आरती वेला को शत-शत लय से भर,
जब था कल कंठों का मेला,
विहँसे उपल तिमिर था खेला,
अब मंदिर में इष्ट अकेला,
इसे अजिर का शून्य गलाने को गलने दो!
शब्दार्थ –
रजत शंख-घड़ियाल – चाँदी के रंग के शंख और घड़ियाल (पूजा में प्रयुक्त एक वाद्य)
स्वर्ण वंशी-वीणा-स्वर – सोने की तरह मोहक बाँसुरी और वीणा के स्वर,
आरती वेला – देवता की आरती करने का समय,
कल कंठों का मेला – कल कंठों का मेला सुंदर कंठ स्वरों से गायी गई आरती का सामूहिक स्वर,
विहँसे उपल – मानो मंदिर निर्माण में प्रयुक्त पत्थर भी हँस रहे हों
तिमिर – अंधकार
इष्ट अकेला – (मंदिर में) भगवान अकेले हैं
अजिर का शून्य – आँगन का सूनापन
गलाने को गलने दो – सूनेपन को समाप्त करने के लिए इस दीप को जल-जल कर गलने दो
प्रसंग –
‘यह मंदिर का दीप’ कविता में महादेवी वर्मा ने कहना चाहा है कि साधक को अपनी साधना करने दो! साधक प्रचार के लिए साधना नहीं करता है। वह किसी को दिखाने के लिए या प्रशंसा के लिए साधना नहीं करता है। वह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए साधना करता है। इस कविता में मंदिर के दीप को साधक का प्रतीक बनाया गया है।
व्याख्या –
महादेवी मंदिर की दिनचर्या की चर्चा करती हुई कहती हैं कि चाँदी के रंग के शंख- घड़ियाल और सोने के रंग की वंशी, वीणा की मधुर ध्वनियों ने आरती के समय को सैकड़ों लयों से भर दिया था। उस समय सुंदर कंठ ध्वनियों का मानो मेला लगा हुआ था। इन सबके प्रभाव से मानो मंदिर की दीवारों में लगे पत्थर भी विहँस पड़े थे। मंदिर के अँधेरे कोने भी मानो खेलने लगे थे। मगर रात होते ही सब लोग चले गए, मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया। अब मंदिर के इष्ट देवता नितांत अकेले रह गए हैं। मंदिर का आँगन सूना-सूना लग रहा है। महादेवी कहती हैं कि मंदिर के इस सूनेपन को दूर करने के लिए इस दीपक को जल-जलकर गलने दो! यदि यह दीपक नहीं जलेगा तो यह सूनापन दूर नहीं हो सकेगा।
03
चरणों से चिह्नित अलिंद की भूमि सुनहली,
प्रणत शिरों के अंक लिए चन्दन की दहली,
झरे सुमन बिखरे अक्षत सित,
धूप-अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित
तम में सब होंगे अंतर्हित
सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो!
शब्दार्थ –
चरणों से चिह्नित – भक्तों के चरणों के निशान
अलिंद की भूमि – बाहरी दरवाजे के सामने की जगह, मंदिर के बाहरी द्वार के पास की जगह जहाँ श्रद्धालु जूते-चप्पल खोल देते हैं।
प्रणत शिरों के अंक – झुककर मस्तक सटाने से पड़े हुए निशान
दहली – देहरी, चौखट
अक्षत सित – चावल के सफेद दाने जिनका उपयोग पूजा में किया जाता है।
धूप-अर्घ्य – धूप-बत्ती और देवता को समर्पित की जानेवाली पूजन सामग्री
नैवेद्य – देवता को समर्पित की जानेवाली भोज्य वस्तु
अर्चित कथा – पूजा-अर्चना की बातें
प्रसंग –
‘यह मंदिर का दीप’ कविता में महादेवी वर्मा ने कहना चाहा है कि साधक को अपनी साधना करने दो! साधक प्रचार के लिए साधना नहीं करता है। वह किसी को दिखाने के लिए या प्रशंसा के लिए साधना नहीं करता है। वह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए साधना करता है। इस कविता में मंदिर के दीप को साधक का प्रतीक बनाया गया है।
व्याख्या –
कवयित्री पुनः मंदिर की दिनचर्या का जिक्र करते हुए कहती हैं कि दिन भर में न जाने कितने श्रद्धालु मंदिर में आए। उनके कदमों के निशान से अलिंद की भूमि भर गई और सुनहली लगने लगी। श्रद्धालुओं के मस्तक झुकाकर स्पर्श करने से चंदन का चौखट निशानों से भर गया है। दिन भर मंदिर में फूल झरते रहे और अक्षत बिखरते रहे। पूजा-पाठ और भोग चढ़ाई जानेवाली असंख्य वस्तुओं से मंदिर भरा पड़ा था। मगर रात होते ही ये सारी चीजें अँधेरे में डूब जाएँगी। दिन भर में जितने लोगों ने पूजा-अर्चना की है उन सबकी पूजा की कथा इस दीपक की लौ में पलने दो! यदि यह दीपक नहीं जलेगा तो सबकी अर्चित-कथा मानो अँधेरे में डूब जाएगी।
04
पल के मनके फेर पुजारी विश्व सो गया,
प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया
साँसों की समाधि-सा जीवन,
मसि-सागर का पंथ गया बन
रुका मुखर कण-कण का स्पंदन,
इस ज्वाला में प्राण-रूप फिर से ढलने दो!
शब्दार्थ –
पल के मनके – क्षण रूपी मनका (माला के दाने)
प्रतिध्वनि का इतिहास – दिन भर मंदिर में होनेवाली ध्वनियाँ अब रात में अनुगूँज बनकर इतिहास हो गई हैं।
प्रस्तरों – पत्थरों
मसि-सागर – स्याही-रूपी अंधकार का समुद्र
स्पंदन – प्रकंपन
प्रसंग –
‘यह मंदिर का दीप’ कविता में महादेवी वर्मा ने कहना चाहा है कि साधक को अपनी साधना करने दो! साधक प्रचार के लिए साधना नहीं करता है। वह किसी को दिखाने के लिए या प्रशंसा के लिए साधना नहीं करता है। वह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए साधना करता है। इस कविता में मंदिर के दीप को साधक का प्रतीक बनाया गया है।
व्याख्या –
कविता की इन पंक्तियों में एक-एक क्षण मानो माला के दाने की तरह बढ़ता गया और रात आ गई। विश्व-रूपी पुजारी इन दानों को जाप करते हुए बढ़ाता गया और अंत में थककर सो गया। मंदिर में ध्वनियों की गूँज-अनुगूँज मौजूद रहती है। रात होने पर इन सबका ब्योरा मानो पत्थर की दीवारों में खो गया। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि सोए हुए लोगों की साँसों का आना-जाना भर सुनाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जीवन साँसों की समाधि बन गया हो! चारों तरफ अँधेरा ऐसे फैला मानो स्याही का समुद्र फैला हो और उस तक जाने के रास्ते बिखरे हों! रात में सब कुछ इतना खामोश हो गया था मानो कण-कण की गतिशीलता और मुखरता स्थगित हो गई हो! दीपक की ज्वाला में इन सब खोयी हुई चीजों को अपना रूप प्राप्त कर लेने दो और उन सबमें प्राण तत्त्व का संचार हो जाने दो! अगर दीपक नहीं होगा तो ये सारी चीजें अँधेरे में डूब जाएँगी।
05
झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी,
आज पुजारी बने, ज्योति का यह लघु प्रहरी,
जब तक लौटे दिन की हलचल,
तब तक यह जागेगा प्रतिपल,
रेखाओं में भर आभा-जल
दूत साँझ का इसे प्रभाती तक चलने दो!
शब्दार्थ –
झंझा – शोर करती हुई बहनेवाली वायु
दिग्भ्रांत – जिसे दिशाओं का बोध न रह गया हो, भटका हुआ
आभा-जल – प्रकाश-रूपी नमी
दूत साँझ का – ये दीपक संध्या के संदेशवाहक की तरह हैं
प्रभाती – सुबह में गाया जानेवाला गीत
प्रसंग –
‘यह मंदिर का दीप’ कविता में महादेवी वर्मा ने कहना चाहा है कि साधक को अपनी साधना करने दो! साधक प्रचार के लिए साधना नहीं करता है। वह किसी को दिखाने के लिए या प्रशंसा के लिए साधना नहीं करता है। वह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए साधना करता है। इस कविता में मंदिर के दीप को साधक का प्रतीक बनाया गया है।
व्याख्या –
कविता की अंतिम पंक्तियों में रात हो गई है। शोर करती हुई वायु प्रवाहित हो रही है। वह ऐसे बह रही है मानो दिशा भूल गई हो! कभी इधर से कभी उधर से! रात ऐसे सो गई है मानो गहरी बेहोशी में हो। मेरी इच्छा है कि आज यह दीपक पुजारी बन जाए, वह प्रकाश का एक छोटा-सा प्रहरी है। जब तक दिन की हलचल लौट न आए तब तक के लिए यह साधक दीपक जागता रहेगा। यह रात की प्रत्येक अँधेरी रेखा में रोशनी की सजलता को भर देगा। यह दीपक शाम के दूत की तरह है। इसे प्रभाती गाए जाने तक जलने दो!
साधक किसी को दिखाने के लिए या प्रशंसा के लिए साधना नहीं करता है। वह अपने संकल्प को पूरा करने करने के लिए साधना करता है।
इस कविता में मंदिर के दीप को साधक का प्रतीक बनाया गया है।
24 और 16 मात्राओं की पंक्तियों से इस कविता का निर्माण हुआ है।