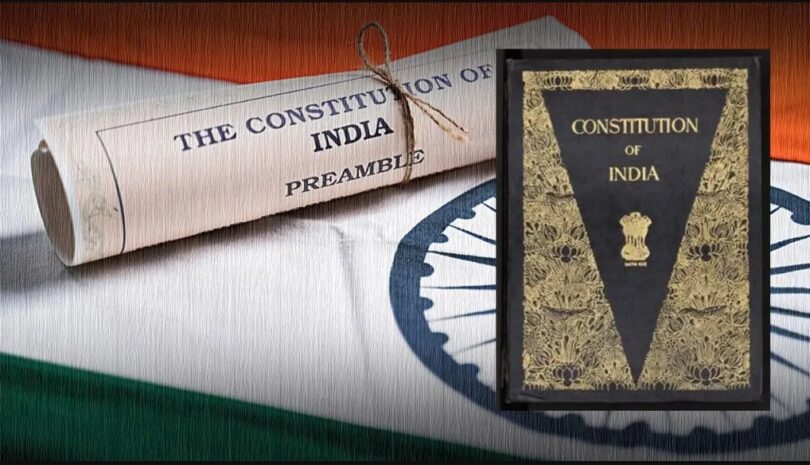अत्यंत प्राचीन काल में एक बहुश्रुत भारतीय कथा के अनुसार जब देश में अराजकता थी, मत्स्य-न्याय का बोलबाला था, बड़ा छोटे पर अत्याचार करता था, किसी की कोई सम्पत्ति या परिवार तक सुरक्षित न था, जनता के विचार- शील लोगों ने इस भय व आतंकपूर्ण स्थिति से तंग आकर उस समय के अत्यंत प्रभावशाली अत्यंत विद्वान और अत्यंत चरित्रवान महान् मनु के पास जाकर निवेदन किया- भगवन् ! इस अराजक अत्याचारपूर्ण स्थिति में हमें बचाइए, जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, प्रति क्षण अपने से बलवान अत्याचारी का भय रहता है। तब मनु ने उनके परामर्श से देश में एक शासक व दंड व्यवस्था स्थापित की और राज्य संस्था का सूत्रपात हुआ। इसके बाद के दीर्घकालीन भारतीय इतिहास में गणतंत्र का वर्णन मिलता है, परंतु समस्त देश के संविधान का निर्माण देश की विशाल जनता के प्रतिनिधियों द्वारा हुआ हो, इसका उल्लेख इतिहास में नहीं मिलता।
संविधान की रूपरेखा
1949 के अंत में स्वतंत्र भारतवर्ष की संविधान सभा ने – जिसमें समस्त देश की जनता के प्रतिनिधि थे— भारत के समस्त ज्ञात इतिहास पहली बार देश का शासन विधान तैयार किया। इस विधान के निर्माण में करीब ढाई वर्ष लगे। प्रत्येक धारा पर खूब विचार मंथन हुआ और उसके बाद 365 धाराओं व 8 अनुसूचियों का महान् संविधान पास हुआ। 26 जनवरी 1950 के दिन उसे देश में लागू किया गया और इसके साथ ही भारत संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया। इस संविधान की संक्षेप से निम्नलिखित रूपरेखा है-
इस देश का नाम भारत है। यह संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है। इन अधिकारों में समानता, धर्म, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, सम्पत्ति और जायदाद की रक्षा तथा शारीरिक स्वतंत्रता आदि सम्मिलित हैं। देश का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति होता है, जो पाँच साल के लिए संसद या विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। शासन-कार्य वह मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। संसद में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रित करता है, फिर उसके परामर्श से शेष मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यह मंत्रिमंडल देश के समस्त शासन व नीति तथा सब खर्चा के लिए संसद के सदस्यों के सामने उत्तरदायी रहता है। संसद का विश्वास न रहने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। यही लोकतंत्र का स्वरूप है।
संसद के दो सदन हैं— लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा के 545 सदस्य 5 वर्षो के लिए बालिग मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। कुछ सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान आदि के प्रतिनिधि रूप में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष बदल जाते हैं। कोई भी कानून या प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी में पेश हो सकता है, परंतु उसके पारित होने के बाद दूसरे सदन में पेश करना पड़ता है। वित्तीय बिल पहले लोकसभा में पेश होते हैं।
राष्ट्रपति के हाथ में कानूनी तौर पर बहुत अधिकार होते हैं। संसद को वह भंग कर सकता है, किसी राज्य का शासन अल्प समय के लिए अपने हाथ में ले सकता है, राज्यों के राज्यपाल व सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्टो के जजों की नियुक्ति करता है, कुछ समय के लिए आर्डिनेंस जारी कर सकता है; किसी पासशुदा विधेयक को रोक सकता है या पुनर्विचारार्थ संसद में भेज सकता है।
राज्यों में राज्यपाल प्रमुख शासक रहता है जो मंत्रिमंडल के सहयोग से शासन करता है। कुछ राज्यों में दो सदन हैं, कुछ में एक। राज्यों के मंत्रिमंडल भी विधान सभा के सदस्यों के प्रति जिम्मेवार होते हैं।
संविधान में निम्नलिखित चार प्रकार के राज्य स्वीकार किए गए थे- ‘क’ श्रेणी के राज्य – असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल (पश्चिम), बम्बई, बिहार, मद्रास और मध्य प्रदेश।
‘ख’ श्रेणी के राज्य- मध्य भारत, राजस्थान, सौराष्ट्र, मैसूर, जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद, तिरुवांकुर कोचीन, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश।
‘ग’ श्रेणी के राज्य – दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, भोपाल, बिलासपुर, मणिपुर।
‘घ’ श्रेणी के राज्य – प्रण्डमान-निकोबार।
भाषा के आधार पर पुनर्गठन के लिए नियत कमीशन ने राज्यों के पुन- गठन की सिफारिशें की। इनके अनुसार कई राज्य परस्पर मिला दिए गए या उनकी सीमाओं में कुछ हेर-फेर किया गया। इस समय भारत में निम्नलिखित राज्य हैं – असम आन्ध्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, पंजाब, बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास, मध्य प्रदेश, मैसूर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तथा अंडमान-निकोबार।
विशेषताएँ
भारतीय संविधान की उपर्युक्त रूपरेखा के बाद इसकी कुछ उन विशेषताओं का उल्लेख कर देना आवश्यक है, जिनके कारण इसका गौरव बहुत अधिक बढ़ गया है।
(1) यह लोकतंत्रात्मक विधान है। भारत में सदियों से चली आती राजतंत्र पद्धति को समाप्त कर दिया गया है और इस दृष्टि से भारत संसार के उन्नततम राष्ट्रों में गिना जाने लगा है। सचाई तो यह है कि लोकतंत्र का पालन जिस खूबी से भारत जैसे विशाल देश में हो रहा है, उसका उदाहरण अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। प्रथम चुनाव में यहाँ 94 करोड़ मतदाताओं की सूची बनाई गई थी। अमेरिका, रूस व ग्रेट ब्रिटेन की कुल जनसंख्या ही इसके बराबर या इससे बहुत कम है।
(2) नागरिकों को बोलने, लिखने, अपना धर्म मानने और निःशस्त्र संगठन करने की स्वतंत्रता दी गई है। किसी अन्य देश में भारत से अधिक स्वतंत्रता नागरिकों को नहीं मिली है।
(3) हिंदू धर्म के कलंक स्वरूप अस्पृश्यता की सदियों से चली आने वाली प्रथा को समाप्त कर दिया गया है।
(4) देश का शासन – विधान न बहुत अधिक केंद्रीय है, न राज्यों को बहुत अधिक स्वतंत्रता दी गई है। केंद्रीय और संघ-विधान के बीच की परिस्थिति को स्वीकार किया गया है। राज्यों की स्वतंत्रता को छीना नहीं गया, किंतु राज्यों पर राष्ट्रपति के नियन्त्रण की व्यवस्था रखी गई है, ताकि वहाँ अरा- जकता और अव्यवस्था को रोका जा सके।
(5) अमेरिका की तरह राष्ट्रपति को बहुत अधिक अधिकार नहीं दिए गए। मंत्रिमंडल को इंगलैंड की भाँति शासन के लिए उत्तरदायी माना गया है। इस प्रकार अमेरिकन राष्ट्रपति व ब्रिटिश मंत्रिमंडल का समन्वय किया गया है।
(6) प्रत्येक वयस्क को मतदान का अधिकार दिया गया है। स्त्री-पुरुष, शिक्षित-अशिक्षित, अमीर-गरीब का कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है।
(7) रूस की भाँति यह संविधान साम्यवादी नहीं है। इसमें व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को स्वीकार किया गया है। किंतु उत्पत्ति के समान वितरण तथा ऐसी अर्थ – पद्धति की ओर, जिससे देश की संपत्ति कुछ हाथों में केन्द्रित न हो जाय, ध्यान देने का आदेश दिया गया है।
(8) संविधान में सरकार को कुछ निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध – निषेध, मद्य निषेध और अनिवार्य शिक्षा आदि की ओर वह ध्यान दे।
(9) हिंदी को राष्ट्र की भाषा माना गया है। 15 वर्षों में (अर्थात् 1965 तक) हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रचलित करने का वचन दिया गया है; तब तक अंग्रेजी राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती रहेगी, परंतु उसका प्रयोग क्रमशः कम होता जाएगा। (परंतु ऐसा हुआ नहीं)
(10) राज्य को ‘सैकुलर’ (धर्मनिरपेक्ष) माना गया है जिसका किसी धर्म- विशेष से संबंध नहीं है।
संविधान पर आक्षेप
साधारण दृष्टि से देखें तो यह संविधान बहुत उत्कृष्ट कोटि का है। संसार के किसी भी अन्य देश के संविधान से इसकी तुलना की जा सकती है, फिर भी इसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता। भारतवर्ष में भिन्न-भिन्न विचारकों ने इसमें भिन्न कमियाँ बताई हैं। साम्यवादी विचारक इसीलिए इससे श्रमन्तुष्ट हैं कि इसमें व्यक्तिगत सम्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है।
समस्त देश में जमींदारी उन्मूलन के कानून में भी इसीलिए संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि उसमें जमींदारो की ज़मीन का मुआवजा दिया गया है। मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन आदि की तथा लोगों को रोजगार की गारंटी नहीं दी गई। गांधीवादी विचारकों को भी इस संविधान में कुछ शिकायतें हैं। गांधीवाद की मूल आत्मा शासन और उद्योग का विकेन्द्रीकरण, मादा जीवन तथा हिमा और सदाचार आदि है। परंतु इस संविधान में न ग्राम पंचायतों पर पूरा जोर दिया गया है और न ग्राम उद्योगों को बड़े उद्योगों से बचाने का प्रयत्न किया गया है। यूरोपियन अर्थशास्त्र को देश के आर्थिक विकास का आधार माना गया है। वोट देने तथा उम्मीदवार बनाने के लिए सदाचार और योग्यता आदि का कारण हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि राज्य को किसी विशेष धर्म के साथ न बाँधा जाए।
समस्त धर्मों की एकता
कविवर रवीन्द्र ने हिंदू धर्म की एक बड़ी विशेषता यह लिखी है कि उसने अनेकता में एकता को देखा है। यही कारण है कि परस्पर अत्यंत विरोधी, नास्तिक, आस्तिक, शैव, शाक्त और वैष्णव, बौद्ध, जैन, वेदान्ती और द्वैतवादी सभी को हिंदू धर्म के विशाल क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया है। कुछ विचारकों का यह विचार है कि यदि इस्लाम तलवार और बल-प्रयोग से धर्म-प्रचार नहीं करता तो उसको भी महान् हिंदू धर्म अपने आँचल में ले लेता। आज धर्म का वह स्वरूप, जो किसी समय समस्त देश को एक सूत्र में बाँधता था, राज्य ने ले लिया है। आज राज्य ही देश के समस्त नागरिकों को एक सूत्र में बाँधता है। इसलिए राज्य का उत्तरदायित्व देश के समस्त संप्रदायों के लिए एक-सा हो जाता है और इसीलिए राज्य का असाम्प्रदायिक रहना आवश्यक है।
यदि किसी तरह देश के संविधान को हिंदू धर्म के साथ जोड़ दिया जाए, तो यह संघर्ष उत्पन्न होगा कि हिंदू धर्म का कौन-सा स्वरूप राज्य को इष्ट है। आर्यसमाजी, जैनी, हिंदू, सिक्ख तथा अन्य साम्प्रदायिक परमात्मा का स्वरूप भिन्न-भिन्न मानते हैं। किसी विशेष देवता व पूजा-पाठ की विशेष पद्धति को संविधान में स्थान देना संघर्ष का कारण बन जाएगा। आज कुछ क्षेत्रों में हिंदू- धर्म की अपेक्षा अपने-अपने संप्रदाय पर अधिक बल देने की प्रवृत्ति है और वे जनसख्या में अपने को हिंदू लिखना भी पसंद नहीं करते। काशी के एक पत्र में बौद्ध धर्म व अशोक के राज्य चिह्न को हिंदू कहकर आलोचना की गई थी। इस दृष्टि से भी राज्य का धर्म-निरपेक्ष व असाम्प्रदायिक रहना ही आवश्यक है। जहाँ तक भारतीय संस्कृति का संबंध है, वहाँ तक देश ने उसे अपनाने की दिशा में कुछ प्रयत्न किया है। देश का राज्य चिह्न अशोक का धर्म चक्र है। “सत्यमेव जयते” राज्य का आदर्श वाक्य है। देव – नागरी में लिखी गई हिंदी देश की राष्ट्रभाषा नियत हुई है। गोवध – निषेध और मद्य निषेध को भारतीय संविधान ने स्वीकार किया है। देश का नाम भारत रखा गया है। यह सब इस बात के सूचक हैं कि देश के शासक और प्रतिनिधि भारतीय संस्कृति के विरोधी नहीं है।