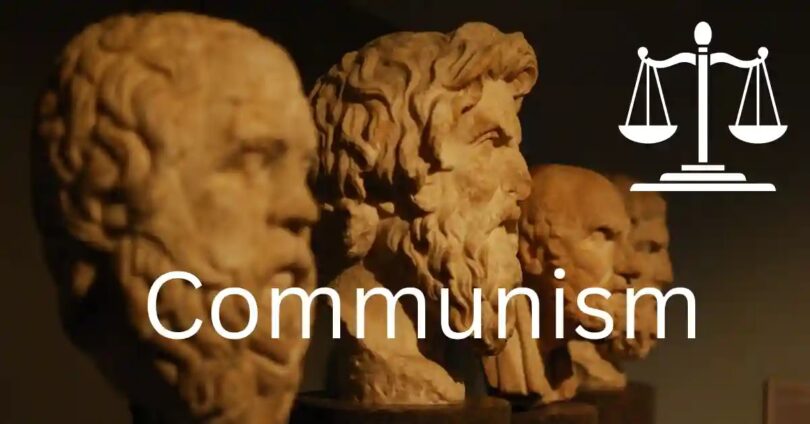दो प्रणालियाँ
आज समस्त संसार दो भागों में बँटता जा रहा है। एक वे देश हैं, जहाँ समाजवाद या साम्यवाद की विचारधारा काम करती है, और दूसरे वे देश हैं जहाँ लोकतंत्रवाद की भावना काम कर रही है। साम्यवाद और लोकतंत्र- वाद, इन दो शब्दों से वस्तुतः दोनों देशों का अंतर स्पष्ट नहीं होता। इस अंतर को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम कुछ अधिक विस्तार से दोनों देशों के अंतर को स्पष्ट करें। साम्यवादी देशों का सरल भाषा में अर्थ यह है कि वहाँ उत्पादन के साधन किसी व्यक्ति-विशेष के न हों और खासकर वे साधन, जो अनेक श्रमियों की अपेक्षा रखते हैं। इन देशों में कल-कारखाने, बैंक, जहाज, रेलगाड़ियाँ तथा जमीन आदि उत्पत्ति के सब साधनों पर सरकार का अधिकार रहता है, एक या अनेक नागरिकों का अधिकार नहीं होता। कोई व्यक्ति दूसरे मजदूर लगा करके उत्पादन कार्य नहीं कर सकता। उत्पादन के सब साधन सरकार के हाथ में रहते हैं। इस तरह देश का समस्त अर्थचक्र सरकार के हाथ में आ जाता है, इसलिए साम्यवादी देशों में अधिकाधिक शक्ति सरकारी नेताओं के हाथ में केंद्रित होती जाती है। ऐसे ही देश एकतंत्रवादी या अधिनायकवादी बनते जाते हैं।
दूसरे प्रकार के देश वे हैं, जो अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। इन देशों में प्रत्येक नागरिक आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होता है। वह कोई भी कारोबार कर सकता है, कारखाना खोल सकता है, बैंक या बीमा कंपनी आदि कायम कर सकता है और इनमें मजदूरों व कर्मचारियों को नौकर रख सकता है। इन देशों में इस प्रकार के स्वतंत्र कारोबारियों की शक्ति कम नहीं होती है। इसलिए देश के नीति-निर्धारण व मार्ग-दर्शन में इनकी काफ़ी आवाज़ होती है। ये लोग अपनी-अपनी पार्टियाँ खड़ी करके प्रतिनिधियों के चुनाव लड़ती हैं। इसलिए सब पूँजीवादी देश अपने को लोकतंत्रवादी भी कहते हैं। पहले प्रायः सब देश लोकतंत्रवादी अथवा राजतंत्रवादी थे, परंतु बीसवीं सदी में साम्यवाद ने एक के बाद एक देश पर प्रभाव जमाना शुरू किया। हम इन पंक्तियों में यह विचार करना चाहते हैं कि साम्यवाद क्या है और उसका जन्म कैसे हुआ। साम्यवाद के दृष्टिकोण पर भी हमें विचार करना है।
कार्ल मार्क्स की देन
साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स यूरोप में उत्पन्न हुआ, जहाँ का दृष्टिकोण भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। वहाँ भौतिक जीवन ही प्रधान लक्ष्य है, और इसलिए वहाँ धन या संपत्ति का बहुत अधिक महत्त्व है। कार्ल मार्क्स ने मानव जाति के समस्त इतिहास का आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया। वह इस परिणाम पर पहुँचा कि मानव समाज का अतीत और वर्तमान इतिहास वर्ग- युद्ध का इतिहास है। जिस वर्ग के हाथ में उत्पत्ति के साधन रहते हैं, उसी की प्रधानता रहती है। वह दूसरे वर्गों के परिश्रम से अनुचित लाभ उठाता है। खून-पसीना एक करने वाला परिश्रमी किसान या मजदूर अपने जीवन की साधारण आवश्यकता भी पूर्ण नहीं कर पाता, किंतु दूसरी ओर पूँजीपति गुलछर्रे उड़ाता है। उत्पत्ति पर इस वर्ग का अधिकार होने से राज्य और कानून भी दरिद्र के शोषण में धनी की सहायता करते हैं।
कार्ल मार्क्स ने संसार के इतिहास का अध्ययन करते हुए यह भी देखा कि हज़ार कोशिश करने पर भी एक ही वर्ग सदा सब के सिर पर बैठा नहीं रहता। जब पैदावार या उत्पत्ति के नए तरीके निकल आते हैं, तब उन पर अधिकार भी नए वर्गों का हो जाता है। नया दल उन्नति करता है। आर्थिक सत्ता इसके हाथ में आ जाने से उसी की जीत होती है और पुराने वर्ग की समाप्ति हो जाती है। लेकिन यह नया वर्ग भी अपने से भिन्न वर्गों के लिए शोषक बन जाता है और फिर उन वर्गों में से किसी एक के हाथों हटा दिया जाता है। इस तरह जब तक एक वर्ग दूसरे का शोषण करने वाला रहेगा, तब तक यह कशमकश चलती रहेगी। यह झगड़ा उसी समय समाप्त होगा, जबकि समाज में अनेक वर्ग न रहकर केवल एक वर्ग रह जाएगा, क्योंकि तब शोषण की गुंजायश ही न रहेगी। तब आज का सा लगातार संघर्ष न रहेगा और न रहेगी प्रतिस्पर्द्धा। किसी को किसी का दमन नहीं करना होगा। इसलिए राज्य की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। कार्ल मार्क्स का विचार था कि वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि समस्त संपत्ति को समाज या राष्ट्र की संपत्ति बना देना चाहिए। संपत्ति पर नागरिकों का निजी अधिकार नहीं होना चाहिए। उत्पादन और श्रम के साधनों पर से व्यक्ति का अधिकार हटाकर समाज का सामूहिक अधिकार स्थापित करने का नाम ही साम्यवाद है।
कार्ल मार्क्स से बहुत पहले सर थामस मोर, फोरियर, राबर्ट ओोवन, प्राउडन आदि ने भी ऐसे विचार पेश किए थे। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इन विचारों को अधिक वैज्ञानिक रूप दिया और इसके प्रचार के लिए 1834 ई. में एक निश्चित संगठन को स्थापित किया। यही साम्यवाद की दिशा में पहला व्यापक संगठन था। मार्क्स ने आवाज उठाई कि ‘संसार के मजदूरों ! एक हो जाओ और पूँजीवाद का जुआ उतार फेंको।’
साम्यवाद का व्याख्याकार लेनिन
साम्यवाद को व्यवहार में लाने वाला प्रथम व्याख्याकार लेनिन था। रूस में उसने बोल्शेविक क्रांति कर वहाँ साम्यवाद को क्रियान्वित कर दिखाया। साम्यवाद का आदर्श बहुत ऊँचा है। रूस के नेता अभी इस आदर्श पर नहीं पहुँचे। यद्यपि बहुत से उत्पत्ति-साधनों पर व्यक्ति का एकाधिकार छीनकर वहाँ उन्हें सरकारी संपत्ति बना दिया गया है, तथापि अभी तक भूमि पर कृषकों का स्वामित्व है और उन्हें सामूहिक कृषि के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कुछ विदेशियों को भी वहाँ कारोबार करने की अनुमति दी गई है।
अभी आदर्श तक नहीं
साम्यवाद का ऊँचा आदर्श यह है कि समाज में असमानता या विषमता की समाप्ति कर दी जाए, हर एक आदमी काम करे और उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे अन्न, वस्त्र आदि सब पदार्थ दिए जाएँ।
लेकिन रूस अभी इस स्थिति तक नहीं पहुँचा है। वहाँ आवश्यकता के अनुसार नहीं, कार्य और किस्म के अनुसार वेतन दिए जाते हैं। इस कारण वहाँ भी अपेक्षाकृत धनी और दरिद्र श्रेणियाँ हैं। श्री जयप्रकाश नारायण के कथनानुसार इस समय रूस में नागरिकों की आय में 1 और 80 का अंतर है। वहाँ बहुत से अधिकारियों को बहुत ऊँचे-ऊँचे वेतन मिलते हैं। उनका जीवन-स्तर भी बहुत अधिक ऊँचा है, जबकि साधारण नागरिक बहुत कष्ट में होता है। शनैः शनैः वहाँ व्यक्ति की निजी आय को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। साम्यवाद के नाम से वहाँ स्टालिन ने जिस तरह देश के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक जीवन पर एकच्छत्र निरंकुश अधिकार कर लिया था, उसका भंडाफोड़ पिछले दिनों में स्टालिन के उत्तराधिकारी रूसी नेताओं ने ही किया है। सामूहिक खेतों की सफलता के जो गीत कुछ दिनों पहले तक गाए जाते थे, उनको भी अब बंद करके धीमी आवाज में स्वीकार किया जाने लगा है कि उन प्रयत्नों में अनेक कमियाँ रह गई हैं। रूस का किसान अपने छोटे से निजी खेत में जितनी फसल पैदा कर लेता है उतनी ही सामूहिक खेत में नहीं हो पाती। मजदूरों और किसानों के दमन की कहानियाँ भी अब प्रकाश में आने लगी हैं।
संसार साम्यवाद की ओर
भले ही रूस में साम्यवाद का ऊँचा आदर्श शिथिल हो रहा हो, किंतु संसार में साम्यवाद की भावना तीव्रता से फैल रही है। पिछले महायुद्ध की परिस्थितियों ने भी साम्यवाद की भावना को बहुत बल दिया है। पदार्थों की दुर्लभता के कारण जनता के कष्ट दूर करने के लिए सरकारों ने व्यापार और उद्योग का नियंत्रण, वितरण का अधिकार तथा राशनिंग आदि अपने हाथ में ले लिए। प्रधान उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की भावना सब देशों में बढ़ी है। स्वयं इंगलैंड जैसे पूँजीवादी देश में मजदूर सरकार ने लोहा और कोयला उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया (भले ही कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने यह कदम वापिस ले लिया)। ईरान ने ब्रिटिश आयल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर लिया है तथा मिस्र ने स्वेज नहर का स्वयं भारत सरकार ने अनेक उद्योगों को हाथ में लेने का निश्चय किया है। सब जीवन बीमा कंपनियाँ सरकार की संपत्तियाँ बन गई हैं। इम्पीरियल बैंक पर भी सरकार का अधिकार हो गया है। राज्यों ने ज़मींदारी प्रथा समाप्त कर दी है। मजदूरों के लिए नए से नए नियम सब देशों में बन रहे हैं। अप्रत्यक्ष कर कम किए जा रहे हैं और प्रत्यक्ष कर बढ़ाए जा रहे हैं। इन सब साधनों से विविध देशों की सरकारें अमीर और गरीब की चौड़ी खाई को कम करने की कोशिश कर रही है।
अभी परीक्षण की स्थिति में
साम्यवाद की दिशा में इतनी प्रगति होने पर भी आज यह नहीं कहा जा सकता कि साम्यवाद संसार की समस्याओं का समाधान करने में सफल होगा। अभी साम्यवाद परीक्षण की स्थिति में से गुजर रहा है। साम्यवाद जहाँ अमीर गरीब की विषमता को दूर करता है, वहाँ वह मानव की — व्यक्ति की — निजी स्वतंत्रता का भी अपहरण करता है। वह उसे समाज का एक पुर्जा भर बना देता है। उसमें स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास की गुंजाइश नहीं रहती, समाज के लिए उसे अपनी बलि दे देनी पड़ती है। साम्यवाद में एक बड़ा दोष यह है कि उसका मूल आधार आर्थिक है किंतु जीवन में अर्थ हो तो सब कुछ नहीं है। प्रेम, धर्म, ईश्वर और देश-प्रेम या परोपकार आदि भी तो गुण हैं, जो मानव समाज का संचालन करते हैं। इनकी उपेक्षा करके मानव के केवल बाह्य अंग अर्थ पर ही आधार रखने वाला साम्यवाद कभी सर्वागीण नहीं हो सकता। वह एकांगी है, इसीलिए संसार के विचारक बहुत ध्यान से इस नए परीक्षण को देख रहे हैं। गांधीवाद में समाजवाद के गुण भी है और संसार की विषमता, प्रतिस्पर्द्धा, विद्वेष को दूर करने की क्षमता भी। इसीलिए बहुत से विचारक गांधीवाद में विश्व की समस्याओं का समाधान देखते हैं।