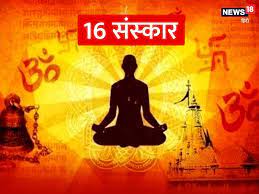गर्भाधान संस्कार –
जिस कार्य के द्वारा पुरुष स्त्री में अपना वीर्य स्थापित करता है, वह गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। शौनक ने भी लिखा है – “जिस कर्म की पूर्ति से स्त्री प्रदत्त शुक्र धारण करती है, उसे गर्भाधान कहते हैं।” पूर्व मीमांसा- कार का भी यही कहना है- गर्मः सन्धार्यते येन कर्मणा तत् गर्भाधानम्।” वैदिक काल में सन्तति एवं सगं के विकास के लिए ऋनि-मुनियों द्वारा निर्दिष्ट प्रार्थना आदि के वचनों में मातृपितृ प्रवृत्ति की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है, किंतु यहाँ यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि गर्भाधान विषयक विधानों का सर्व- प्रथम व्यवस्थित रूप हमें गृह्य-सूत्रों में प्राप्त होता है। परवर्ती धर्मशास्त्र, स्मृति एवं अन्यान्य ग्रंथों में इस संस्कार के संबंध में अधिक वैज्ञानिक सामग्री का निर्देश हुआ जहाँ गर्भाधान काल, नक्षत्र एवं स्वीकृत रात्रियों का अत्यंत विशद विवेचन है।
पुंसवन संस्कार —
प्रस्तुत संस्कार गर्म धारण हो जाने पर किया जाता है। इसका अभिप्राय उस कर्म से था जिसके अनुष्ठान से पुत्र सन्तति का जन्म हो- “पुमान् प्रसूयते येन कर्मणा तत्पुंसवनमीरितम्।” इस अवसर पर गायी जाने वाली ऋचाओं में पुत्र का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। पुत्र जन्म देने वाली माता की प्रशंसा की जाती है अथर्ववेद तथा सामवेद में इस प्रकार की प्रार्थनाएँ उपलब्ध होती हैं। गृह्यसूत्रों के अनुसार यह संस्कार गर्भ धारण करने के पश्चात दूसरे या तीसरे मास में संपन्न किया जाता है – “पुरास्यन्दत इतिमासे द्वितीय तृतीए वा।’ इस अवसर पर एक विशेष कार्य किया जाता है। वह है कि गर्भवती स्त्री के दाहिने नासिका रन्ध्र में वटवृक्ष का रस गर्भपात का निरोध तथा पुंसन्तति के जन्म के निश्चय के उद्देश्य से छोड़ा जाता था।
सीमन्तोन्नयन –
यह संस्कार गर्भकाल का तीसरा संस्कार था। इस संस्कार में गर्भवती स्त्री के केशों को उठाने का क्रिया- विधान है – “सीमन्त उन्नीयते यस्मिन् कर्मणी तत्सीमन्तोन्नयम्”। जन सामान्य के हृदय में यह आस्था थी, कि गर्भवती स्त्री को अमङ्गलकारी शक्तियाँ दुखित कर देती हैं; अतः उनके निवारण के लिए विशेष संस्कार की आवश्यकता है। आश्वलायन गृह्यसूत्र में इस विश्वास का उल्लेख मिलता है, जहाँ यह लिखा है कि राक्षसियाँ नारी के प्रथम गर्भ को खाने के लिए आती हैं इसलिए पुरुष को चाहिए कि उन अमङ्गलकारी शक्तियों के विनाश के लिए वह श्री का आवाहन करे। इन अमङ्गलकारी प्रवृत्तियों को भगाने के लिए ही इस संस्कार का विधान किया गया है। इस संस्कार का दूसरा प्रयोजन माता के लिए ऐश्वर्य तथा गर्भस्थ शिशु के लिए दीर्घायुष्य की कामना भी था। बोद्धायन गृह्यसूत्र एक अन्य प्रयोजन का भी संकेत मिलता है। वह यह है कि गर्भवती स्त्री को प्रसन्न करना भी इस संस्कार का प्रयोजन है। इस संस्कार का समय गर्भाधान के चौथे मास में बताया गया है – “चतुर्थे गर्भमासे सीमन्तोन्नयनम्”“ अथवा पुंसवनवत् प्रथमे गर्भे मासे षष्ठे अष्ठमेवा”।” सुश्रुत संहिता में लिखा है कि ‘गर्भधारण के समय से स्त्री को मैथुन, श्रम, दिवाशयन, रात्रि जागरण, सवारी पर यात्रा, भय, रेचन, रक्तस्रवण, मल-मूत्र का असामाजिक स्थगन आदि से बचाना चाहिए। इस निर्देश का स्पष्ट ही आशय शिशु की रक्षा से है।
जातकर्म संस्कार —
इस संस्कार का उद्देश्य निर्विघ्न प्रसव होने के अतिरिक्त बालक को शूरवीर, यशस्वी, वर्चस्वी बनाने का था। जातकर्म संस्कार के अवसर पर होने वाली एक क्रिया यह भी थी कि आर्य सन्तान के जन्म लेते ही उसकी जिह्वा पर स्वर्ण की सलाई से घृत एवं मधु से “ ओ3म्” लिखा जाता था, तथा कान में ‘वेदोऽसि’ कहा जाता था। अथर्ववेद के एक संपूर्ण सूक्त (1/11) में सरल एवं सुरक्षित प्रसव के लिए प्रार्थनाएँ तथा उपचार वर्णित हैं। गृह्यसूत्रों में इस संस्कार का विशद वर्णन है। गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र, एवं स्मृतियों में भी धार्मिक तत्त्वों का निर्देश है। परंतु मध्ययुगीन पद्धतियों में मातृ-गृह-प्रबन्ध, उसमें प्रवेश के विधि-विधान, प्रसूता के निकट वांछनीय व्यक्तियों की उपस्थिति तथा कतिपय शिशु मेधा जनन, आयु, बल प्राप्ति के लिए कामनाएँ तथा विधान हैं। यह संस्कार नाभि-बंधन के पूर्व ही संपन्न किया जाया था।
नामकरण संस्कार —
भारतीय हिंदू-धर्म ने प्राचीन काल से ही व्यक्तिगत नामों के महत्त्व को स्वीकार कर नामकरण की इस भाषा शास्त्रीय समस्या को धार्मिक संस्कार में परिणत कर दिया था। वृहस्पति ने ‘वीरमित्रोदय-संस्कृत- प्रकाश, में नामकरण की अनिवार्यता की ओर संकेत किया है। वह लिखता है कि नाम समस्त लौकिक व्यवहारों का हेतु है, शिद का आधायक है और भाग्योदय का हेतु है। मनुष्य अपने नाम के आधार पर ही कीर्ति प्राप्त करता है। अतः नामकरण संस्कार प्रशंसनीय है—”नामाखिलस्य व्यवहार हेतुः शुभावहं कर्म सुभाग्य हेतु नाम्नंव कोतिलभते मनुष्य ततः प्रशस्तं खलु नाम कर्म।” ऋग्वेद में भी नामन् शब्द का उल्लेख है। नामकरण की यह परंपरा प्राचीनतम है, क्योंकि वैदिक साहित्य में व्यक्ति तथा पदार्थों के नाम निर्धारित हैं। इस प्रकार ऋग्वेद, ऐतरेय, एवं शतपथ ब्राह्मण में गुह्यनाम का भी उल्लेख मिलता है। नवजात शिशु के नामकरण के विषय में प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण’ में इस प्रकार मिलता है-तस्मात्पुत्रस्य जातस्य नाम कुर्यात्” विभिन्न सूत्र-ग्रंथों के अनुसार यह संस्कार जन्म के दशवें अथवा बारहवें दिन संपन्न किया जाता है। अन्यान्य ग्रंथों में 11 व दिन, 101 व दिन तथा दूसरे वर्ष के प्रारंभ में करने का भी संकेत मिलता है।
निष्क्रमण संस्कार- नवजात शिशु को विधि-विधान के साथ प्रथम बार गृह से बाहर लाने की विधि का नाम निष्क्रमण है, तत्सम्बद्ध संस्कार निष्क्रमण संस्कार है। यह चौथे मास में होने वाला संस्कार है। बालक घर से बाहर निकलकर सूर्य का दर्शन करता था।
वैदिक साहित्य में केवल गृह्यसूत्रों में इस संस्कार का केवल इतना ही संकेत मिलता है कि — शिशु को बाहर ले जाकर “तच्चक्षुर्देवहितं2, मंत्र के पाठ के साथ सूर्य के दर्शन कराता है। परवत्तीं स्मृतियों एवं निबन्धों में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। निष्क्रमण संस्कार का समय जन्म के बारहवें दिन से चौथे मास तक विभिन्न रूपों में था। यम का कथन है कि तृतीय माह में शिशु को सूर्य दर्शन कराना चाहिए, चतुर्थ मास में चंद्रदर्शन-
ततस्तृतीए कर्त्तव्यं मासि सूर्यस्य दर्शनम्।
चतुर्थमासि कर्त्तव्यं शिशोश्चन्द्र दर्शनम् ॥
सूत्रकाल में यह संस्कार माता-पिता द्वारा शिशु को सूर्यदर्शन कराकर ही समाप्त हो जाता था किंतु परवर्त्ती साहित्य में अधिकाधिक विधि-विधानों के साथ अलंकृत बालक को कुल देवता के समक्ष लाना, वाद्य संगीत के साथ देवता की पूजा करना, आठों लोकपाल, सूर्य, चंद्र, वायुदेव एवं आकाश की स्तुति करना तथा बाद में ब्राह्मण को भोजन दानादि देने का समावेश भी हो गया है। प्रस्तुत संस्कार का उद्देश्य – वायु सेवन, सृष्टि अवलोकन का प्रथम शिक्षण है तथा दैहिक आवश्यकता की पूर्ति है।
अन्नप्राशन –
बालक की शरीर वृद्धि के साथ ही उसे पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। माँ के द्वारा मिलने वाले दुग्ध से उसकी पूर्ण तृप्ति न होने के कारण तथा मां के शरीर को स्वस्थ रखने की भावना के साथ ही इस संस्कार का उदय हुआ है। ‘सुश्रुत संहिता’ नामक आयुर्वेदीय ग्रंथ में शिशु को षष्ठ मास में पथ्य भोजन देने का विधान मिलता है। यद्यपि वैदिक साहित्य में भी कुछ इस प्रकार की श्रुतियां मिलती हैं, किंतु इस संस्कार को सूत्रकाल में ही आकर कर्मकाण्डीय आव- रण मिलता है। गृह्यसूत्रों के अनुसार यह संस्कार जन्म के छठे मास में किया जाता था। षष्ठे मास्यन्नप्राशनम्।” मनु एवं याज्ञवल्वक्य आदि स्मृतियों का भी यही मत है। किंतु लौगाक्षी का अपना विचार यह है कि शिशु की पाचन शक्ति के बढ्ने अथवा दाँतों के निकलने पर ही इस संस्कार का विधान उचित है – “बष्ठे अक्ष प्राशनमं- जातेषु दन्तेषु जातेषु वा।” किसी-किसी ग्रंथ में इस अवसर पर शिशु को माँस देने का भी विधान है, परंतु मार्कण्डेय पुराण तथा अन्यान्य ग्रंथों में भी मधु-धी तथा खीर खिलाने का विधान मिलता है।
चूड़ाकर्म संस्कार –
धर्मशास्त्र के अनुसार संस्कार्य व्यक्ति को दीवांयु, सौंदर्य तथा कल्याण की प्राप्ति करना ही इस संस्कार का प्रयोजन था आयुर्वेदीय ग्रंथों से भी उस संस्कार का समर्थन होता है। मुंडन के लिए सिर को गीला करने का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सूत्रकाल में आकर चूड़ाकर्म के विधि-विधानों का व्यवस्थित रूप मिला। गृह्यसूत्रों के अनुसार यह संस्कार जन्म के प्रथम वर्ष के अंत में अथवा तृतीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व हो जाना आवश्यक है तृतीय वर्षे चौसम्। किंतु परवर्त्ती साहित्य में इस आयु को 5 वर्ष से 7 वर्ष तक भी माना है। इस संस्कार में सिर के सभी वालों को मुड़वाकर चोटी का रखना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंग है। इस संस्कार के अवसर पर सिर को गीला कर बालों को काटा जाता है, फिर केशों को गीले आटे के पिण्ड के अथवा गोबर के पिण्ड के साथ फेंकना (गुप्त रूप में)। चौथी बात है, शिखा रखना। इस संस्कार के साथ एक वैज्ञानिक तत्त्व यह भी निहित है कि शिखा जिस स्थान पर रखी जाती है, वह कोमलतम स्थान है, केशों से उसकी रक्षा होती है। यह भावना सुदूर अतीत में रही हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ शिखा जातीय सूत्र की बोधक तो अवश्य ही है।
कर्णवेध संस्कार —
कानों का छेदा जाना सूदूर अतीत में केवल सौंदर्य के प्रसाधन के रूप में ही था; किंतु परवर्ती काल में इसकी कुछ उपयोगिता सिद्ध हो जाने के उपरान्त इसकी आवश्यकता पर बल देने के लिए धार्मिक आवरण में भी आवृत्त कर दिया गया। सुश्रुत संहिता का कथन है कि रोगादि से बचना तथा भूषण अथवा अलङ्करण के निमित्त बालक के कानों का छेदन करना चाहिए। सुश्रुत अण्डकोष की वृद्धि तथा आँत वृद्धि निरोध के लिए भी कर्णवेध संस्कार का विधान करता है। इस संस्कार का सर्वप्रथम अथर्ववेद के एक सूक्त में विधान मिलता है। वृहस्पति के अनुसार यह संस्कार जन्म के 10 वें 12 वें अथवा 16 वें दिन किया जाता था। गर्गऋषि छठें, सातवें, आठवें अथवा बारहवें मास में इस संस्कार का निधान करता है। श्रीपति बालक के दाँतों के निकलने से पूर्व ही इसका विधान करते हैं। कात्या- यन तीसरे या पांचवें वर्ष के निर्देश के साथ शुभ दिन में पूर्वाभिमुखासीन बालक के क्रमशः दायें, बायें कान को छेदन का निर्देश करता है।
विद्यारंभ संस्कार —
बालक के शिक्षा ग्रहण के योग्य हो जाने पर विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। इसी को दूसरे शब्दों में अक्षरारंभ कहा जाता था। सर्वप्रथम स्मृतियों में ही इस संस्कार का उल्लेख मिलता है। इसका आरंभ चौल एवं मुंडन संस्कार के साथ ही किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी इसी विचारधारा की पुष्टि होती है। बालक स्नानादि से पवित्र होकर गणेश, सरस्वती, गृह देवता, लक्ष्मीनारायण आदि की स्तुति के साथ गुरु के सम्मुख बैठकर अक्षरों को तीन बार पढ़ता था।
उपनयन संस्कार –
गुरु के समीप ले आना — इस अर्थ का यह बोधक शब्द एक सुदीर्घ ऐतिहासिक परंपरा को आत्मसात् किए हुए हैं। अथर्ववेद में इस शब्द का प्रयोग ब्रह्मचारी को ग्रहण करने के अर्थ में किया गया है। किंतु इस शब्द का वास्तविक अर्थ आचार्य द्वारा आगत शिष्य को दीक्षादान है। ब्राह्मणकाल में भी यही मान्यता बनी रही और सूत्रकाल में भी यही स्थिति रही। किंतु परवर्तीकाल में गायत्रीमंत्र द्वारा द्वितीय जन्म के अर्थ में उपनयन शब्द रूढ़ हो गया है। मनु और याज्ञवल्क्य, उपनयन संस्कार से बालक का द्वितीय जन्म मानते हैं। किंतु आगे की परंपरा छात्र का आचार्य के निकट लाने के अर्थ में ही इस संस्कार की मान्यता की इतिश्री समझने लगी। आज इस संस्कार से केवल यज्ञोपवीत संस्कार ही माना जाता है | मातृ-पितृ-आचार्य ऋण को सदैव स्मरण कराने के लिए आचार्य-संस्कार को कराता है। ऐसी भी मान्यता थी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पुत्रों को 16, 22, 24 वर्ष तक यज्ञोपवीत (उपनयन) संस्कार अवश्य ही कर लेना चाहिए। अन्यथा वह व्रात्य (पतित) इस संज्ञा का अधिकारी होता है। वैसे इस संस्कार का ब्राह्मण पुत्र के लिए आठवें क्षत्रिय पुत्र के लिए ग्यारहवें, वैश्य पुत्र के लिए बारहवें वर्ष का भी विधान है।’
वेदारंभ संस्कार –
प्राचीनकाल में उपनयन संस्कार के साथ ही वेदों का अध्यननाध्यापन प्रारंभ हो जाता था, किंतु परवर्त्तीकाल में संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही तो उपनयन केवल दैहिक संस्कार मात्र रह गया। अतः इस संस्कार के पूर्व ही ब्रह्मचारी लोकभाषा का अध्ययन आरंभ कर देता था। इसलिए संस्कृत भाषा तथा वैदिक साहित्य के अध्ययनाध्यापन के आरंभ करने के लिए एक अन्य संस्कार का उद्भव आवश्यक माना गया। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वेदारंभ संस्कार का उदय हुआ है। इस संस्कार का सर्वप्रथम उल्लेख व्यासस्मृति में मिलता है। इस वेदारंभ-संस्कार में ब्रह्मचारी को आचार्य अनेक सदुपदेश देकर उपनयन संस्कार के बाद एक वर्ष के भीतर ही गायत्री मंत्र की दीक्षा के साथ अपना अध्यय- नाध्यापन प्रारंभ कर देता था।
केशांत अथवा गोदान —
इस संस्कार में ब्रह्मचारी की श्मश्रुओं का सर्वप्रथम क्षौर किया जाता था। इसे गोदान – संस्कार भी कहते हैं क्योंकि इस अवसर पर आचार्य को गौ का दान किया जाता था। यह संस्कार ब्रह्मचारी की सोलह वर्ष की अवस्था में संपन्न किया जाता था। इस संस्कार की मान्यता के संबंध में अनेक आचार्यों में विवाद है। कोई कोई आचार्य चूड़ाकरण के साथ भी इस संस्कार को सम्बद्ध करते हैं।
समावर्तन संस्कार –
अथवा स्नान-वीर मित्रोदय में समावर्त्तन का अर्थ है- तसमावर्त्तनं नाम वेदाध्ययनान्तरम् गुरुकुलाद् स्वगृहागमनम्, अर्थात् वेदाध्ययन के उपरान्त गुरुकुल से अपने घर को प्रत्यावर्त्तन का नाम समावर्त्तन है। इस संस्कार का दूसरा नाम ‘स्नान-संस्कार’ भी है क्योंकि समावर्त्तन-संस्कार के करने से पूर्व ब्रह्मचारी को शीतल पवित्र जल से स्नान कराने का भी विधान था। दूसरे शब्दों में इस संस्कार को ‘दीक्षान्त-संस्कार’ भी कहा जाता था। प्राचीन मान्यता के अनुरूप ब्रह्मचर्याश्रम एक दीर्घसत्र था। गृह्यसूत्र में लिखा है कि- “ दीर्घसत्रं वा एष उपैति यो ब्रह्मचर्यमुपैति” इस दीर्घसत्र के उपरान्त स्नान एक अनिवार्य विधान था, क्योंकि संस्कृत का अध्ययन सागर सन्तरण के समान माना जाता था और वह स्नातक भी विद्या- सागर का पारङ्गत माना जाता था। “इस प्रकार विद्यार्थी जीवन के अंत में किया जाने वाला प्रस्तुत सांस्कृतिक स्नान भी विद्यार्थी के द्वारा विद्या-सागर को पार करने का प्रतीक था।”
विवाह-संस्कार –
समस्त संस्कारों में विवाह का महत्त्वपूर्ण स्थान है। अधिकांश गृह्यसूत्रों का आरंभ विवाह-संस्कार से होता है। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में भी वैवाहिक विधि-विधानों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। उपनिषदों के युग में भी आश्रम चतुष्टय का सिद्धान्त पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुका था, जिनमें गृहस्थाश्रम की महत्ता सर्वाधिक स्वीकार की जा चुकी थी। गृह्य-सूत्रों, धर्म-सूत्रों एवं स्मृतियों में भी परवर्त्तीकाल में प्रस्तुत संस्कार का पूर्ण परिचय मिलता है। स्वामी दयानन्द ने “गृहाश्रम-संस्कार” का भी विधान किया है; उनके अनुसार ऐहिक और पारलौकिक सुख प्राप्ति के लिए विवाह करके अपने सामर्थ्य अनुसार परोपकार करना और नियत काल में यथाविधि ईश्वरोपासना और गृह कृत्य करना और सत्य धर्म में ही अपना तन, मन धन लगाना तथा धर्मानुसार सन्तानों की उत्पत्ति करना, इसी का नाम गृहाश्रम संस्कार है।” किंतु मेरे विचार से विवाह एवं गृहाश्रम संस्कार को एक ही मान लेना उचित है।
स्वामी दयानन्द ने विद्यारंभ एवं केशांत को मान्यता न देकर वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम के प्रवेश करने पर संस्कार का विधान किया है, अतः हम इन दोनों ही संस्कारों का संक्षिप्त परिचय यहाँ देना अनुपयुक्त नहीं समझते हैं।
वानप्रस्थाश्रम प्रवेश संस्कार –
प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार यहाँ चार आश्रमों की पूर्ण प्रतिष्ठा थी— ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। वान- प्रस्थाश्रम का आशय यह है कि मानव अपनी गृहस्थाश्रम के लिए निर्धारित आयु को पूर्ण करके अर्थात् पचास वर्ष की आयु होने पर अथवा प्रपौत्र के हो जाने पर गृहस्था- श्रम का त्याग कर अरण्य निवास करे अथवा भावी जीवन के निर्माण के लिए संयम- पूर्वक साधना करे। यही नहीं, प्राचीन मान्यता के अनुरूप मुक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वरार्चन भी करे। जैसा कि लिखा भी है—
“ब्रह्मचर्याश्रम समाप्य गृहीभवेत् गृही भूत्वा वनी भवेत् बनी भूत्वा प्रवृजेत्” इसी श्लोक में संन्यासाश्रम का भी उल्लेख है, जिसमें वानप्रस्थाश्रम के उपरान्त संन्यास लेने का विधान है। संन्यासाश्रम में दीक्षित होने पर मानव मोह आदि का परि- लाग कर पक्षपात रहित विरक्त हो समस्त जन-जीवन के परोपकारार्थं विचरण करे। अन्त्येष्टि संस्कार — हिंदू के जीवन का अन्तिम संस्कार अन्त्येष्टि है, जिसके साथ वह अपने ऐहिक जीवन का अन्तिम अध्याय समाप्त करता है। भारतीय पुन- जन्मवाद में आस्था रखकर एक भारतीय इस संस्कार को करता है क्योंकि परलोक में सुख एवं कल्याण की प्राप्ति के लिए यह संस्कार आवश्यक माना गया है। बोधायन पितृमेध सूत्र में कहा गया है कि – “जात संस्कारेणेमं लोकमभिजयतिमृत्संस्कारेणामुं लोकम्” अर्थात् जन्मोत्तर संस्कारों के द्वारा व्यक्ति इस लोक को जीतता है और मरणोत्तर संस्कारों द्वारा उस लोक को। अन्त्येष्टि-क्रियाओं में व्यवहृत ऋचाएँ ॠग्वेद तथा अथर्ववेद में उपलब्ध होती हैं। इसका विधान कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरी- यारण्यक के षष्ठ अध्याय में प्राप्त होता है। परवर्ती कतिपय गृह्य सूत्रों में अन्त्येष्टि संस्कार से सम्बद्ध विधि-विधानों का बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। इस संस्कार के करने से कुछ विशेष लाभ भी है। इस संस्कार के करने से एक तो संक्रामक रोग एवं कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात यह भी है कि इस संस्कार से मृतक तथा जीवित के प्रति गृहस्थ के कर्त्तव्यों में सामञ्जस्य स्थापित होता है। यह पारिवारिक और सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान का एक विस्मयजनक समन्वय तथा जीवित सम्बन्धियों को सांत्वना प्रदान करना भी इसका एक लक्ष्य था।
आज बच्चों के निर्माण के लिए न जाने कितने साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, न जाने कितनी संस्थाएँ केवल बच्चों के निर्माण के लिए कार्य कर रही हैं। प्राचीन भारत में इन सभी का अभाव था, किंतु मानव आज से अधिक सभ्य एवं शिष्ट तथा बल संपन्न था। इसका एकमात्र कारण संस्कारों का क्रियान्वयीकरण ही था। संस्कार व्यवहार में मानव-जीवन के निर्माण व विकास की क्रमबद्ध योजना है। ए संस्कार जीवन के परिष्कार एवं व्यक्तित्व के विकास में भी अपना योगदान करते हैं। समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सफल पथ प्रस्तुत करते हैं। संस्कार शिक्षा दान का एक वैज्ञानिक प्रयोग है, महाभारत के प्रमुख पात्र अभिमन्यु ने माँ के पेट में ही चक्रव्यूह की रचना तथा उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वैवाहिक नियम समाज में पारिवारिक जीवन को सुखद बनाने के साथ ही सामाजिक कुरीतियों के निवारण में योग देते हैं। वानप्रस्थ एवं संन्यासाश्रम राष्ट्र के सर्वाङ्गपूर्ण अभ्युदय एवं शिक्षा के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष यह है कि मानव निर्माण एवं सर्वाङ्गीण विकास में संस्कार महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। निश्चय ही ए संस्कार मनुष्य को वास्तविक अर्थों में मानव बनाने का कार्य करते हैं।