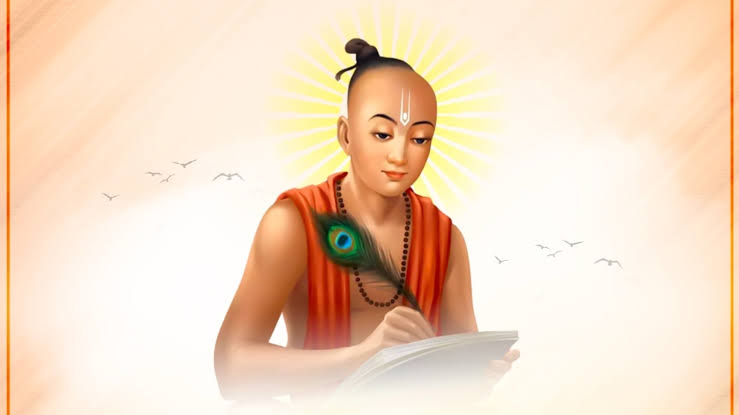(1) प्रस्तावना -तुलसीदास जी के जन्म के समय की परिस्थिति
(2) तुलसीदास का जन्म और वाल्य काल
(3) शिक्षा-दीक्षा और विवाह
(4) संन्यास और भ्रमण
(5) कव्य-रचना
(6) मृत्यु
(7) तुलसीदास जी की सर्वप्रियता –
(क) कविता,
(ख) भक्ति,
(ग) समाज-सुधार
(8) उपसंहार – हिंदू जाति पर तुलसीदासजी का ऋण
भारतवर्ष में मुसलमानों का आधिपत्य पूर्णतः स्थापित हो जाने पर हिंदुओं के हृदय में गौरव और आत्माभिमान के भाव नहीं रह गए। कट्टर और धार्मिक असहिष्णु मुसलमान हिंदुओं के धर्म पर आक्षेप करते थे, उनपर अत्याचार करते थे और पराधीन हिंदू दीन बने हुए सब कुछ सह लेते थे। वस्तुतः हिंदुओं का जीवन निराशामय था। उनके लिए उसमें कोई माधुर्य नहीं रह गया था। संसार में उनके आँसू पोंछने वाला कोई नहीं था। गज की एक ही पुकार पर पैदल दौड़ आनेवाला परमेश्वर अब उनकी सहस्रों पुकारों को नहीं सुनता था। हिंदुओं में ऐसी दुर्दशा के समय भारतवर्ष में गोस्वामी तुलसीदास जी का आविर्भाव हुआ जिन्होंने हिंदुओं के भग्न होते हुए हृदय को संभाला और उन्हें दुष्ट दलनकारी भगवान् राम की झाँकी कराकर उनके जीवन को सरस बना दिया। साथ ही अपनी अलौकिक प्रतिभा से हिंदी साहित्य को प्रौढ़ता की चरम सीमा पर पहुँचा दिया, उसके कलेवर को देदीप्यमान रत्नों से अलंकृत किया।
गोस्वामी तुलसीदासजी ने संवत् 1554 में श्रावण शुक्त 7 को बाँदा जिले के अन्तर्गत राजापुर नामक गाँव में जन्म धारण किया। इनके जन्म के संबंध में यह दोहा प्रचलित है।
“पन्द्रह सौ चौअन विषै कालिन्दी के तीर।
श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर॥”
इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी माना जाता है। ये सरयूपारी ब्राह्मण थे। इनका जन्म का नाम रामवोला था। ये जब उत्पन्न हुए तब पाँच वर्ष के बालक के समान थे और इनके मुँह में 32 दाँत भी थे। जन्म के समय ये रोए नहीं बल्कि इनके मुख से ‘राम’ शब्द निकला। पिता ने बालक को राक्षस समझा और उसकी उपेक्षा की। पर माता ने उसे अपनी मुनिया नामक दासी को पालन पोषणार्थ दे दिया। जन्म के पाँच दिन बाद माता का स्वर्गवास हो गया। पाँच वर्ष पीछे मुनिया भी मर गई। तब बालक के पिता के पास बालक ले जाने का संवाद भेजा गया पर उन्होंने उसे लेना स्वीकार न किया। इस प्रकार पिता परित्यक्त बालक तुलसीदास लोगों के द्वार-द्वार भटकता फिरा।
दो वर्ष तक बालक तुलसीदास की यही दशा रही। इसके अनंतर बाबा नरहरिदास ने उसे अपने पास रख लिया और शिक्षा दी। ये ही गोस्वामीजी को रामचंद्रजी की कथा सुनाया करते थे। इन्हीं के साथ वे काशी गए और इनके गुरु स्वामी रामानंदजी के निवास- स्थान पंचगंगा घाट पर रहने लगे। वहाँ पर पास ही एक विद्वान महात्मा शेषसनातन जी रहते थे जिन्होंने तुलसीदासजी को वेद, पुराण, दर्शन – शास्त्र, इतिहास आदि पढ़ाया। कुछ समय पश्चात् नरिहरिदास वहाँ से चित्रकूट चले गए और तुलसीदासजी वहाँ विद्या पढ़ते रहे। शेषसनातनजी की मृत्यु के बाद 15 वर्ष तक अध्ययन कर के गोस्वामीजी अपनी जन्म भूमि राजापुर को लौट आए। यहाँ इनके परिवार में कोई नहीं रहा था। गाँव के लोगों के आग्रह से तुलसीदासजी ने यहीं रहना निश्चय किया। ये रामचंद्रजी की कथा में मग्न रहा करते थे और लोगों को उसका रसास्वाद कराया करते थे। एक बार यमुना पार करके एक ग्राम के रहनेवाले भारद्वाज गोत्र के एक ब्राह्मण राजापुर स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदास जी की कथा सुनी। गोस्वामीजी की योग्यता और सौंदर्य पर मुग्ध होकर उन्होंने अपनी लड़की इन्हें ब्याह दी। जनश्रुति इस ब्राह्मण को दीनबन्धु और लड़की को रत्नावली के नाम से जानती है।
तुलसीदासजी अपनी पत्नी में इतने अनुरक्त रहते थे कि एक बार इनकी अनुपस्थिति में उसके नैहर चले जाने पर ये उसका वियोग न सह सके और आधी रात में ससुराल जाकर उससे मिले। स्त्री इनके इस कार्य से अत्यंत क्षुब्ध होकर इन्हें फटकारती हुई बोली-
“अस्थि चर्म-मय देह मम तामें ऐसी प्रीति।
तैसी जो श्रीराम महँ होति न तौ भव-भीति॥”
यह बात तुलसीदास जी को ऐसी लगी कि ये तुरन्त काशी आकर संन्यासी हो गए। वहाँ से अयोध्या जाकर चार महीने रहे। फिर तीर्थ-यात्रा के लिए निकले और जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका होते हुए बद्रिकाश्रम गए। यहाँ से ये कैलाश और मानसरोवर तक चले गए। इस यात्रा में लगभग 16 वर्ष लग गए। अन्त में चित्रकूट जाकर ये बहुत दिनों तक रहे।
संवत् 1616 में चित्रकूट में सूरदासजी इनसे मिलने आए और यहीं इन्होंने ‘गीतावली’ तथा ‘कृष्ण गीतावली’ की रचना की। इसके पीछे अयोध्या जाकर संवत् 1631 में इन्होंने ‘रामचरितमानस’ का प्रारम्भ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। रामायण का कुछ अंश विशेषतः किष्किन्धाकाण्ड काशी में लिखा गया। इन तीनों ग्रन्थों के अतिरिक्त नौ ग्रन्थ गोस्वामीजी के और प्रसिद्ध हैं। वे हैं – दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछू, पार्वती मंगल, जानकी- मंगल, बरवै- रामायण और वैराग्य संदीपिनी।
संवत् 1680 में श्रावण कृष्णा 3 को गोस्वामीजी का शरीरान्त हुआ, जैसा कि इस दोहे से प्रकट है-
“संवत् सोरहसो असी, असी गङ्ग के तीर।
श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तज्यो शरीर॥”
गोस्वामीजी की सर्व-प्रियता के कारण इनकी कविता, भक्ति और समाज-सुधार हैं। कविता की दृष्टि से हिंदी साहित्य में इनका -स्थान सर्वोच्च है। इनकी कविता में प्रायः हृदय के सभी भाव चित्रित हुए हैं। मानव हृदय पर जैसा विस्तृत अधिकार इन महानुभाव का देखा जाता है वैसा हिंदी के किसी भी अन्य कवि का नहीं। रामचंद्रजी की कथा के मार्मिक स्थलों के हृदयग्राही वर्णनों से इनकी भावुकता का परिचय मिलता है। बाहरी दृश्यों के चित्रण में भी इन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। इस दृष्टि से भी हिंदी के अन्य कवियों से ये बहुत ऊँचे उठ जाते हैं। भिन्न-भिन्न व्यापारों में संलग्न मनुष्यों की मुद्राओं और प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बड़े सजीव उतरे हैं। इन्होंने काव्य की सभी प्रचलित शैलियों में अपनी रचनाएँ की हैं और उनमें पूर्ण सफलता प्राप्त की है। कविता के बाहरी अङ्ग अर्थात् उक्ति का अनूठापन, अलंकार और भाषा का जैसा सुंदर रूप इनकी कविता में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। काव्य-भाषा ब्रज और अवधी दोनों पर इनका समान अधिकार देखा जाता है। इनकी-सी प्रौढ़, सुव्यवस्थित और शुद्ध भाषा बहुत थोड़े कवि लिख सके हैं। हिंदी में ऐसा कोई कवि नहीं हुआ जिसका भिन्न-भिन्न भाषाओं पर गोस्वामीजी के समान अधिकार रहा हो। सबसे बड़ी विशेषता गोस्वामीजी का वर्णनीय विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामचंद्रजी को अपने काव्य का विषय बनाकर इन्होंने अपनी वाणी से सुधाधारा प्रवाहित की और उसमें हिंदू-जाति को स्नान कराके उसका दुःख दूर किया।
कविता से गोस्वामीजी को जितनी लोकप्रियता मिली है उससे किसी अंश में भी कम भक्ति से नहीं प्राप्त हुई है। जो मनुष्य कविता के गुण-दोष विवेचन करना नहीं जानता वह भी इनकी भक्ति-भावना पर मुग्ध है। इन्होंने अपनी राम-भक्ति में हिंदू-धर्म के सव पक्षों का सामञ्जस्य करके शैवों, वैष्णवों, शाक्तों और कर्मठों के झगड़ों का अन्त किया और धर्म को अधिक चलता रूप प्रदान किया। ‘विनय पत्रिका’ में इन्होंने गणेशजी, शिवजी, हनुमानजी, सूर्य भगवान्, देवीजी, भैरवजी आदि देवी-देवताओं की स्तुति करके अपनी धार्मिक उदारता का परिचय दिया है। ‘रामचरित मानस’ में तो यहाँ तक कह दिया गया है :-
“शिव-द्रोही मम दास कहावै। सो नर मोहि सपनेहुँ न भावै॥”
गोस्वामीजी की भक्ति में उदारता के साथ-साथ अनन्यता भी पाई जाती है। ‘दोहावली’ की ‘चातक- चौतीसी’ और ‘विनय-पत्रिका’ के कतिपय पद इसके परिचायक हैं। इनकी भक्ति मर्यादा की सर्वदा रक्षा करती है। मर्यादा उसका प्रधान अंग है। काकभुशुण्डि और शिवजी के शाप का मामला इस तथ्य का ज्वलन्त उदाहरण है।
वास्तव में गोस्वामीजी की सबसे अधिक सर्व-प्रियता का कारण है इनका समाज-सुधार। इनसे पहले हिंदू-समाज की बड़ी हीन- दशा थी। हिंदू वर्णाश्रम धर्म को छोड़ बैठे थे। वेद-शास्त्रों की निंदा होती थी। विद्वानों, सन्तों और पूज्य व्यक्तियों का निरादर होता था। नए-नए मत बढ़ रहे थे। उधर मुसलमानों के अत्याचार भी हो रहे थे। ऐसा ज्ञात होता था कि हिंदू समाज नष्ट-भ्रष्ट हो जाएगा। गोस्वामीजी ने ऐसी भयङ्कर परिस्थिति में उत्पन्न होकर हिंदू समाज को बचाया, उसे नया जीवन प्रदान किया। वर्णाश्रम धर्म की फिर से प्रतिष्ठा हुई। वेद-शास्त्रों का महत्त्व जन साधारण को ज्ञात हुआ। धर्म के वास्तविक रूप से विमुख करने वाले मतों का उन्मूलन किया गया। दुष्ट दलनकारो भगवान् राम का मङ्गलमय रूप दिखाकर जनता में आशा और शक्ति का सञ्चार किया गया। ‘रामचरित मानस’ सरीखा अद्वितीय ग्रन्थ रचकर गोस्वामीजी ने हिंदू जाति का कल्याण कर दिया। इससे समाज का कितना हित हुआ है, यह बतलाना शब्द की शक्ति से परे है। आज उसी पवित्र ग्रन्थ का यह प्रभाव है कि प्रत्येक हिंदू धर्म पर श्रद्धा रखता है, सन्मार्ग में पैर रखता है, विपत्ति में धैर्य रखता है, पापों से घृणा करता है और राम-नाम को नहीं भूलता।
अन्त में यही कहना है कि हिंदू-समाज पर गोस्वामीजी का अपार ऋण है। इन्होंने हिंदू-समाज के लिए जो कुछ किया है उसे सहस्त्रों उपदेशक भी नहीं कर सकते थे। हिंदी, हिंदू-धर्म और हिंदुओं का कल्याण करने वाले गोस्वामी धन्य हैं और धन्य है वह जननी जिसके गर्भ से ऐसी महान आत्मा की अभिभूति हुई।
“भारी भवसागर उतारतो कवन पार,
जो पै यह रामायन तुलसी न गावतो।”