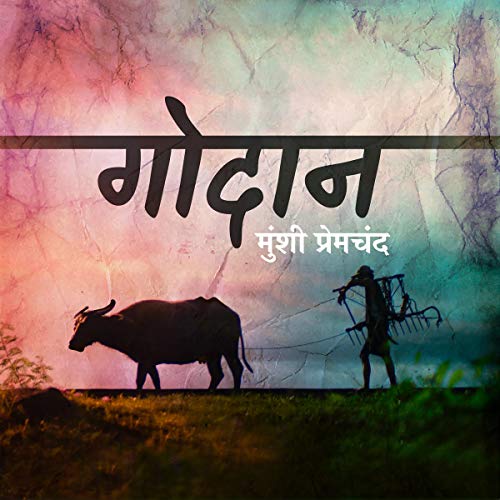प्रेमचंद जी की सब रचनाओं को जब हम क्रम से पढ़ते हैं तो हमें उनका जीवन तथा साहित्य सतत् परिवर्तनशील दिखलाई देता है। उसका आशावादी दृष्टिकोण धीरे-धीरे ठेस खाकर यथार्थवाद की ओर बढ़ा है और जीवन के अंत तक पहुँचकर वह स्पष्ट रूप से यथार्थवादी हो गया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण लेकर भी भारतीय आदर्श को भुलाना मुंशी प्रेमचंद नहीं सीखे थे। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास ‘गोदान’ है, जिसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण लेकर आपने पात्रों की परिस्थितियों में और परिस्थितियों को पात्रों के हाथों में खूब कलाबाजी खिलवाई है। ‘गोदान’ लिखते समय लेखक उपन्यास लिखने बैठा है; आशावादी स्वप्नों के फूल खिलाने नहीं। राम-राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य उस समय उसके सम्मुख नहीं है। वह यथार्थ जीवन को चित्रित करता है। समस्याएँ आती भी हैं तो बहुत स्वाभाविक रूप में आती हैं, लेखक द्वारा आदर्श-पूर्ति के लिए निर्मित नहीं की जातीं। जीवन के सजीव चित्र लेखक ने उपस्थित करने का प्रयत्न किया है, निर्बल और कठपुतली के समान नहीं। गोदान का ‘होरी’ ‘रंगभूमि’ के सूरदास की भाँति जीवन में सफल न होकर ही भारतीय ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी दृष्टिकोण को निखरे रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। ‘गोदान’ में कठोर सत्य पर आशावादी चादर डालकर सुख-स्वप्नों की कल्पना करने का प्रयास प्रेमचंद ने नहीं किया। ‘गोदान’ में प्रेमचंद जी ग्रामीण जीवन के साथ-साथ नागरिक जीवन की भी उपेक्षा करके नहीं चले हैं ‘होरी’ के संघर्षमय जीवन के शहरी पात्रों का आमोद-प्रमोद, थियेटर और शिकार का भी सजीव चित्रण किया गया है, जिससे पाठक यथार्थवाद के जाल में फँसकर ऊब नहीं उठता और उसका मनोरंजन प्राप्त करने वाली आकांक्षाओं को ठेस भी नहीं लगती। एक ओर भारतीय समाज की दैनिक दशा लेखक ने ग्रामीणता के चित्रण द्वारा प्रस्तुत की है और नागरिक अहंकार के साथ-साथ, सांस्कृतिक विकास जिसे कहते हैं, समाज सेवा, शिक्षा प्रचार, नाच रंग और इसी प्रकार की प्रसन्नता वर्धक बातों को भी जुटाया है। इस प्रकार दो विपक्षी चरित्रों को लेकर लेखक ने समन्वय के साथ कथा और पात्रों के चरित्र चित्रण का उत्कर्ष दिखलाया है। दोनों चरित्रों के आमने-सामने आ जाने पर दोनों के गुण और दोषों का इतना निखरा चित्र सामने उपस्थित हो जाता है जितना पृथक्-पृथक् रहने पर वह संभव नहीं। वास्तव में यह उपन्यास दो पृथक्-पृथक् कहानियों को लेकर चलता है और वह दोनों कथाएँ एक-दूसरी से स्थान-स्थान पर कुछ मिल जाने पर भी पृथक् ही रहती हैं। दोनों कथाओं को उपन्यासकार ने आद्योपांत खूब निभाया है। कुछ प्रेमचंद के आलोचक इन दो कथाओं के होने को उपन्यास का दोष भी मानते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं मानते बल्कि और उल्टी लेखक की कला-कुशलता का आभास हमें इसमें मिलता है। इस प्रकार ‘गोदान’ की कथावस्तु बिखरी हुई होने पर अपनी विशेषता रखती है और कहीं उसका सौंदर्य नष्ट नहीं होने पाता। ‘गोदान’ के चित्रण में लेखक ने निष्पक्ष भाव से काम लिया है। भविष्य की संभावनाओं के लिए वर्तमान का गला नहीं घोंटा गया। अपने काल से समाज का सजीव चित्रण इस उपन्यास में लेखक ने प्रस्तुत किया है। ‘गमन’ का लेखक पात्रों को जीवन-पथ पर छोड़कर स्वयं सृष्टा बन जाता है ‘होरी’ अपनी परिस्थिति और स्वभाव के अनुसार स्वयं अपना पथ निर्माण करता है। परिस्थितियाँ उसे मिलती हैं और वह उनसे संघर्ष करता हुआ जीवन के पथ पर अग्रसर होता है। नियति के हाथों में खेलता है और अनथक परिश्रम करता हुआ जीवन के अंत तक चला जाता है। ग्रामीण जीवन का खिलाड़ी ‘होरी’ परिस्थितियों के थपेड़े सहने में असमर्थ है; परंतु नगर के रायसाहब, मिर्जा और मेहता को लेखक ने इतना निर्बल नहीं बनाया। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली है और उन पर परिस्थितियों का यदि आघात होता है तो वह परिस्थितियों से टक्कर लेने में भी समर्थ हैं। कहानी के विचार से ग्रामीण कहानी अधिक क्रमिक और सुगठित है। उसका विकास भी नगर की कहानी से अधिक सुंदर और क्रमबद्ध है। नागरिकों को कबड्डी खिलाना प्रेमचंद जी भी अपनी सूझ है, जिसका शहर के व्यवहारिक जीवन से कम संबंध है। ‘होरी’ के रूप में उपन्यासकार ने भारतीय किसान वर्ग का वह चित्रण किया है जिसमें किसान के अंदर पाए जाने वाले सभी गुण और दुर्गुण वर्तमान हैं। समाज की मर्यादा को मानता हुआ वह ईश्वर से डरता है। गाँव के मुखियाओं का उत्पीड़न वह अपनी परिस्थितियों को देखक सहन करता है। धर्म के ठेके दारों का अत्याचार सहन करता हुआ भी सुनिया’ को घर में आश्रय देता है, सम्मिलित परिवार में छोटे भाई ‘होरी’ और ‘शोभा’ को पुत्रवत पालता है, अलग होने पर भी उनका मान-अपमान होरी का अपना मान-अपमान है। भाई द्वारा अपनी गाय को जहर दिए जाने पर भी वह पुलिस द्वारा अपने भाई के घर की तलाशी लिवाने को सहन नहीं कर सकता। भाई के लापता हो जाने पर वह भाभी की सहायता करता है। यह सब चरित्र के गुण होने पर भी वह महाजन के सामने झूठी कसमें खा सकता है, मन को गीला करके भारी बना देना और रुई में बिनौले मिला देना भी वह अनुचित नहीं समझता। अपने भाई के दो-चार रुपये भी वह दबा सकता है, यदि बाहरवालों की दृष्टि उस पर न पड़े। वह समाज से भय मानता है, अपनी आत्मा से नहीं। यह हैं होरी के जीवन के दोनों पक्ष, जिनके अंतर्गत जीवन भर संघर्ष करता हुआ वह चलता चला जाता है। खानदान के मान के लिए वह महाजन का शिकार बना हुआ है और इस खोखले खानदान के मान में ही वह अपना सर्वस्व गवाकर एक दिन कोरा मजदूर मात्र रह जाता है। मजदूरी करते हुए उसे लू लग जाती है और वह बीमार पड़ जाता है। दशा बिलकुल बिगड़ जाने पर ‘होरी’ भाभी से गोदान करने को कहता है। धनिया सन बेचकर जो बीस आने पैसे लाई थी पति उन्हें के मुर्दा हाथों में रखकर कहती है, “महाराज ! घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। यहीं पैसे हैं, यही इनका गोदान है।” और स्वयं चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है। ‘गोदान’ का यही अंत है। होरी का मृतक शरीर पड़ा है, धनिया मूर्च्छित पड़ी है और सूदखोर दातादीन अब भी हाथ पसारे पुरोहित बना सामने खड़ा है। ‘गोदान’ एक किसान की नीच साहूकार द्वारा शोषण की कहानी है। इस उपन्यास में सूदखोरों के भी वर्ग बनाकर उपन्यासकार ने रख दिए हैं। झींगुर सिंह, दातादीन और लाला पटेश्वरी यह सभी किसानों का रक्त चूसने के लिए जोंक के समान हैं। दुलारी साहूकारिन भी किसी से कुछ कम नहीं है। साहूकारों के अत्याचार के साथ-साथ जमींदार और सरकारी अफ़सरों की सख्ती का भी चित्रण ‘गोदान’ में किया गया है। बिरादरी के अत्याचारों का वर्णन प्रेमचंद जी ने किया है और दिखलाया है किस-किस प्रकार शादी, ब्याह, मुंडन, कर्ण छेदन, जन्म-मरण सब पर बिरादरी का ही अधिकार है। बिरादरी द्वारा निर्मित कृत्रिम नियमों का उल्लंघन करने वालों को तो मानो वह कच्चा ही चबाने को तत्पर रहती है। उसके कृत्रिम नियम पालन करके आप चाहे जो कुछ भी पाप कर्म क्यों न करते रहें बिरादरी आपके मार्ग में नहीं आती। ‘दातादीन’ एक चमारिन से फँसा हुआ होकर भी संस्कार कराता है और बिरादरी में मान का पात्र भी है। होरी पर बिरादरी आपत्तियों का पहाड़ ढहा देती है। ग्रामीण समाज शहरी समाज से अधिक कड़ा है और अपने नियमों का उल्लंघन कदाचित् सहन नहीं कर सकता। ‘गोदान’ में गोवर, सिलिया, दातादीन इत्यादि द्वारा सामाजिक बंधनों के विरुद्ध विद्रोह भी प्रेमचंद ने प्रकट किया है।
‘गोदान’ में भारतीय संस्कृति का लेखक ने विशेष ध्यान रखा है और यह विशेषता उनके प्रायः सभी उपन्यासों में मिलती है। लेखक को देश का अग्रदूत मानते हुए उन्होंने कहीं पर भी अपने आदर्श और मर्यादा को हाथ से नहीं जाने दिया है। उनका विचार था कि लेखक पर समाज और देश का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। पाश्चात्य सभ्यता के भारत में बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध भी प्रेमचंद जी ने प्रकाश डाला है और उसका हर प्रकार से खंडन किया है। उन्होंने पश्चिम के नारी स्वातन्त्र्य के प्रतिपादन पर भी प्रकाश डाला है। गृहस्थी-संचालन के मूल में प्रेमचंद ने सेवा को प्रधान स्थान दिया है। आँख मींचकर नकल करना उन्हें पसंद नहीं था। वैसे पश्चिमी सभ्यता से आदान-प्रदान की भावना को आपने प्रश्रय दिया है। नारी को वहाँ भोग-विलास की उच्छृंखल-सामग्री मात्र न मानकर गृहस्वामिनी मानकर चलते हैं। गोदान में ‘मालती’ के जीवन में भारतीयता आ जाने से भारतीय संस्कृति की प्रधानता स्पष्ट हो जाती है। लेखक जिस मार्ग को उचित समझता है उसी मार्ग पर उसे ले जाता है। इस प्रकार ‘गोदान’ विशेष रूप से भारतीय सामाजिक समस्याओं का स्पष्टीकरण है, जिसमें लेखक विशेष कलात्मक रूप से सफल हुआ है। यह लेखक की सबसे परिपक्व रचना है और इसमें उसने उपन्यास-साहित्य का उच्चतम उत्कर्ष उपस्थित किया है।