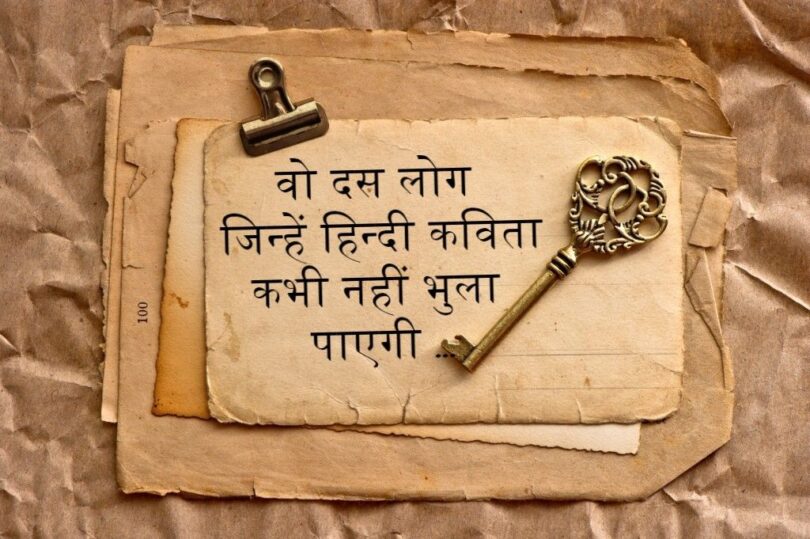हिंदी साहित्य का नवीन युग भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी के काल से प्रारंभ होता है। इस युग को वर्तमान युग का गद्य-युग भी कहते हैं। गद्य-युग कहने का यह तात्पर्य कभी नहीं समझना चाहिए कि इस काल में पद्य का सर्वथा लोप हो गया और उसका स्थान गद्य ने ले लिया। इस युग में गद्य साहित्य के साथ पद्य साहित्य भी अबाध रूप से प्रवाहित होता चला आ रहा है। इतिहास के विद्वानों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि साहित्य काल का प्रतिबिंब होता है। जिस काल में जो साहित्य लिखा गया है उसकी व्यापक परिस्थितियों का प्रभाव प्रधान रूप से उस पर पड़े बिना नहीं रह सकता। हिंदी साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालकर देखिए कि राजपूतों के उच्छृंखल काल में बीरगाथाओं का साहित्य प्रस्फुटित हुआ, मुसलमानी राज्य-काल में निराश्रित जनता ने भक्ति का आश्रय लिया और देश में भक्ति साहित्य का प्रसार हुआ, और फिर वर्तमान काल में जब संसार बदल रहा था तो भारत भी दास नहीं रह सकता था, इस मूल्य को पहिचान कर भारत के आत्मसम्मानी नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन प्रारंभ किये, जनता में देश प्रेम और स्वतंत्रता की भावना जाग्रत हुई, जिसके फलस्वरूप साहित्य में भी राष्ट्रीयता की लहर उठी और वह कवियों की वाणी बनकर जनता के हृदयों में छा गई। यह पहली प्रवृत्ति है वर्तमान युग की कविता की। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत भारतेंदु-युग से लेकर आज तक अनेकों कवियों ने सुंदर काव्य की रचना की है। यहाँ हम मैथिलीशरण जी की ‘भारत-भारती’, सुभद्राकुमारी चौहान की ‘झांसी की रानी’ और माखनलाल चतुर्वेदी की ‘सुमन के प्रति’ या ‘पुष्प की अभिलाषा’ कविता को नहीं भुला सकते।
प्राचीन युग से इस युग में दूसरा परिर्वतन भाषा के दृष्टिकोण में हैं। इस काल की कविता का साहित्य खड़ीबोली में लिखा गया है। एक प्रसिद्ध प्राचीन मत था कि खड़ीबोली में सरल कविता नहीं लिखी जा सकती। वर्तमान युग के प्रसिद्ध कवि ‘जयशंकर प्रसाद’, ‘मैथिलीशरण गुप्त’, आचार्य ‘निराला’, सुमित्रा नंदन ‘पंत’, ‘महादेवी वर्मा, कविवर ‘बच्चन’ इत्यादि ने इस प्राचीन मत की धज्जियाँ बिखेरकर उसे एक उपहास की वस्तु बना दिया। गीत-गोविंद की सरसता लेकर हिंदी खड़ीबोली में पद लिखे गए और कविताएँ रची गईं।
यहाँ कामायनी का एक सरस पद देखिए-
“तुमुल कोलाहल में, मैं हृदय की बात रे मन!
विकल होकर नित्य चंचल, खोजति जब नींद के पल,
चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन-
जहाँ मरूँ ज्वाला धधकती, चातकी, धन को तरसती,
उन्हीं जीवन घाटियों में, मैं सरस बरसात रे मन!”
इस काल में कविता विभिन्न धाराओं में बही है। कुछ प्राचीन प्रणाली के भी कवि इस काल में हुए हैं परंतु कोई विशेष महत्त्वपूर्ण पुस्तक या कविता उन कवियों की नहीं मिलती। इसलिए विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं। रत्नाकर इस काल के प्राचीन प्रणाली के उल्लेखनीय कवि हैं। खड़ीबोली-साहित्य के इस युग में कई नवीन वादों का प्रादुर्भाव हुआ। इन वादों में दो वाद छायावाद और प्रगतिवाद उल्लेखनीय हैं। कुछ फुटकरवाद भी सामने आए परंतु उनकी कोई महत्त्वपूर्ण रूपरेखा नहीं बन सकी।
यह काल बुद्धिवाद के विकास का है, इसमें रूढ़िवाद के लिए कोई स्थान नहीं। अंग्रेजी साहित्य के पठन-पाठन से स्वतंत्रता के विचारों का प्रचार हुआ। हिंदी-कविता केवल शृंगार, भक्ति और रीतिकालीन प्रवृत्तियों के सीमित क्षेत्र से निकलकर स्वतंत्र मानव-विश्लेषण के क्षेत्र में आ गई। मानव जीवन की कठिनाइयों और परिस्थितियों के अंदर साहित्य ने झाँका और उनके विश्लेषण की ओर अग्रसर हुआ। अंग्रेजी राज्य इस समय व्यवस्थित था, इसलिए जनता के विचारों में भी वीरगाथा काल की उच्छृंखलता नहीं थी। साहित्य में भी स्थिरता आई और काव्य में जीवन की अनेक समस्याओं के साथ अनेकरूपता भी आई। साहित्य का क्षेत्र परिमित न रहकर विस्तृत हो चला। जातीयता और समाज-सुधार की ओर लेखकों का ध्यान गया। काव्य ने सादगी, सौंदर्य को पहिचाना जिससे रीतिकालीन प्रवृत्ति का एकदम ह्रास हुआ।
खड़ीबोली कविता की कुछ विशेषताएँ हैं जो पुरानी किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती। इसमें हमें संस्कृत छंदों का प्रयोग मिलता है। ब्रजभाषा के छंद इसके लिए उपयुक्त नहीं हो सके। शब्दों के तद्भव रूप प्रयोग में न लाकर कवि तत्सम रूप प्रयोग में लाए हैं। कविताओं में जो तुकों की प्रधानता आ गई थी इस युग के कवियों ने अपने को उनसे मुक्त कर लिया और बहुत सुंदर अतुकांत कविताएँ लिखीं। इस धारा को प्रवाहित करने का श्रेय महा-कवि ‘निराला’ को है।
नाथूराम शर्मा, अयोध्यासिंह उपाध्याय, मैथिलीशरण गुप्त, सियारामशरण गुप्त इस एक धारा के कवि हैं। इन कवियों ने विविध विषयों पर सफलतापूर्वक लेखनी उठाई है और हिंदी साहित्य को ‘साकेत’ ‘प्रिय प्रवास’ और ‘भारत-भारती’ जैसी अमूल्य रचनाएँ प्रदान की है। माखनलाल चतुर्वेदी, ‘नवीन’, सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि ने राष्ट्रीय कविताएँ लिखी हैं।
तीसरी धारा के कवियों में जयशंकर ‘प्रसाद’, ‘निराला’, ‘पंत’, ‘महादेवी वर्मा’ इत्यादि के नाम उल्लेखनीय हैं। ‘कामायनी’ और ‘यामा’ इस धारा की अमूल्य देन हैं और हिंदी साहित्य की और अनेकों अन्य पुस्तकें भी। पल्लव, गुंजन, अनामिका, यह सभी सुंदर कविताओं के संग्रह हैं। जिनमें अपनी-अपनी विशेषता विद्यमान है।
कविवर ‘बच्चन’ ने ‘हालावाद’ की अपनी पृथक् धारा प्रवाहित की परंतु वह उसी तक सीमित न रहे अतः उन्होंने प्रगतिवादी कविताएँ तथा कुछ-कुछ छायावादी कविताएँ भी लिखीं।
इस काल का कवि भक्ति काल की स्वतंत्रता अपने में रखता है और वीरगाथा काल की स्वछंदता तथा रीतिकाल की रसिकता। इस प्रकार तीनों काल का निचोड़ हमें इस काल में मिलता हैं। इस काल का कवि किसी का आश्रित नहीं, उसे किसी की प्रशंसा नहीं करनी है। वह अपनी इच्छा का स्वछंद पुजारी है। जैसा चाहता है, लिखता है। उस पर किसी का अंकुश नहीं। यही कारण है कि आज का साहित्य बंधन-विहीन साहित्य है जो किसी काल, विषय अथवा भावना के साथ नहीं बांधा जा सकता। यह मुक्त है और पूर्ण वेग के साथ अबाध रूप से सर्वन्नोमुखी होकर प्रसारित हो रहा है। संसार के सभी उच्चतम साहित्यों के साथ-साथ आशा है कि निकट भविष्य में ही हिंदी कवि का साहित्य आगे बढ़ता जाएगा।