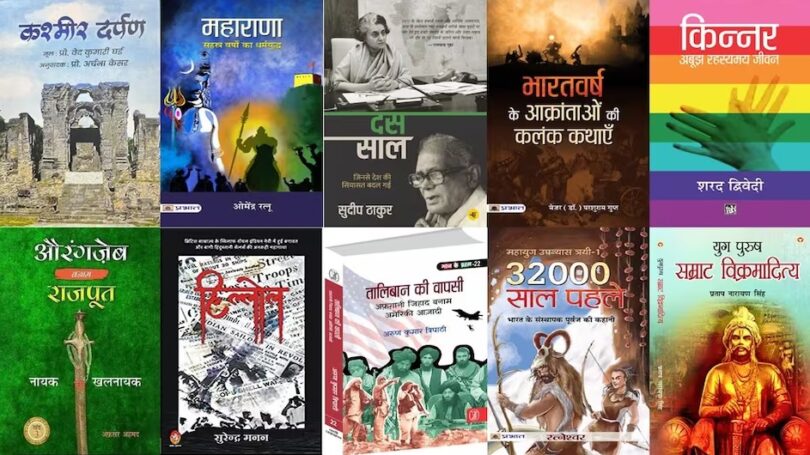हिंदी में गद्य का उत्थान हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने तीन कालों के अंतर्गत विभाजित किया है। भारतेंदु से पहले काल, भारतेंदु-काल और फिर द्विवेदी-काल। गल्प और उपन्यास साहित्य का प्रारंभ हमें निबंधों की भाँति भारतेंदु से पूर्व के काल में न मिलकर उन्हीं के काल से मिलता है। भारतेंदु बाबू से पूर्व जो कथाएँ मिलती भी हैं उनका साहित्यिक महत्त्व कुछ नहीं है।
नाटक-साहित्य की भाँति कथा-साहित्य भी हिंदी में सर्वप्रथम मौलिक रचनाओं द्वारा न आकर अनुवादों के ही रूप में आया। संस्कृत साहित्य उपन्यास या कहानी के प्रकार का साहित्य नहीं मिलता। इसलिए संस्कृत से अनुवाद होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। प्रथम अनुवाद बँगला और अंग्रेजी से हुए, परंतु इनकी भाषा अधिक रोचक नहीं बन पाई, क्योंकि उस समय तक भाषा में रोचकता का अभाव था और वह धीरे-धीरे सुधर रही थी। गदाधर सिंह, रामकृपाल वर्मा और कार्तिक प्रसाद खत्री इस काल के प्रधान अनुवादक थे।
लाला श्रीनिवास को हम हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास-लेखक मानते हैं। आपके ‘परीक्षा गुरू’ उपन्यास का शिक्षित समाज में काफ़ी आदर हुआ। इसके पश्चात् तो मौलिक तथा अनुवादों की हिंदी में झड़ी लग गई। बाबू राधाकृष्ण जी का ‘निःसाहय हिंदू’, बालकृष्ण भट्ट का ‘नूतन ब्रह्मचारी’, गोपाल राम गहमरी के बँगला के अनुवाद, अयोध्यासिंह उपाध्याय का ‘वेनिस का बाँका’ तथा देवकीनंदन खत्री की ‘चंद्रकांता संतति’ इस काल की प्रमुख रचनाएँ हैं।
इस काल में उपन्यास केवल दिलचस्पी के लिए या चमत्कारप्रधानता के लिए ही लिखे गए। उनमें न तो चरित्र चित्रण ही किसी काम का था और न सामाजिक समस्या और उन पर विवेचना ही। भाषा में प्रवाह अवश्य था और कथा की तारतम्यता तो उनकी विशेषता थी। इस काल के मौलिक उपन्यास उच्च कोटि के साहित्य की श्रेणी में नही रखे जा सकते। उनकी विदेशी अनुवादों से कोई तुलना नहीं। देवकीनंदन खत्री के अतिरिक्त किसी अन्य लेखक ने जनता को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया।
इस काल के पश्चात् हिंदी उपन्यासों तथा कहानियों का नवीन काल प्रारंभ होता है। और यह काल बहुत महत्त्वपूर्ण भी है। युग का संचालक तथा प्रतीक हम मुंशी प्रेमचंद को मानते हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रथम उपन्यासकार हैं जिन्होंने तिलस्म और अय्यारी को छोड़कर सामाजिक समस्याओं के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की ओर ध्यान दिया। आपने हिंदी के उपन्यास-साहित्य के अभाव को पहिचाना और अपने प्रयत्नों द्वारा उस अभाव की पूर्ति की। यहाँ हम कथा के इस युग को शैली की विचार धाराओं में विभक्त करते हैं। इन तीनों के प्रवर्तक मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर ‘प्रसाद’ तथा पाण्डेय बेचन शर्मा ‘उग्र’ हैं।
प्रथम धारा, जो प्रेमचंद ने बहाई, उसकी भाषा विशुद्ध होते हुए भी अपने अंदर में उर्दू के शब्दों बिलकुल नहीं खो पाई। यह मुहावरेदार कुछ उर्दू-मिश्रित हिंदुस्तानी का चलता स्वरूप है जो उपन्यासों के लिए उपयुक्त भी रहा और लोकप्रिय भी बन गया। इस भाषा में रवानी है और गांभीर्य भी। इस धारा के लेखकों में नवीनता अवश्य पाई जाती है परंतु प्राचीनता का भी सर्वथा अभाव नहीं। सामाजिक समस्याओं को लेकर इस धारा के लेखकों ने लेखनी उठाई और काफी सफलतापूर्वक उन समस्याओं पर प्रकाश डाला, परंतु फिर भी इनकी लेखनी द्वारा समाज का वह स्पष्ट और सत्य चित्रण नहीं हो पाया, जो आज का समालोचक चाहता है। इस धारा के लेखकों के चित्रण बहुत लंबे होते हैं और उनमें वर्णनों की भरमार रहती है। अंग्रेजी साहित्य के विक्टोरिया-काल की झलक इनके साहित्य में मिलती है। संक्षेप में कुछ कहे जाने की प्रवृत्ति उनमें नहीं थी। इन लेखकों में उपदेशात्मक प्रवृत्ति भी थी। मानो लेखक होते के नाते उपदेशक होने का भार भी इन्होंने अपने सिर पर ले लिया था। इस धारा के प्रधान लेखक मुंशी प्रेमचंद, विश्वनाथ कौशिक तथा पंडित सुदर्शन इत्यादि हैं।
दूसरी धारा को प्रचलित करने वाले थे बाबू जयशंकर ‘प्रसाद’। इनके उपन्यास और कहानियों में आदर्शवाद को प्रधानता दी गई है। इनके चित्रण बहुत सजीव और मार्मिक हैं परंतु इनकी भाषा उपन्यासों और कहानियों के अनुकूल नहीं है। इनकी भाषा में तत्सम शब्दों का ही अधिक प्रयोग मिलता है, इसलिए कम हिंदी जानने वाले पाठकों में आपकी रचनाएँ अधिक प्रसारित नहीं हो सकीं। भावुकता इनकी रचनाओं में कूट-कूटकर भरी है। कहीं-कहीं पर तो कहानियों में कविता का मिठास आ जाता है और साथ ही साथ गांभीर्य भी। इनकी कथाओं में बुद्ध-कालीन संस्कृति का चित्रण मिलता है। ग्रामीण दृश्यों का भी चित्रण है, परंतु बहुत कम। कथाओं में कथोपकथन अधिक मिलते हैं, चरित्र चित्रण बहुत सजीव हैं। चंडीप्रसाद जी ‘हृदयेश’ इत्यादि इस धारा के अन्य लेखक हैं। इस धारा में प्रवाहित होने के लिए पांडित्य की आवश्यकता थी और कथा लेखकों में इसका अभाव होता है। इसलिए इस धारा में बहने वाले बहुत कम लेखक साहित्य में पैदा हो सके। इस धारा के साहित्य का मूल्य रचनात्मक साहित्य की दृष्टि से बहुत अधिक है।
तीसरी धारा, जिसके प्रवर्त्तक ‘उग्र’ जी थे, बहुत चटपटी भाषा तथा विचारों के साथ साहित्य में आई। मनचले नौजवानों और प्रेम पुजारियों ने के इसका हाथों-हाथ आगे बढ़कर स्वागत किया और इस धारा का प्रचार भी बहुत हुआ; परंतु यह धारा हिंदी साहित्य का कुछ अधिक हित नहीं कर सकी। इस धारा का साहित्य उच्चकोटि के साहित्य की श्रेणी में नहीं आ सका और समाज के चरित्र को सुधारने तथा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में भी इसने कोई सहयोग नहीं दिया। इस धारा के लेखकों ने समाज के नग्न चित्र प्रस्तुत किए हैं और जीवन की कमजोरियों को ज्यों-का-त्यों खोल-कर रख दिया है। लेखकों ने कमजोरियों को केवल खोलकर रख देना ही अपना कर्त्तव्य समझा है, कोई सुझाव वह प्रस्तुत नहीं कर सके। इस धारा की रचनाओं में गांभीर्य का अभाव रहा है। यही कारण था कि इसकी रचनाएँ केवल एक ही वर्ग द्वारा अपनायी गईं। पाण्डेय बेचन ‘उग्र’ आचार्य चतुरसेन शास्त्री इत्यादि इस धारा के प्रमुख लेखक हैं।
इस प्रकार इन धाराओं में बहता हुआ साहित्य (उपन्यास तथा कहानी) उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ। आज के युग का हिंदी-कथा-साहित्य बहुत समुन्नत दशा में है और वह किसी भी अच्छे साहित्य के सम्मुख तुलना के लिए रखा जा सकता है। आज हिंदी में बहुत अच्छे लेखक हैं जो इस साहित्य को निरंतर उन्नति देने में जुटे हुए हैं और अपनी एक-से-एक अच्छी रचना पाठकों को प्रदान कर रहे हैं। इस साहित्य का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।