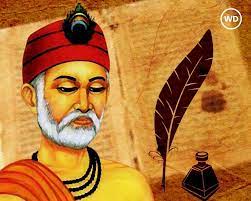संत कबीर का प्रादुर्भाव जिस काल में हुआ, उस समय देश के वातावरण में एक भारी उथल-पुथल थी। विभिन्न मत-मतांतरों और धर्मों का प्रचार इधर-उधर उनके धर्मानुयायी कर रहे थे। मुसलमान अपना राज्य स्थापित कर चुके थे और हिंदू तथा मुसलमान धर्मों में प्रधान रूप से संघर्ष चल रहा था। धर्म-परिवर्तन के लिए बल का प्रयोग किया जा रहा था और एक धर्मावलंबी दूसरा धर्म अपनाने के लिए विवश किए जा रहे थे।
प्रत्येक धर्म के दार्शनिक पक्ष में भिन्नता पाई जाती थी। सुन्नियों और सूफियों में भी परस्पर मनोमालिन्य कम नहीं था। हिंदी कविता पर सूफी-सिद्धांतों का गहरा प्रभाव पड़ा और एक प्रेम मार्गी धारा ही बह निकली। इस धारा के अंतर्गत आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रेम द्वारा कराया गया है। महाकवि जायसी का पद्मावत् काव्य इस दिशा में महत्त्वपूर्ण ग्रंथ है।
हिंदू धर्म में भी संप्रदायों की कमी नहीं थी सभी के दर्शनों में कुछ-न-कुछ अंतर और मतभेद पैदा हो गया था। शाक्त शक्ति की उपासना करते थे और उनका विश्वास पंच मकार (मत्स्य, मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा) में था। शैवों तथा वैष्णवों में भी पारस्परिक संघर्ष कम नहीं था। द्वैत और अद्वैत के पचड़े में लोगों को डाला जा रहा था। अद्वैतवादी ‘जग मिथ्या’ कह कहकर अपना प्रचार कर रहे थे। इनके अनुसार ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद प्रकट हो रहा था वह मायाजन्य है। यदि मनुष्य ज्ञान के आलोक में देखे तो माया का जाल कट सकता है। ज्ञान द्वारा ही आत्मा और परमात्मा का एकीकरण संभव है। इसी समय हठ योग के आधार पर गोरखपंथियों का भी मत भारत में प्रतिष्ठा पा चुका था और उसके अनुयायियों की भी कमी नहीं थी।
यह तो थी भारत के धार्मिक क्षेत्र की परिस्थिति। सामाजिक क्षेत्र की स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। हिंदू समाज में जाति-पाँति और छूतछात की बुराइयों आ चुकी थीं। मूर्ति पूजा का प्रचार बढ़ चला था और वास्तविकता से लोग पीछे भाग रहे थे। जनता में धार्मिक ठेकेदारों ने भाँति-भाँति के अंधविश्वास फैला रखे थे और यही दशा मुसलमान जनता की भी थी। हिंदुओं की जाति-पाँति व्यवस्था का उन पर भी प्रभाव कम नहीं हुआ और उनके भी आपस में कई दल बन गए।
ऐसी धार्मिक और सामाजिक परिस्थिति में संत कबीर का जन्म हुआ। संत कबीर का साहित्य परिस्थितिजन्य है और उसमें समय की पूरी-पूरी छाप मिलती है। साहित्यिक दृष्टिकोण से यह वीरगाथा का भग्नावशेष था और एक नवीन युग का सूत्रपात्र हो रहा था। भाषा का रूप भी बदल चुका था और वह जनता की प्रचलित भाषा का रूप धारण करती जा रही थी। केवल राज-स्थान तक ही उसकी सीमा न रहकर अधिक व्यापक क्षेत्र में उसका प्रचार बढ़ता जा रहा था।
संत कबीर ने अपने साहित्य द्वारा हिंदी में एक नवीन धारा की आधार-शिला की स्थापना की जिसे साहित्यकारों ने बाद में जाकर भक्ति-काल नाम दिया। आपका साहित्य मुसलमानों तथा हिंदुओं में सामंजस्य स्थापित करने के निर्मित लिखा गया और आपने एकेश्वरवाद पर जोर दिया। आपने अपनी कविता में हिंदू तथा मुसलमानों, दोनों पर ही, कसकर छींटे कसे हैं। आपने राम और रहीम में कोई अंतर नहीं माना। इन नामों की विभिन्नता में फँसकर लोग अपना अहित कर रहे हैं, पारस्पारिक संघर्ष को बढ़ाकर जीवन की शांति को खो रहे हैं, यह उनके लिए खेद का विषय था। आप तो विभिन्न धर्मों को परमात्मा की प्राप्ति के विभिन्न मार्ग मानते थे। आपने ईश्वर को सगुण और निर्गुण से परे मानकर दोनों विचारधाराओं के पारस्परिक मतभेद को मिटाने का प्रयत्न किया –
“सरगुन निरगुन ते परे तहां हमारा ध्यान”
आपने अपने साहित्य में, हिंदू तथा मुसलमान, दोनों में फैली हुई सामाजिक कुरीतियों की कटु आलोचना की है। दोनों ही धर्मो के अंधविश्वासों का आपने खंडन किया है। मूर्ति पूजा तथा जाति-पाँति के भेद-भावों के विपरीत आपने जी खोलकर लिखा है।
“दुनिया कैसी बावरी, पत्थर पूजन जाए।
घर की चकिया कोई न पूजे, जाका पीसा खाय॥”
आप देवी-देवताओं, पीर पैगंबरों, मठ और माताओं इत्यादि पर नाक रगड़ने को मूर्खता मानते थे। तिलक, माला, चंदन इत्यादि में आपने ढोंग ही पाया। आपने अंत:करण की शुद्धि पर बल दिया है। स्पष्ट शब्दों में आपने भक्तों को समझाया कि आप लोग — ‘कर का मनका छाँड़िकै मन का मनका फेर’। दिखावों की बातों में फँसना और उनके द्वारा जनता का अहित करना कबीरदास जी का सिद्धांत नहीं था। आपने हिंदू तथा मुसलमान दोनों के धर्मों में फैली हुई भ्रांतियों तथा कुप्रथाओं का खंडन किया और सद्भावना के साथ जनहित की भावना को साथ लेकर विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने का प्रयत्न किया।
कबीर का दर्शन हमें उनके रहस्यवाद की भावना में मिलता है। रहस्यवाद के अंतर्गत आत्मा की अंतहित प्रवृत्ति शांति और निश्छल रूप से अपना संबंध परमपिता परमात्मा से स्थापित कर लेती है और इस प्रकार दोनों में कोई भेद-भाव नहीं रहता। आत्मा शुद्ध होकर इस स्थिति में इतनी पवित्र हो जाती है कि उसे अपने में और राम में कोई अंतर नहीं प्रतीत होता। इसी स्थिति में कबीरदास जी कहते हैं-
“ना मैं बकरी, ना मैं भेड़ी, ना मैं छुरो गंडास में।
दूँढना होय तो दूँ ढले बन्दे मेरी कुटी मवास में॥”
आपके रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफ़ी प्रेमवाद का सम्मिश्रण मिलता है। अद्वैतवादी होने के नाते आपने माया को माना है और माया के बीच से हटाने पर आपने आत्मा और परमात्मा का मेल संभव गिना है। माया से आत्मा की मुक्ति केवल ज्ञान के आश्रय से हो सकती है। कबीर के साहित्य पर यह सूफी-धर्म का प्रभाव है कि उन्होंने परमात्मा को स्त्री स्वरूप में और आत्मा की पुरुष स्वरूप में देखा है।
अद्वैतवाद और सूफीमत के अतिरिक्त आपका साहित्य हठयोग की भी विभिन्न प्रकार की उक्तियों से भरपूर है। कबीरदास जी स्वयं हठयोगी थे या नहीं इसके विषय में निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता परंतु इतना तो निश्चय ही है कि उनका ज्ञान हठयोग के विषय में कुछ कम नहीं था। उन की कविता में ‘हठयोग की क्रियाओं का विस्तार के साथ वर्णन मिलता है। हठयोग के अनुसार नाड़ी तत्त्व और गुणों को आधार मानकर आपने कई रूपक प्रस्तुत किए हैं। निम्नलिखित रूपक में शरीर का चादर में मिलान किया गया है-
झीनी-झीनी बीनी चदरिया।
काहे का ताना काहे को भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया।
इंगला, पिंगला, ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया।
अष्ट कमल दल चरखा डोल, पाँच तत्त्व गुन बीनी चदरिया,
साँई को बुनत मास दस लागे, ठीक-ठीक के बोनी चदरिया।
इस प्रकार आपका साहित्य धर्म, अध्यात्म, दर्शन और समाज के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखता है। विचारधारा के अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में भी आपकी कविता कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। आपकी भाषा प्रधानतया पूर्वी ही है परंतु उसमें अवधी, खड़ी, ब्रज, बिहारी, पंजाबी और राजस्थानी की यहाँ-वहाँ पुट मिलती है। जहाँ तक छंदों का संबंध है वहाँ तक पिंगल के नियमों का पालन नहीं दिखलाई देता। आपके छंदों में विभिन्न प्रकार के दोष दिखलाई देते हैं। मात्राओं की कमी या आधिक्य और यति भंग इत्यादि दोष से मुक्त तो शायद ही कोई छंद हो। इनके अतिरिक्त आपकी भाषा भी सुसंस्कृत और परिमार्जित नहीं है, परंतु इन दोषों के रहने पर भी आपके साहित्य में सरस-रस की धारा प्रवाहित होती है, और हृदय की भावना का प्रवाह बहुत ही मार्मिक ढंग से हुआ है। आत्मा के संयोग और वियोग पक्ष को लेकर कवि ने संयोग तथा विप्रलंभ का सुंदर निर्वाह किया है। कहीं-कहीं पर भक्त की सूर से उपमा देकर वीर रस भी प्रवाहित किया गया है। अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग कबीरदास की कविता में मिलता है।
इस प्रकार कबीरदास के साहित्य को हम हर दृष्टि से सफल और महत्त्व-पूर्ण समझते हैं। यह समय की आवश्यकता का साहित्य था जिसमें कवि ने अपने ज्ञान और सरसता का वह श्रोत प्रवाहित किया है कि जिसने भारतीय जनता के जीवन में सामंजस्य, सुख, शांति और सरसता का संचार करने का भरसक प्रयत्न किया है। आपकी कविता में भक्ति काव्य की दृष्टि से हार्दिक विदग्धता किसी प्रकार सूर तथा तुलसी-साहित्य से कम नहीं है।