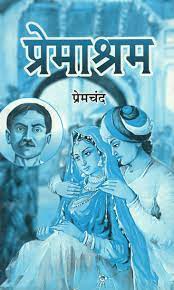‘प्रेमाश्रम’ सेवासदन के पश्चात् मुंशी प्रेमचंद जी का दूसरा उपन्यास है। ‘प्रेमाश्रम’ में उपन्यासकार ने किसी एक चरित्र का निर्माण नहीं किया वरन् अनेकों चरित्रों का निर्माण किया है। प्रेमचंद जी चरित्र चित्रण-कला में इतने प्रवीण थे कि कहीं पर भी उनके चरित्र चित्रण में शिथिलता देखने को नहीं मिलती।
‘प्रेमाश्रम’ में समाज के साथ-साथ लेखक ने राजनीति के क्षेत्र में भी पदार्पण किया है। देश-प्रेम भावना से उपन्यास के प्रधान पात्र ओत-प्रोत होकर चलते हैं। समय की प्रायः सभी प्रचलित विचारधाराओं का समावेश हमें इस उपन्यास में मिलता है। समाज और राजनीति की प्रतिनिधि विचारधाराओं को लेकर ही उपन्यासकार ने अपने इस उपन्यास की रचना की है और यही कारण है कि ‘प्रेमाश्रम’ को पढ़कर उस समय का प्रत्यक्ष चित्र पाठक के नेत्रों में झूलने लगता है। ‘प्रेमाश्रम’ के विषय में ‘प्रेमाश्रम’ की समालोचना करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग करें? बंकिमचंद्र जी के उपन्यासों को देखकर अंग्रेजी-साहित्य से परिचित समालोचक तुरंत कह सकते हैं कि यह स्काट के ढर्रे के ऐतिहासिक उपन्यास हैं। रवींद्रनाथ जी के उपन्यासों को आप सामाजिक कहते हैं। आपको अंग्रेजी साहित्य में इनकी जोड़ के बहुत से उपन्यास-लेखक मिलेंगे। जार्ज ईलियट, थैकरे या डिकेंस-इसके तथा रवींद्रनाथ जी के उपन्यास-क्षेत्र में कोई भारी भेद नहीं है। परंतु प्रेमचंद जी के उपन्यास इन श्रेणियों में से किसी में नहीं आ सकते। इन उपन्यासकारों का काम यह है कि किसी समय के समाज का चित्र खींच दिया, और पात्रों से सहानुभूति दिखाकर, उनको उठाकर, या उन्हें नीचा दिखाकर पाठकों के चरित्र सुधारने का प्रयत्न किया। परंतु इनमें भविष्य का चित्र नहीं है। कला में शायद प्रेमचंद जी से अधिक निपुण हों, परंतु इनमें वह उत्तेजना शक्ति नहीं, उतना कल्पना का विकास नहीं। वे समाज के सामने एक आइना रख सकते हैं जिसे देखकर वह हँसे या कुढ़े। परंतु उस आइने के पीछे कोई चित्र नहीं, जिसकी सुंदरता तक पहुँचने के लिए उसके हृदय में उत्तेजना हो।
‘प्रेमाश्रम’ के उपन्यास-पट पर तो 1921 के भारतीय समाज का स्पष्ट चित्र है और पीछे किसी भावी भारत की छाया। ऐसे चित्र का क्या नामकरण हो? क्या ‘प्रेमाश्रम’ दार्शनिक उपन्यासों की श्रेणी में रखा जाए?
मुंशी प्रेमचंद देहाती झगड़ों के करुणाजनक चित्रण में बहुत सफल हुए हैं। यों तो राय कमलानंद, गायत्री, विद्या, ज्ञानशंकर, ज्वालासिंह, डॉ० इर्फान-अली के राग-रंग नगर निवासियों के हैं, परंतु उनका अस्तित्व देहात पर ही है। सुक्खू, बिलासी, मनोहर, बलराज, क़ादिर मियाँ-वे सब तो पूरे देहाती ही हैं।
चरित्र चित्रण कला को जाने दीजिए। शायद किसी और समय, देहाती और बेगार मुकदमेबाजी और नौकरी के प्रश्न इतने रुचिकर न होते, पर यह उपन्यास सन् 1921 का लिखा हुआ है और उस वर्ष के अंदर जितना आंदोलन और राजनैतिक ज्ञान देहातों में पहुँच गया, उतना शायद ही साधारण रूप से 50 वर्ष में पहुँचता।
‘प्रेमाश्रम’ हाजीपुर का दूसरा नाम है, परंतु उपन्यास की नींव में लखनपुर है। वह बनारस के पास हो या कलकत्ते के — इससे कोई प्रयोजन नहीं। सुक्खू चौधरी जैसे पंचों के सरपंच क़ादिर मियाँ जैसे नरम देहाती नेता, मनीपुर के अक्खड़ किसान, बलराज जैसे उदार हृदय और बलिष्ठ नवयुवक भारतवर्ष के प्रत्येक गाँव में मिलते हैं। उनके प्रभाशंकर कैसे जमींदार थे, जो अभ्यगतों के सम्मान में अपनी इज्जत समझते थे, आसामियों के प्रति सहानुभूति थी और उसके विरुद्ध अदालत जाने में संकोच होता था; ऐसे जमीदार भी सुखी थे और उनके किसान भी।
परंतु इधर पाश्चात्य सभ्यता के साथ मालिकों की आवश्यकताएँ भी बढ़ीं। जिन ज़मीदारों के पुरखे बहलियों पर चढ़ते थे, घुटने के ऊपर तक धोती और चार आने सिलाई का अँगरखा या मिर्जई पहनते थे, उनकी संतानों के लिए मोटर की सवारी, लम्बी रेशमी किनारे की धोती और साहबी ठाट की आवश्यकता पड़ने लगी। देहात की उन्नति कौन करता, इज़ाफ़ा और बेदखली का अत्याचार होने लगा।
अभी तक लखनपुर पर सिर्फ़ उन पर अत्याचार है जो वर्षा ऋतु के बाद गाँवों पर धावा करते हैं। अभी ज्ञानशंकर ने जमींदार पर हाथ नहीं लगाया। इसीलिए अभी मनोहर के साथियों का यही विचार है कि अंग्रेज हाकिम अच्छे होते हैं। परंतु इधर प्रभाशंकर का बुढ़ापा, जमींदारी की आमदनी से ज्यादा खर्च, और इधर ज्ञानशंकर पर पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव और योवन की उमंग। ज्ञानशंकर ने हर तरफ हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया; बस, इनके पदार्पण से उपन्यास का प्रादुर्भाव हुआ।
यहाँ पर प्रश्न होता है कि इस उपन्यास में कोई नायक और नायिका है या नहीं? यदि है तो कौन है, और नहीं है तो क्यों नहीं है?
यह तो हम मान ही नहीं सकते कि इस उपन्यास में नायक और नायिका हैं ही नहीं। यदि चरित्र की उज्ज्वलता पर ही ध्यान दिया जाए, तो एक और प्रेमशंकर और दूसरी ओर विद्या-यही पात्र लेखक के आदर्श मालूम पड़ते हैं। इस उपन्यास में ज्ञानशंकर का चरित्र आदरणीय नहीं है। गायत्री भी विद्या के समान तुच्छ मालूम पड़ती है। परंतु हैं ये ही उपन्यास के नायक और नायिका। ज्ञानशंकर न होते तो कोई लखनपुर का नाम ही न सुनता।
ज्ञानशंकर का चरित्र बहुत जटिल है। एक भारतीय नवयुवक पर पश्चिमी शिक्षा की नई रोशनी का प्राथमिक प्रभाव क्या पड़ता है; यह बहुत ही खूबी के साथ दिखलाया गया है। उच्च शिक्षा ने उसकी भारतीय आत्मा को ही नष्ट कर दिया है। जब कभी किसी पवित्र आत्मा के सामने से उसकी ऐश्वर्य-लोलुपता का परदा हट जाता है, तो हमें उसकी अंतरात्मा के मधुर प्रकाश की झलक दिख पड़ती है, परंतु फिर परदा गिर जाता है। और ज्ञानशंकर फिर उसी ऐश्वर्य छाया की ओर बढ़ता हुआ दिखलाई देता है। ज्ञानशंकर नायक होते हुए भी अपने भाग्य का विधाता नहीं है। वह समझता है कि अपनी चतुरता के बल पर वह अपना भविष्य आनंदमय बना सकेगा, परंतु काल उसे भी नचाता है। प्रभाशंकर की भलमनसाहत, प्रेमशंकर के त्याग, गायत्री की लालसा, ज्वालासिंह का स्वाभिमान, राय कमलानंद की निष्काम संसार-परता, सभी से वह लाभ उठाता मालूम होता है। परंतु किसलिए?
उपन्यास के दो अंग हैं। एक सामाजिक, दूसरा राजनैतिक। ज्ञानशंकर दोनों को बाँधे हुए है। पर इन दोनों में एक-एक प्रधान पात्र भी हैं। सामाजिक अंग पर गायत्री का प्रभुत्व है और राजनैतिक अंग के विधाता प्रेमशंकर हैं।
गायत्री के चरित्र का इजाफे से कोई संबंध नहीं है। वह एक बड़ी भारी जमींदारी की मालकिन अवश्य है। उसके प्रबंध के लिए वह ज्ञानशंकर को बुलाती है परंतु इन बातों का उसके चरित्र से कोई विशेष संबंध नहीं है। गायत्री का पतन धर्म-जाल की ओट से होता है। उसे नहीं मालूम होता कि वह किधर जा रही है और जब अकसमात् उसके सामने पाप का अंधकारमय गढ़ा दिखाई देता है, तो फिर वह समाज को अपना मुँह नहीं दिखाती। हिंदू-विधवा का पतन यों ही होना स्वाभाविक है।
उपन्यास का वह अंश अधिक करुणामय है जिसमें लखनपुर की गाथा है। इस अंश के प्रधान पात्र प्रेमशंकर हैं। यदि पश्चिमी शिक्षा का एक फल ज्ञान-शंकर की ऐश्वर्य-लोलुपता में है तो दूसरा फल प्रेमशंकर की निष्काम जाति-सेवा में। जिस समुद्र में हलाहल विष है, उसमें अमृत भी है। प्रेमशंकर उस शिक्षा के अमृत रूपी फल हैं। कुछ मित्रों का ख्याल है कि प्रेमशंकर में गाँधी जी की छाया है। यदि हम लेखक के मन की थाह लेने का साहस तो करें तो इस पात्र में हमें महर्षि टॉल्स्टाय के चरित्र की हल्की-सी छाया दिखलाई पड़ती है।
ज्ञानशंकर चाहते हैं कि प्रेमशंकर को गाँव का आधा हिस्सा न देना पड़े। इसके लिए क्या-क्या जाल रचे, श्रद्धा को कहाँ तक भरा, बिरादरी को कहाँ तक उभारा। परंतु प्रेमशंकर अमेरिका से और ही पाठ सीख आए है। उन्हें साम्यवादियों के मतानुसार एक आदर्श कृषक संस्था तैयार करनी थी, गाँव को तिलांजलि दे दी और जाति सेवा में लीन हो गए। श्रद्धा छूट गई, उसका उन्हें समय-समय पर शोक होता है। भाई से बिगाड़ हो गया, इसके लिए भी उनकी आत्मा को क्लेश होता है। पर वह अपने कर्त्तव्य से विचलित नहीं होते। इसीलिए लेखक ने भी भविष्य की बागडोर को उनके हाथ से नहीं जाने दिया।
प्रेमशंकर हाजीपुर को एक साम्यवादी गाँव बना कर, लखनपुर का उद्धार करते हैं और मायाशंकर को आदर्श जमींदार का पद देने में सफल होते हैं। प्रेमशंकर के संसर्ग में जो पात्र आया, उसको उन्होंने पवित्र कर दिया। उदंड मनोहर, स्वार्थी ज्ञानशंकर और लालसामयी गायत्री इस योग्य नहीं थे, इसलिए लेखक ने इनका अंत ही कर दिया। सुक्खू चौधरी बैरागी हो गया, ज्वालासिंह डिप्टी कलक्टरी छोड़कर जाति सेवा में रत हुए, डॉक्टर इर्फान अली ने वकालत छोड़ दी और डॉ० प्रियानाथ एक सर्वप्रिय डॉक्टर हो गए; यहाँ तक कि पतित दयाशंकर का भी उन्होंने अपनी सुश्रुषा से उद्धार कर दिया। प्रेमशंकर का जीवन एक प्रकार श्रद्धा के बिना अपूर्ण सा था, सो श्रद्धा और प्रेम का ज्वाला द्वारा सम्मिलन भी हो गया।
और भी पात्र हैं। गाँव में अत्याचारी अंग्रेज नहीं हैं। मनोहर और सुक्खू की गौसखाँ तथा साहबों के अहलकारों से ही शिकायत है। ज्वालासिंह न्याय करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु धोखा खाते हैं और उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। गौसखों का भी वही अंत हुआ जो अत्याचारी जिलेदारों का होता। मनोहर की उद्दण्डता का भी फल उसे मिल गया। सुक्खू को मनोहर के खेतों की बड़ी लालसा थी, परंतु गाँव पर विपत्ति आने पर वह उनका नेता हो गया। कादिर मियाँ गाँव के सच्चे सेवक बने रहे। दुखरन भगत पर विपत्ति का दूसरा ही असर हुआ। निराशा ने उसके हृदय में जन्म भर की संचित शालिग्राम के प्रति श्रद्धा उखाड़कर फेंक दी। बलराज गाँव के भविष्य का युवक है। उसमें जो स्वतंत्रता है, वह किसी में नहीं, क्योंकि उसके पास जो परचा आता है उसमें लिखा है कि रूस में किसानों का राज्य है। यदि परिस्थितियाँ प्रतिकूल हुई तो वह भविष्य का बोल्शेविक होगा। मनोहर की पतिव्रता गृहिणी विलासी इनके झगड़ों को शांत करने का प्रयत्न करती रहती है, पर गाँव में विप्लव उसी के द्वारा होता है। न उस गाँव की द्रोपदी पर गौसखों का अत्याचार होता, न विद्वेष की आग इतनी भड़कती। इस विप्लव के शांत होने पर जो बचते हैं, वे उपसंहार में भावी गवर्नर हिज़ एक्सिलेंसी गुरदत्त राय चौधरी और भावी जमींदार मायाशंकर के समय में रामराज्य का सुख भोग करते हुए दर्शन देते हैं।
कथा-प्रसंग के परे और भी पात्र हैं। राय कमलानंद का चित्र विशेषकर भावमय है। मालूम नहीं कि यह उपन्यास लेखक के मस्तिष्क से निकले हैं या इनकी जोड़ के संसार में कोई हैं भी। इनका जीवन सांसारिक-विलास में मग्न है। पर इससे इनके पौरुष में कोई अंतर नहीं आता। इनकी भोग क्रियाएँ इसीलिए थीं कि जीवन की चरम सीमा तक भोग कर सकें। इनका आत्म-बल इतना प्रखर था कि ज्ञानशंकर भी उनके सामने नहीं ठहर सका, परंतु जीवन का आदर्श त्रुटियों से भरा है।
विद्या और श्रद्धा के चित्र भी उल्लेखनीय हैं। दोनों साधारण हिंदू-रमणियाँ हैं। विद्या के चरित्र में जटिल समस्या की कमी नहीं आई, और जब उस पर कष्ट पड़ता है तो लेखक उसे बरदाश्त करने योग्य न समझकर उसका अंत ही कर देता है। कुटिल ज्ञानशंकर की पतिव्रता पत्नी का यहीं अंत होना था। श्रद्धा के सामने पहले से ही धर्म और प्रेम की समस्या मौजूद है। पर प्रेमशंकर के चरित्र का अंत में उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि धर्म की शृंख-लाएँ ढीली पड़ गई। लेखक ने श्रद्धा को प्रेम से मिलाकर दोनों का जीवन सार्थक कर दिया।
पात्रों का अवलोकन करके अब लेखन शैली पर विचार करें। प्रेमचंद की यह पुरानी आदत है कि भाषा हिंदी ही रहती है, पर शब्दों का रूप पात्रानुसार बदलता रहता है। ‘प्रेमाश्रम’ में देहाती पात्र भी हैं, इसलिए उनके काम में आने वाले शब्द भी वैसे ही हैं। रिसवत, सरबस, मुद्रा, मसक्कत, मूरख, सहूर, अचरज, कागद, ये सब देहातियों के ही शब्द हैं। भाषा सिर्फ करतार की बिगड़ गई है यह ठेठ गँवारू है और जितने देहाती हैं उनकी भाषा में पूर्वोक्त प्रकार के शब्द आने से लालित्य बढ़ ही जाता है।
प्रेमचंद जी अपनी लेखन शैली में ‘इनवर्टेड कॉमाज़’ का प्रयोग न करके प्राचीन परिपाटी का ही अनुसरण किया है। पुरानी हिंदी में इनवर्टेड कॉमाज़ नहीं थे। वार्तालाप में पात्र का नाम और उसके बाद बस कॉमा आ गया। कोई आंतरिक विचार हुए या कोई लम्बी बातचीत हुई तो इसकी आवश्यकता नहीं।
मनोविकार के चित्र तथा विचित्र उपमाएँ उपन्यास-धारा की तरंगों पर कमल के फूलों की तरह दर्शन देती चली जाती है।
यह उपन्यास अपने ढंग का अनूठा उपन्यास है जिसे लिखकर उपन्यासकार ने हिंदी-साहित्य-निधि के कोष को भरा है। यह उपन्यास हिंदी-साहित्य के उन उपन्यासों में से है जिन्हें लेकर हिंदी साहित्य अन्य भाषा के उपन्यासों में सगर्व खड़ा हो सकता है और उसके सम्मुख अपनी महत्ता प्रस्तुत कर सकता है।