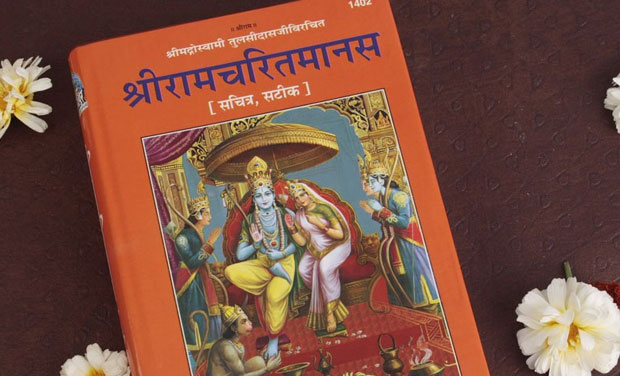प्राचीन भाषाओं में कालिदास कृत ‘रघुवंश’, ‘वाल्मीकीय रामायण’ होमर-कृत ‘ ईलियड’, वर्जित-कृत ‘ईनियड’, फिरदौसी-कृत ‘शाहनामा’ और आधुनिक भाषाओं में मिल्टन का ‘पैराडाइज़ लॉस्ट’ दाँते का, ‘डिवाइन कॉमेडी,’ माइकेल मधुसूदन दत्त का ‘मेघनाद वध’ इत्यादि प्रमुख काव्य माने जाते हैं। रामचरित-मानस को हम बहुत सुगमता से उक्त काव्य ग्रंथों की श्रेणी में रख सकते हैं। भाषा, भाव, काव्य-सौंदर्य, दूरदर्शिता दर्शन, हृदयग्राहिता, पाठकों में सम्मान और व्यापकता सभी दृष्टिकोणों से मानस एक अलौकिक ग्रंथ है जिसकी तुलना संसार के किसी भी महाकाव्य से की जा सकती है। मानस मानव संसार के उन अमर ग्रंथों में से है जिसमें क्षण-भंगुर काव्य का सृजन कवि ने नहीं किया बल्कि मानव के उन मूल भावों का विवेचन किया है जिनके द्वारा कवि ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से मानव समाज का जीता-जागता स्वरूप सामने रख दिया।
महाकाव्य भाषा और भाव का संयोग है। गोस्वामी तुलसीदास ने ‘मानस’ में प्रेम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इत्यादि मानव के सभी विकारों का सुंदर भाषा में चित्रण किया है। मानस की भाषा भारत के अधिकांश वासियों की भाषा है इसलिए इस ग्रंथ का लाभ केवल कुछ इने-गिने साहित्य प्रेमी ही न उठाकर समी काव्य-प्रेमी तथा भक्तों ने उठाया है। हिंदी साहित्य के इस ग्रंथ ने जितनी ख्याति प्राप्त की है उतनी अन्य कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं कर सका। यह भारत की जनता के हृदय का ग्रंथ बना और गले का कंठहार। इसके बिना आज हिंदू जाति की गति नहीं। फिर हो भी भला क्यों नहीं, आप मानस को आद्योपांत पढ़िए और बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक का आनंद-लाभ करिए। बचपन में राम हमारे भाई है, कौशल्या हमारी माता है, दशरथ हमारे वृद्ध पिता हैं। गुरु के साथ जाने को आज्ञा देने पर दशरथ को उसी प्रकार दुख होता है जिस प्रकार वृद्ध पिता को होना स्वाभाविक है परंतु पुत्र आज्ञा-पालन में संकोच नहीं करता। राम धनुर्विद्या सीखते हैं, वन-वन विचरते हैं, यौवनावस्था में कुमारी के प्रेम-पाश में फँसते हैं, सीता-दर्शन होने पर राम और लक्षमण का वार्तालाप सुंदर है। यह सौंदर्य स्वयं वाल्मीकि भी अपनी रामायण में नहीं ला पाए हैं। राम का गार्हस्थ्य जीवन कष्टमय है, संभवतः इसलिए क्योंकि इस जीवन के प्रति कवि स्वयं भी उदासीन था। राम की वन यात्रा का कवि ने बहुत सजीव चित्रण किया है। लंकाकांड में युद्ध वर्णन पुराने ढंग का है और बहुत योग्यता के साथ किया गया है। यहाँ मन्दोदरी का चरित्र-चित्रण स्वाभाविक है। तुलसीदास ने मानसिक चित्र खींचने में जितनी निपुणता बाल-कांड और अयोध्याकांड में दिखलाई है उतनी अन्य किसी कांड में नहीं दिखला पाए हैं। उत्तरकांड तो बालकों और युवकों की समझ में ही आना कठिन है, ज्ञान का वर्णन है त्यागी मनुष्यों के लिए। इस प्रकार यह ग्रंथ आद्यो-पांत अपने-अपने स्थान पर सुंदर है।
इस महाकाव्य में कवि ने समाज के प्रायः सभी पात्रों का सृजन किया है। पुत्र के रूप में राम, लक्ष्मण, भरत, पुत्री सीता, पिता दशरथ, जनक, माता कौशल्या, सुमित्रा कैकेयी; भाई राम, लक्ष्मण, भरत, विभीषण, सुग्रीव; मित्र सुग्रीव, विभीषण; स्त्री सीता, जनता अयोध्या की जनता राजा दशरथ, शत्रु, रावण; देशद्रोही विभीषण, दुष्ट भाई वाली इस प्रकार समाज में जितने प्रकार के भी चरित्र उपलब्ध हो सकते हैं, कवि ने खोज-खोजकर इस महाकाव्य में सफलतापूर्वक चित्रित किए हैं।
मानस कवि की हिंदी साहित्य को एक अनूठी देन है। इस महाकाव्य में तुलसी ने अपने काव्य और दर्शन दोनों का समन्वय किया है। महाकवि तुलसी-दास ने इस ग्रंथ द्वारा उस लोक धर्म का प्रतिपादन किया है जिसकी निर्गुण पंथ के कवि अवहेलना करते चले आ रहे थे। पारस्परिक संबंधों की उदासीनता को दूर कर कवि पति प्रेम, मित्र भक्ति, मातृ-स्नेह, कुल-मर्यादा, अत्याचार का दमन इत्यादि भावनाओं से भारतीय समाज को एक बार फिर से भर दिया है। जनता को कर्त्तव्य की वेदी पर लाकर खड़ा कर दिया है और जीवन को जीवन मानकर चलने का आदेश दिया है। कवि ने जनता के भूले हुए लौकिक कर्त्तव्यों की ओर ध्यान दिलाया। मानस की रचना करके आपने मानस के अंग-प्रत्यंग पर प्रकाश डाला है। व्यक्तिगत साधना और भक्ति के बहाव में मनुष्य को लोक-धर्म ठुकराने की आज्ञा कवि ने नहीं दी। सीता के दुबारा बनवास के पश्चात् राम साधू हो सकते थे परंतु नहीं, उन्हें अपना कर्त्तव्य पालन करना था। इस प्रकार तुलसीदास ने मानस की रचना करके समय के झूठे वेदान्तियों को अपनी भक्ति के बहाव से पाखंड फैलाने से रोका और ज्ञान तथा भक्ति के बीच में एकता स्थापित की।
रामचरितमानस की कथा आज जनता के जीवन की अपनी कथा है। काव्य में उसका तारतम्य कहीं टूटने नहीं पाया। व्यर्थ का चित्रण जैसा जायसी के पद्मावत में मिलता है उसका मानस में अभाव है। जिस बात को मानस में कवि ने कहना चाहा है उसका आभास हमें पहले से ही मिलना आरंभ हो जाता है। इसलिए वह सामने जब आती तो भार-स्वरूप नहीं मालूम देती। ग्रंथ में जहाँ-जहाँ भी दुष्ट पात्रों का समावेश हुआ है वहाँ वहाँ उस पर कवि अपना कोप प्रकट करने में नहीं चूके हैं। ब्राह्मणों की महिमा का कवि ने गान किया है। स्त्री की निंदा की हैं, परंतु प्रमदा के रूप में नारी अथवा अन्य किसी रूप में नहीं। यदि हम महाकाव्य की एक पंक्ति को काव्य से बाहर निकालकर विचार करना आरंभ कर देते हैं तो वह कवि के साथ अन्याय होता है। क्योंकि हमें उस पंक्ति का अर्थ उसी स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ जिस पात्र के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। यदि तुलसी ने “ढोर गँवार शूद्र पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी” लिख भी दिया है तब भी सीता का चरित्र चित्रण क्या संसार की माता के रूप में उन्होंने नहीं किया?
काव्य की दृष्टि से मानस एक अनुपम काव्य है। इसमें अच्छे काव्य के सभी गुण विद्यमान हैं। प्रायः नौ के नौ रस इस ग्रंथ में कहीं न कहीं पर मिलते हैं और यदि अलंकारों को खोजकर निकालने का प्रयत्न किया जाए तो वह भी एक रीतिकालीन ग्रंथ की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं। अर्थालंकार के साथ-साथ अनुप्रासों पर कवि ने विशेष बल दिया है। ग्रंथ दोहा और चौपाई में लिखा गया है। तुलसीदास जी ने यों तो सभी रसों में रचना की है परंतु इनका विशेष रस शांत ही रहा है। जायसी की भाँति मानस की भाषा भी कवि ने अवधी ही चुनी है। शास्त्र-पारंगत विद्वान् होने के कारण गोस्वामी जी की शब्द-योजना साहित्यिक और संस्कृत-गर्भित है।
कथा-काव्य या प्रबंध-काव्य के भीतर इतिवृत्ति वस्तु व्यापार-वर्णन, भाव-व्यंजना और सवाद, ये अवयव होते हैं। अयोध्यापुरी की बाल लीला, नख-शिख जनक-वाटिका के वर्णन कहीं पर भी कवि ने इतिवृत्ति की शृंखला को टूटने नहीं दिया है। जिस मर्यादा का पालन कवि ने रामचरित रचने में किया है काव्य रचना में भी उसे भुलाया नहीं है। न कहीं आवश्यकता से अधिक वर्णन है और न कहीं आवश्यकता से कम। मानस में कवि ने प्रसंगों के अनुकूल भाषा और रसों के अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया है। समाज और परिस्थिति के अनुसार ही संस्कृत-गर्भित हिंदी और ठेठ ग्रामीण भाषा का प्रयोग काव्य में किया गया है। घरेलू प्रसंग होने के कारण कैकेयी और मंथरा के संवाद ठेठ बोली में हैं। काव्य में शृंगार का लोप नहीं है, परंतु मर्यादा के साथ उसे कवि ने कुशलतापूर्वक निभाया है।
इस प्रकार मानस पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने मानस की रचना केवल अपने दृष्टिकोण से नहीं की वरन् समस्त संसार पर दृष्टि फैलाकर की है। इसमें जीवन के मार्मिक चित्रण हैं, प्रकृति का असीम सौंदर्य है, दर्शन की पैनी साधना है, काव्य का अलौकिक सौंदर्य है, भक्ति की मर्यादा है, हिंदू मात्र के सब धर्मों का समन्वय है, मानव जीवन की एकता का महान् आदेश है, और सबसे सुंदर है शांत रस का अथाह सागर जिसमें डुबकियाँ लगाकर मानव अपने जीवन की, अपने हृदय की और अपने शरीर की जलन को सर्वदा के लिए बुझा सकता है। मानस को पढ़कर हृदय और मन को शांति मिलती है और यह भूले-भटके जीवन-राही का पथ निर्देशन करता है। मानस की रचना करके कवि ने केवल हिंदी भाषा भाषियों का ही नहीं वरन् मानव समाज का महान हित किया है।