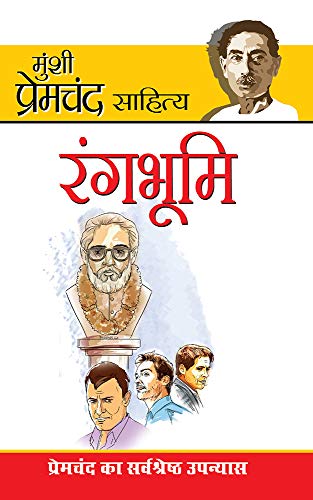रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का चौथा उपन्यास है। इस उपन्यास में भारत के अंदर कल-कारखानों का उदय और ग्रामीण उद्योगों का पतन दिखलाया है। शहर और ग्रामों की यह समस्या उस समय पश्चिमीय देशों में समाप्त हो चुकी थी और पूर्वी देशों में चल रही थी। कारखानों के प्रताप से ग्राम शहर में परिवर्तित होते जा रहे थे और उसी के विपरीत विद्रोह की भावना को लेकर उपन्यास कार ने रंगभूमि की रचना की है। इसी समय भारत में गांधी जी अपनी चर्खा-प्रणाली का प्रचार कर रहे थे। इस चर्खे के प्रचार के साथ-साथ चल रहा था महात्मा गाँधी का असहयोग आंदोलन। यही कारण था कि यह गांधी जी की चर्खा विषयक प्रस्तावना संपत्ति-शास्त्र-वेत्ताओं को उतना आकृष्ट न कर सकी और देहातों में करघे इत्यादि की योजनाएँ अधिक प्रस्फुटित नहीं हो सकीं। भारत के देहाती बराबर कल-कारखानों के चक्कर में फँसते रहे। सरकार ने समाज को सहयोग नहीं दिया और न ही देहाती उद्योग-धंधों को जिसका स्पष्ट फल यह हुआ कि देहातों में जो बचे-खुचे देहाती धंधे थे वह भी समाप्त होने लगे और कलों का प्रचार भारत में बढ़ने लगा। अंग्रेजी कारखानों में बनी हुई कलों को बेचने के लिए भारत का बाजार खुल गया और भारत का रुपया विदेश को जाने लगा। रंगभूमि सरकार की इस नीति के विरुद्ध उस काल में एक खुला हुआ विद्रोह था। साथ ही साथ भारत की राजनीति को यह एक सुझाव भी था।
रंगभूमि के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के विषय में कालीदास कपूर एम० ए० लिखते हैं-“विनय और सोफ़ी के चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक हैं। मनुष्य और स्त्री की प्रेम भावना में क्या अंतर है? क्या यह सत्य है कि मनुष्य का प्रेमोपासना-मार्ग आदर्श प्रेम के आकाश से लालसा के पाताल तक है और स्त्री का उससे उलटा, लालसा के पाताल से आदर्श प्रेम के आकाश तक। यदि ऐसा हो तो चरित्र-चित्रण में स्वाभाविकता का अंश अवश्य है। विनय में जो कुछ देश सेवा का अंकुर है वह उसकी माता जाह्नवी की कृपा से। सोफ़ी के प्रेम-पाश में फँस-कर उसमें अधर्मता आ जाती है। विनय आदर्श प्रेम से गिरकर इंद्रिय भोग की लालसा में अपनी आत्मा को हानि पहुँचाता है। सोफ़ी का दूसरा ही हाल है। वह आदर्शवादिनी है। यों तो वह अबला है परंतु विनय के प्रति अंकुरित प्रेम उसे कर्मवीरागंना बना देता है। उपन्यास के दूसरे भाग में उसी का राज्य है।
प्रेमचंद जी ने भारतीय स्त्रीत्व तथा मनुष्यत्व का वास्तविक चित्र खींचा है। मनुष्य लालसा और लोभ के वश तो कर्मण्य रहते हैं परंतु आदर्श उन्हें अकर्मण्य और आलसी कर देता है। स्त्रियाँ भी लालसा और लोभ के पाश में फँस जाती हैं; पर अपना धर्म नहीं खोतीं।
प्रेमचंद जी देहाती जीवन का करुणामय चित्र खींचने में दक्ष हैं। सेवा-सदन प्रेमाश्रम और रंगभूमि में प्रेमचंद का प्रेम शहर से देहात की ओर अधिक है। ‘प्रेमाश्रम’ में प्रेमचंद जी ने ‘सेवासदन’ की भाँति एक आदर्श ग्राम की सृष्टि की है। पर साथ ही वास्तविक लखनपुर की भी पूरी व्याख्या की है। ‘रंगभूमि, का पांडेपुर ‘प्रेमाश्रम’ का लखनपुर है। ‘रंगभूमि’ में वह हृदय-विदारक दृश्य है कि कल और कारखाने किस प्रकार इस ग्राम का विनाश करते हैं और उसके साथ ही अधर्म का प्रचार बढ़ाते हैं। इसकी सूरदास ने कारखाने बनने की प्रस्तावना पर पहले से ही सूचना दे दी थी। “सरकार बहुत ठीक कहते हैं। मुहल्ले की रौनक जरूर बढ़ जाएगी, रोजगारी लोगों को फ़ायदा भी खूब होगा। लेकिन जहाँ यह रौनक बढ़ेगी, वहाँ ताड़ी-शराब का भी तो प्रचार बढ़ जाएगा, कसाबियाँ भी तो आकर बस जाएँगे। परदेशी आदमी हमारी बहू-बेटियों को घूरेंगे, कितना अधर्म होगा? देहात के किसान अपना काम छोड़कर नौकरी के लालच से दौड़ेंगे, यहाँ बुरी बुरी बातें सीखेंगे और अपने बुरे आचरण अपने गाँवों में फैलाएँगे। देहातों की लड़कियाँ बहुएँ मजूरी करने आयँगी और यहाँ पैसे के लोभ में अपना धर्म बिगाड़ेंगी। यही रौनक शहरों में है, यही रौनक यहाँ हो जाएगी। बजरंगी और जगधर के मकान मिट गए, सूरदास को झोंपड़ी के लिए सत्याग्रह करना पड़ा। परंतु यह दृश्य उतने कष्टमय नहीं हैं जितना कि वह जिसमें देहात के नवयुवक घीसू और विद्याधर का नैतिक पतन होता है। ठीक ही है धन का देवता बिना आत्मा का बलिदान पाए प्रसन्न नहीं होता।” इस उपन्यास पर देहात के जीवन का साम्राज्य है। नायक और नायिकाएँ शहर के हैं, पर वे देहात पर अपनी जीविका के लिए निर्भर हैं। ‘रंगभूमि’ में देहाती जीवन के विनाश का करुणामय दृश्य है। क्षेत्र काशी से उदयपुर तक है। उपन्यास के पात्र देशी और विदेशी, देहाती और शहर के हैं— गाँव का नायक सूरदास है और उसके ही चरित्र में देहात के जीवन का चरित्र है देहातियों की सरलता, धर्म-भीरुता, साहस, सहन-शक्ति, प्रकृति, घरेलू झगड़े, संगठन-शक्ति इन सबका प्रतिबिंब सूरदास में मिलता है।
‘सेवासदन’ में देहात के उदय, ‘प्रेमाश्रम’ में उसके मध्याह्न और रंगभूमि में उसके अस्त होने का दृश्य है। प्रथम उपन्यास में आशा, दूसरे में आशा और निराशा, दोनों का मेल, और तीसरे में अंधकार और निराशा, रंग-भूमि में करुणा की पराकाष्ठा है। इस उपन्यास का हास्य भी करुणा से घिरा हुआ है। प्रेमचंद जी के चरित्र चित्रण में एक दोष है, जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। आपको जब पात्रों की आवश्यकता नहीं रहती, जब उसमें रंग भरते-भरते आप थक जाते हैं, तब झट उनका गला घोंट डालते हैं। ‘सेवासदन’ में कृष्णचंद नदी में डूबकर आत्महत्या करता है, ‘प्रेमाश्रम’ में गायत्री पहाड़ से गिरकर जान देती है और रंगभूमि में विनय पिस्तौल द्वारा अपनी हत्या करता है।
हमें यह ढंग दोषपूर्ण मालूम होता है। आत्महत्या की नीति तथा धर्म-शास्त्र दोनों में निषेध है और धर्म और नीति दोनों की अवहेलना करना न कवि के लिए योग्य है और न उपन्यास लेखक के लिए। उपन्यास लेखक को भी कवि की भाँति अपनी कला में निरंकुशता का अधिकार प्राप्त है, परंतु इतना नहीं कि जिस कर्म का शास्त्र तथा नीति में निषेध हो उसका लेखक द्वारा सम्मान किया जाए।
इतना सब कुछ होते हुए भी प्रेमचंद के उपन्यासों का महत्त्व कम नहीं होता, प्रेमचंद जी जोशी की प्रेमचंद के प्रति आलोचनाओं से सहमत नहीं हैं। यह उपन्यास क्षणभंगुर नहीं है। हिंदी के दुर्भाग्य से इनका अनुवाद, अभी तक किसी पाश्चात्य भाषा में नहीं हुआ है। यदि कभी हो, और यूरोप के विद्वान् प्रेमचंद की रवींद्रनाथ ठाकुर और टाल्स्टाय से तुलना करें तब हम भी समझने लगेंगे कि ये उपन्यास भी कुछ महत्त्व रखते हैं। प्रेमचंद का यथासमय भारतीय साहित्य में वही सम्मान होगा जो डिकेंस और टॉलस्टाय को यूरोपीय साहित्य में प्राप्त है। भारत का हृदय कलकत्ते की गलियों में नहीं है, न वह शिक्षित बंगाल की अट्टालिकाओं में है। उनका हृदय देहात में है, किसान के टूटे-फूटे झोंपड़ों में है। हरे-भरे खेतों को देखकर उसे शांति मिलती है। अनावृष्टि से अन्न सूख जाता है। उस दृश्य का मार्मिक चित्र जिसने खींचा है वह देश भर का धन्यवाद-पात्र है। अभी भारतीय किसानों में शिक्षा का अभाव है। जिस समय यह समझेंगे कि कोई साहित्यिक ऐसा भी हुआ था कि जिसने उस समय अपने जीवन की अनुभूतियों को हमारी झोंपड़ियों में लाकर बिठलाया था और हमारा उस समय का चित्रांकन करके आनंद लाभ लिया था, जब देहाती असभ्य समझे जाते थे, तो वह काल प्रेमचंद के विकास का काल होगा, तब उनके उपन्यासों के पात्र भारत के भाग्य विधाता बनकर अपने पूर्वजों को सम्मान के उच्चतम आसन पर बिठलाकर उसकी पूजा करेंगे।