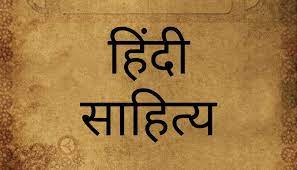रीति काल में हिंदी काव्य की रचना मुख्य रूप से शृंगार रस को लेकर ही हुई है। इस युग के कवियों ने कृष्ण-भक्ति का सहारा लेकर श्रीकृष्ण का राधा तथा अन्य गोपियों से प्रेम संबंध दिखाया है। उन्होंने अपने काव्य की रचना मुक्तक काव्य के रूप में की है। राधा कृष्ण प्रेम को लेकर जितना साहित्य इस युग में लिखा गया उतना इससे पूर्व कभी नहीं लिखा गया था। श्रीकृष्ण की बाल लीला की इस काव्य में पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई है, किंतु विनय- भाव से युक्त शुद्ध भक्ति के छंद कहीं कहीं उपलब्ध हो जाते हैं। आये हम इस युग के कवियों और उनके काव्य की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे।
(1) कविवर केशवदास –
केशव ने अपने काव्य में अलंकारों को प्रमुख स्थान दिया है। उन्होंने राम- भक्ति और कृष्ण भक्ति दोनों की ओर समान ध्यान दिया है। उनकी रचनाओं में ‘रामचन्द्रिका’, ‘कविप्रिया’ और ‘रसिकप्रिया’ सब से मुख्य हैं। ‘रामचन्द्रिका’ महाकाव्य है और शेष दोनों रचनाएँ मुक्तक रूप में लिखी गई हैं। स्वतंत्र मुक्तक काव्य लिखने के अतिरिक्त उन्होंने ‘कविप्रिया’ और ‘रसिकप्रिया’ में अलंकारों और रसों आदि के उदाहरण देने के लिए भी कविताएँ लिखी है, किंतु प्रायः ऐसे छंद काव्य-कला की दृष्टि से अधिक सुंदर नहीं बन सके है। उनके काव्य में शृंगार रस को मुख्य स्थान प्राप्त हुआ किंतु उन्होंने अन्य रसों को भी अपने काव्य में पर्याप्त स्थान दिया है।
(2) कविवर चिंतामणि-
चिंतामणि ने काव्य की रचना करने के अतिरिक्त प्राचार्य के रूप में भी अपनी प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया है। उन्होंने भी काव्य के विभिन्न अंगों के उदाहरण उपस्थित करने के लिए काव्य-रचना की है। उनके काव्य में शृंगार रस को मुख्य स्थान प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि उन्होंने अपने काव्य में श्रीकृष्ण की प्रेम-लीलाओं के अनेक सूक्ष्म तथा स्थूल चित्र उपस्थित किए हैं। उन्होंने अपने काव्य की रचना मधुर ब्रजभाषा में की है।
(3) महाकवि बिहारीलाल –
बिहारी सौंदर्यवादी कवि थे। उन्होंने ‘बिहारी सतसई’ नामक ग्रंथ की रचना की है। हिंदी के सतसई – काव्यों में इस कृति का सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसमें शृंगार रस को मुख्य स्थान दिया गया है और उसके संयोग तथा वियोग के चित्रों को अनेक रूपों में उपस्थित किया गया है। इसमें कवि ने नायिका भेद के अनुसार नायिका की विभिन्न स्थितियों का उल्लेख किया है। इसमें भावो का सूक्ष्म रूप से प्रतिपादन किया गया है। यह शृंगार रस की सर्वश्रेष्ठ रचना है, किंतु इसमें नीति और भक्ति के अनेक दोहों के कारण शांत रस का भी सुंदर समावेश हुआ है। बिहारी ने दोहे के समान छोटे छंद में व्यापक भावों का समावेश कर अपनी प्रतिभा का प्रशंसनीय परिचय दिया है। भाव पक्ष की भांति उनके काव्य का कला पक्ष भी अत्यंत श्रेष्ठ बन पड़ा है। आगे हम उनका प्रकृति वर्णन संबंधी एक सुंदर दोहा उद्धृत करते हैं-
“छकि रसाल सौरभ सने, मधुर माधुरी गंध।
ठौर-ठौर भरत झेंपत, भर-भर मधु अंध॥”
(4) कविवर मतिराम –
मतिराम ने कवि के अतिरिक्त आचार्य के रूप में भी साहित्य सेवा की हैं। उन्होंने शृंगार रस को लेकर सरस काव्य की रचना की है। उनकी ‘सतसई’ में शृंगार रस के दोहों के अतिरिक्त भक्ति और नीति संबंधी दोहों का भी अच्छा संग्रह हुआ है। शृंगार रस के अंतर्गत उन्होंने जहाँ सयोग शृंगार के छविपूर्ण चित्र उपस्थित किए है वहाँ विरह का भी उपयुक्त चित्रण किया है। उनके काव्य में भावना और कला, दोनों ही की दृष्टि से स्वाभाविकता की ओर पूरा ध्यान दिया गया है।
(5) महाकवि देव —
देव ने भी कवि और आचार्य, दोनों के रूप में अपनी कुशलता दिखाई है। उन्होंने शृंगार रस को लेकर अनेक सरस कवित्तों की रचना की है। उनकी कविताओं में मौलिकता को पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने काव्य में कल्पना को भी पर्याप्त स्थान प्रदान किया है। यह कल्पना कहीं स्पष्ट और कहीं अस्पष्ट रूप में प्राप्त होती है। उन्होंने शृंगार रस के अनेक स्वच्छ चित्र उपस्थित किए हैं। उनके काव्य की बिहारी के काव्य से प्रायः तुलना की जाती है। मिश्रबन्धु, पंडित कृष्णबिहारी मिश्र और डॉ. नगेन्द्र ने उनके काव्य की विशेष रूप से प्रशंसा की है।
(6) कविवर पद्माकर –
पद्माकर ने भी कवि और आचार्य, दोनों के रूप में काव्य-साधना की है। उनकी कविताओं में कृत्रिमता का स्पष्ट अभाव रहा है। उन्होंने अपने भावों को स्वाभाविक रूप में उपस्थित किया है और यथास्थान कल्पना का भी उपयोग किया है। भावों के अनुसार उनकी भाषा भी अनेक रूपों में बदलती रही है। इसी कारण कहीं वह कोमल रूप में प्राप्त होती है और कहीं उसमें ओज का समावेश हो गया है।
(7) महाकवि घनानंद –
घनानंद ने अपने काव्य में प्रेम की सुंदर व्यंजना उपस्थित की है। उन्होंने प्रेम की गंभीरता का अच्छा उद्घाटन किया है। उनके काव्य का संबंध भी कृष्ण की प्रेम-लीलाओं से ही रहा है। शृंगार रस के अंतर्गत उन्होंने संयोग शृंगार की अपेक्षा वियोग शृंगार का अधिक मार्मिक वर्णन किया है। रीति काल के कवियों में उनकी भाषा सबसे अधिक मधुर तथा स्वच्छ रही है। वैसे भी भाषा की दृष्टि से ब्रजभाषा के कवियों में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है।
इन प्रमुख कवियों के अतिरिक्त रीति काल में सेनापति, भिखारीदास, रसलीन, प्रताप सिंह, ग्वाल और बेनी प्रवीण ने भी अच्छे काव्य की रचना की है।
सामान्य विश्लेषण
रीति काल के काव्य का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें शृंगार रस के विभिन्न अंगों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। उसमें प्रेम की गंभीरता के स्थान पर रसिक कृष्ण के चंचल प्रेम-भावों को अधिक स्थान प्राप्त हुआ है। कृष्ण का यह रूप रीति काल से पूर्व भक्ति काल के राधावल्लभी संप्रदाय के कवियों की रचनाओं में प्रवेश पा चुका था। अतः इसके लिए केवल रीतिकालीन कवियों की ही निंदा उचित नहीं है। आधुनिक युग के अनेक आलोचकों ने शृंगार रस की अधिकता और उसके स्थूल चित्र उपस्थित करने के कारण रीति काल के शृंगार-काव्य का विरोध किया है। इस स्थान पर यह ध्यान रखना चाहिए कि इस युग में केवल शृंगार रस के स्थूल चित्र ही नहीं मिलते, अपितु कुछ कवियों ने उसे सूक्ष्म रूप में भी उपस्थित किया है। इन कवियों में बिहारी और देव के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने काव्य में नायिका के रूप के ऐसे अनेक उज्ज्वल और प्रभावशाली चित्र उपस्थित किए हैं जिनकी किसी भी अवस्था में उपेक्षा नहीं की जा सकती। शृंगार रस के प्रेम-भाव को मानव-जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अतः केवल उसका चित्रण करने के कारण ही किसी व्यक्ति के साहित्य की निंदा नहीं की जा सकती। रीति काल के कवियों की भूल यह है कि उन्होंने इस प्रेम भाव का सर्वत्र श्रीकृष्ण की प्रेम- लीलाओं से संबंध दिखाया है। यदि इसके स्थान पर उन्होंने शृंगार रस का स्वतंत्र चित्रण किया होता और उसमें भक्ति को मिलाने का प्रयत्न न किया होता तो उन्हें अधिक सफलता मिलती।
इस स्थान पर यह भी उल्लेखनीय है कि रीति काल में शृंगार-काव्य के अतिरिक्त वीर-काव्य और नीति काव्य की भी रचना की गई थी। वीर-काव्य की रचना करने वाले कवियों में भूषण लाल और सूदन प्रमुख है। इनमें भी भूषण का स्थान सब से मुख्य है। उन्होंने कवि-कर्म के साथ-साथ आचार्यत्व का भी निर्वाह किया है। अपनी ‘शिवराजभूषण’ शीर्षक रचना में उन्होंने आचार्यत्व और कवित्व का साथ-साथ समावेश किया है। यह एक अलंकार ग्रंथ है और इसमें शिवाजी के महत्त्व को स्पष्ट करने वाले – छंदों को अलंकारों के उदाहरणों के रूप में उपस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके ‘शिवाबावनी’ और ‘छत्रसाल – दशक’ नामक दो अन्य काव्य ग्रंथ भी उपलब्ध होते हैं। इनमें क्रमश: महाराज शिवाजी और महाराज छत्रसाल के शौर्य का ओजस्वी वर्णन किया गया है।
नीति काव्य की रचना करने वाले कवियों में कविवर वृंद का नाम उल्लेखनीय है। उनके अतिरिक्त बिहारी और मतिराम आदि अन्य कवियों ने भी नीति-विषयक कुछ स्फुट छंदों की रचना की है। वृंद कवि ने अपनी ‘वृंद- सतसई’ में केवल नीति-विषयक विचारधारा का ही समावेश किया है। हिंदी में नीति-काव्य की रचना करने वाले कवियों में उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने काव्य की रचना दोहा छंद में ब्रजभाषा में की है। नीति के समावेश की दृष्टि से उनके अधिकांश छंद मार्मिक तथा श्रेष्ठ बन पड़े हैं।