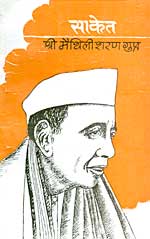‘साकेत’ बाबू मैथिलीशरण गुप्त का वह अमर काव्य है कि जिसमें उन्होंने एक ऐसे पात्र का चरित्र चित्रण किया है जिसके प्रति आज तक हिंदी साहित्य सर्वदा ही उदासीन रहा। यों ‘साकेत’ में रामायण की पूरी ही कथा आ जाती है परंतु उर्मिला का चित्रण कवि ने पूरे दो सर्गों में किया है। अयोध्या में प्रधानतया होने वाली घटनाओं को ही इस काव्य में महत्त्व दिया गया है इसीलिए इस ग्रंथ का नाम कवि ने ‘साकेत’ रखा है। राम के राज्याभिषेक से लेकर चित्रकूट में राम-भरत मिलन तक की कथा आठ सर्गों में चलती है। फिर नौ और दस सर्ग में उर्मिला के वियोग का नाना परिस्थितियों में कवि ने चित्रण किया है। कवि ने उर्मिला की अंतवृत्तियों का विस्तार के साथ वर्णन किया है।
‘साकेत’ प्रबंध-काव्य है परंतु यह कवि ने उस समय लिखना प्रारंभ किया था जब उनकी प्रवृत्ति गीत-काव्य की तरफ हो चली थी। मुक्तक कविताएँ गीतों के रूप में हिंदी साहित्य के अंदर प्रविष्ट हो चुकी थीं और कवि-वर मैथिलीशरण जी भी उस धारा के प्रवाह से अपने को न बचा सके। गीतों के इसी बहाव के कारण कवि के ‘साकेत’ में वैसी प्रबन्धात्मकता नहीं आ पाई जैसी कि इस ग्रंथ के लिए आवश्यक थी।
‘साकेत’ में उर्मिला का विरह-वर्णन एक विशेष चीज है, जिसमें कवि ने पुरानी पद्धति के आलंकारिक-चमत्कार के साथ सजीव वर्णन किया है। आज की गीतात्मकता, नवीन वेदना और लाक्षणिक-वैचित्र्य वाली कविताओं ने साकेत की कविता में प्राण फूँक दिए हैं। ‘साकेत’ की उर्मिला विरह में पागल होकर भी आदर्श और कर्त्तव्य को नहीं भुलाती। जब स्वप्न में उसे लक्ष्मण सामने खड़े दिखाई देते हैं तो वह प्रसन्न नहीं होती, बल्कि कह उठती है-
“प्रभु नहीं फिरे, क्या तुम्हीं फिरे?
हम गिरे, अहो ! तो गिरे, गिरे !”
दंडकारण्य से लेकर लंका तक की घटनाएँ शत्रुघ्न के मुँह से मांडवी और भरत के सम्मुख वर्णन कराई गई हैं। यह कथा बहुत रसात्मक और रोचकता के साथ कही गई है। कवि ने हिंदी काव्य में रामायण के पात्रों में चरित्रों का जो आदर्श पुराने समय मिलता है उसे निभाने और उसी में आधुनिकता का पुट देने का सफल प्रयत्न किया है। किसानों और श्रमजीवियों के साथ सहानुभूति, राज्य की व्यवस्था में प्रजा का हाथ, सत्याग्रह, मानवता के अटल सिद्धांतों के अनुसार विश्वबंधुत्व इत्यादि पर कवि ने प्रकाश डाला है। कवि ने ग्रंथ में आधुनिकता लाने का भरसक प्रयत्न किया है।
समय और काल के अनुसार उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं के साथ प्रणालियों को ग्रहण करते हुए चलना मैथिलीशरण की विशेषता है। इसीलिए साकेत का लेखक इस काल का प्रतिनिधि कवि कहलाया है। साकेत में कवि ने बहुत साफ और सुथरी भाषा का प्रयोग किया है। भाषा में माधुर्यं लाने के लिए कवि ने बंगभाषा के कवियों का अनुसरण किया है। “साकेत गुप्त जी की सामंजस्यवादी रचना है, मद में झूमने वाली रचना नहीं।” इस काव्य में सभी प्रकार की उच्चता प्राप्त होती है। सरसता, सरलता और माधुर्य की त्रिवेणी के संगम पर इस ग्रंथ को सृष्टि हुई है और यही कारण है कि इसकी प्रत्येक पंक्ति से रस टपकता है। जिस समय चित्रकूट पर सीता जी बहाने से लक्ष्मण को उर्मिला के पास झोंपड़ी में भेज देती हैं और लक्ष्मण सहमकर लौटने लगता है तो कवि ने उर्मिला के मुँह से कितने सुंदर शब्दों में प्रेम रस प्रवाहित कराया है-
“मेरे उपवन के हरिण, आज बनचारी।
मैं बांध न लूंगी तुम्हें, तजो भय भारी॥”
‘साकेत’ के लक्ष्मण और सीता ‘रामचरितमानस’ के लक्ष्मण और सीता नहीं हैं। जिस मर्यादा का पालन कवि तुलसीदास ने किया है वह बंधन गुप्त जी ने ढीले कर दिए। ‘साकेत’ के पात्र आज के पात्र हैं, जिनमें सीता भाभी है और लक्ष्मण उसका देवर, फिर क्यों न उनमें कहीं न कहीं हास्य का, उपहास का और व्यंग्य का पुट आ जाए? कवि ने कवि-कल्पना के आधार पर भाभी और देवर का बहुत सुंदर चित्रण किया है। इस चित्रण में भारतीय आदर्श-वाद को भी हाथ से नहीं जाने दिया है और वर्तमान सामाजिक दृष्टि में भी लाकर कवि ने अपने काव्य के पात्रों को खड़ा कर दिया है। ‘साकेत’ को पढ़-कर हम केवल कल्पनाओं और आदर्शवाद में ही नहीं घूमते वरन् दुनिया के महान् चरित्रों की कलात्मक कल्पना भी करते हैं।
‘साकेत’ का नायक हम राम को न मानकर लक्ष्मण को मान सकते हैं; क्योंकि इस ग्रंथ में प्रधान चित्रण लक्ष्मण और उर्मिला का ही है। परंतु लक्ष्मण के चरित्र का विकास राम के ही साथ हो सकता है इसलिए राम के महत्त्व को भी कम नहीं किया जा सकता। लक्ष्मण की सेवा-भावना और त्याग का कवि ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। ‘साकेत’ की कैकेयी ‘मानस’ की कैकेयी से भिन्न है। ‘साकेत’ की कैकेयी को अपनी भूल ज्ञात होने पर बहुत खेद होता है। ‘साकेत’ अपने ढंग का अकेला महाकाव्य है। इसमें स्थान-स्थान पर गीत और छंदों की अनेकरूपता होते हुए भी प्रबन्धात्मकता को कवि ने खूब निभाया है। घटनाओं का तारतम्य ‘साकेत’ में कवि ने बहुत सुंदर दिया है।
खड़ीबोली साहित्य का यह प्रथम महाकाव्य है जिसमें हम राम-भक्ति-शाखा की वर्तमान प्रगति के दर्शन करते हैं। इसमें खड़ीबोली का मँजा हुआ स्वरूप है जिसमें माधुर्य के साथ-साथ अलंकारशास्त्र की भी पूरी निपुणता प्राप्त होती है। कवि ने इस काव्य में अपनी कला, पांडित्य और भावुकता का सुंदर सम्मेलन प्रस्तुत किया है। यह इस युग की वह अनुपम देन है जो हिंदी साहित्य से एक अमर रचना बनकर आई है और ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता जाएगा, हिंदी के पाठकों में इसकी सर्वप्रियता बढ़ती ही जायगी। बाबू मैथिलीशरण गुप्त की यह वह प्रतिनिधि रचना है जिसके आधार पर एक कवि को पूर्ण रूप से समझा जा सकता है।