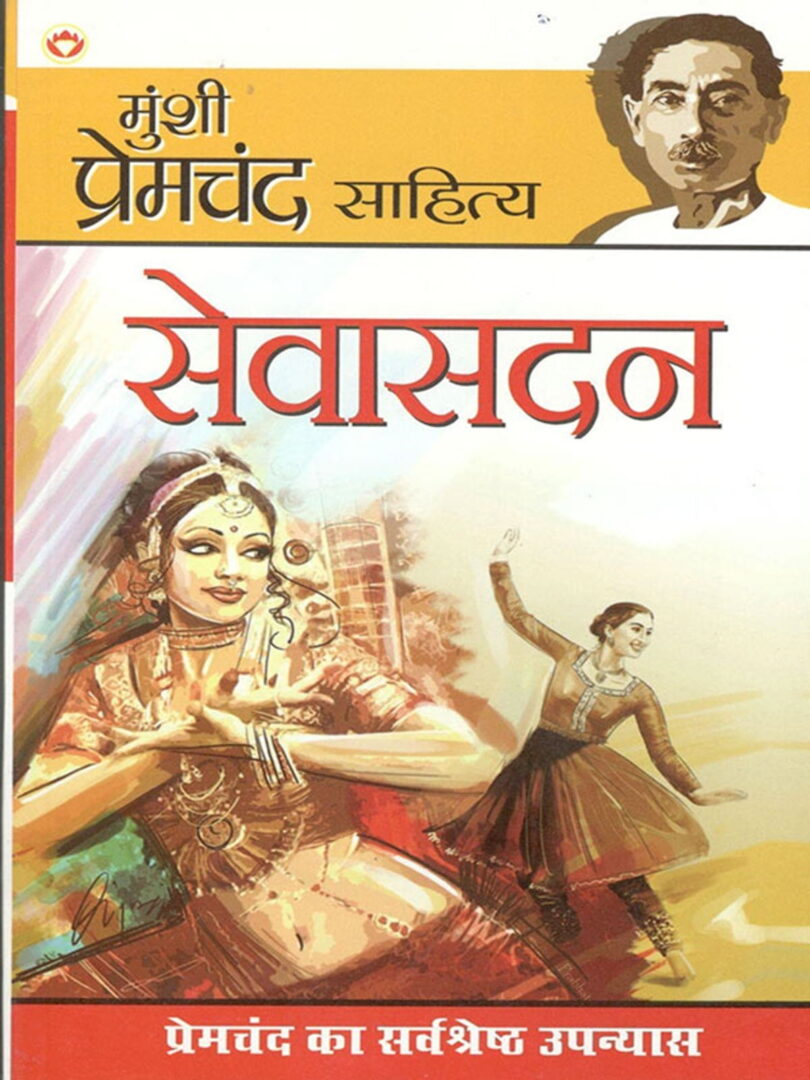‘सेवासदन’ मुंशी प्रेमचंद जी के प्रारंभिक उपन्यासों में से है। इसमें एक वेश्या का चरित्र चित्रण उपन्यासकार ने कलात्मक ढंग से किया है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में समाज सुधार पर विशेष बल दिया है। अपने इसी आदर्श को सम्मुख रखते हुए लेखक ने इस उपन्यास का भी निर्माण किया है। उपन्यास में चरित्रों का चित्रण लेखक ने विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के साथ किया है और ऐसे सुंदर चरित्र पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं कि वह वास्तविक-से ही जान पड़ते हैं। वेश्याओं के बाजार में लेखक अपने पाठकों को ले जाता अवश्य है परंतु उनकी भावनाओं को इतना संतुलित करके रखता है कि कलुषित होने की हवा तक भी नहीं लगने देता। पाठक के सामने पद्मसिंह या विट्ठलदास ही रहते हैं। सदन या भोली के प्रति पाठक के मन में सहानुभूति नहीं उत्पन्न होने पाती। कालिदास कपूर लिखते हैं-
“वारवनिताओं का आदर होने से गृहस्थाश्रम का अधःपतन होता है। ‘सेवासदन’ में कही गई कहानी के द्वारा उनके उद्धार की रीति बताई गई है। इस उपन्यास का प्रधान उद्देश्य यही है। परंतु इसके प्रत्येक पात्र के चरित्र से एक न एक शिक्षा मिलती है। कृष्णचंद्र सच्चे हैं, परंतु उन्हें अपने सत्य को देश की दहेज प्रथा-रूपणी भीषण दुर्देवी के चरणों में बलिदान करना पड़ता है। अपनी दुलारी और शिक्षिता लड़की के विवाह के लिए दहेज की रकम जुटाने को वह रिश्वत लेते हैं, पकड़े जाते हैं, कैद भुगतते हैं। घर मटियामेट हो जाता है। एक लड़की निर्धन वर के गले मढ़ी जाती है, दूसरी दासी होकर अपना समय काटती है, इसी मानसिक क्लेश का शिकार बनकर बहुत शीघ्र संसार से कूच कर जाती है। इस अग्नि परीक्षा में हरिश्चंद्र ही का सत्य टिक सकता था। जेल से लौटने पर कृष्णचंद्र के चरित्र का अच्छी तरह पतन हो गया है। लेखक महोदय बहुत देर तक उनको हमारे सामने नहीं रहने देते। विपत्ति-सागर में दो-चार और गोते लगाकर वह हमारी दृष्टि से लुप्त हो जाते हैं।”
कृष्णचंद का-सा शोकमय अंत और किसी का नहीं हुआ। बाकी चरित्रों के चित्रण में कहीं आनंद है, कहीं शोक और कहीं विप्लव परंतु अंत शांति-पूर्ण है। इन चरित्रों में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य चरित्र सुमन का है।
अत्युक्ति न समझिए, सुमन ही के चरित्र चित्रण में उपन्यास का गौरव है। उसी में उपन्यास के प्राण हैं। सुमन के चरित्र में यदि कहीं भी बट्टा लग जाता तो उपन्यास किसी काम का न रहता। लेखक महाशय उसे पढ़ा-लिखा कर, और शारीरिक सुख का शौकीन बनाकर, पंद्रह रुपये महीने पर नौकर एक अधेड़ ब्राह्मण से ब्याह देते हैं ! चरित्र चित्रण में सुमन को एक बात ने बचा लिया है कि वह भारतीय नारी है, पतिव्रता है सही, परंतु आत्म गौरव और शारीरिक सुख की लालसा उसको वह व्रत निबाहने नहीं देती। इधर वह देखती है कि समाज में पतिव्रता की कोई कदर नहीं। घर के सामने ही यह देखती है कि पतिता भोली का आदर-सम्मान बड़े-बड़े धर्मज्ञ करते हैं पर उसके लिए इतना भी नहीं कि वह अपनी मर्यादा को एक नीच सिपाही के हाथ से भी बचा सके। पति महाशय (गिरजाधर जी) क्या करें? पत्नी के वस्त्राभूषण और मान-प्राप्ति की लालसा को वह कुछ और ही समझे। एक दिन आग लग ही गई, सुमन तो गृहिणी के उच्च पद से गिर गई।
परंतु अभी कुछ और पतन होना बाकी है। दूसरे दृश्य में उसे हम दाल-मंडी के एक कोठे पर देखते हैं। यदि लेखक महाशय जरा भी चूक जाते तो सुमन के पतन की पराकाष्ठा हो जाती। मदनसिंह के प्रेम-पाश में सुमन फँस जाती है, परंतु पतित नहीं होने पाती। इसके पहले ही समाज-सुधारक विट्ठल दास उसके उद्धार के लिए पहुँच जाते हैं पर उसका उद्धार नहीं होता। विधवा-आश्रम में उसको बहुत शीघ्र लाया जाना, समाज की कृपा से उसके उद्धार-विरुद्ध कठिनाइयों का पड़ना, शांता की विपत्ति, उसके भावी श्वसुर मदनसिंह का विरोध-इसमें से किसी एक का भी काम कर जाना सुमन को गिरा देने के लिए काफी था। परंतु लेखक उसको हर तरफ से बचाकर अंत में ‘सेवासदन’ की संचालिका का पद तक देते हैं। सुमन ने अपने ही को नहीं उपन्यास को भी गिर जाने से बचा लिया।
स्त्री-पात्र में यदि प्रधान चरित्र सुमन का है तो पुरुष पात्रों में पद्मसिंह का लोहा मानने योग्य है। कथा प्रसंग में वह कुछ देर बाद दिखाई देते हैं। परंतु फिर वह दृष्टि के सामने से नहीं हटते। पद्मसिंह एक साधारण समाज-सुधारक हैं। विचारों के बहुत ऊँचे हैं, हृदय के बहुत कोमल हैं, परंतु हैं दब्बू। ऐसे पुरुष लेख चाहे जितने लिख मारें, वक्तव्य चाहे जितनी झाड़ आएँ परंतु मौका पड़ने रहेंगे सबसे पीछे। नाच के बड़े विरोधी, परंतु मित्रों ने दबाया तो जलसा करा बैठे। इसका उन्हें बहुत प्रायश्चित भी करना पड़ा – न यह नाच होता और न सुमन घर से निकाली जाती। वह विट्ठलदास की शरण लेते हैं। परंतु उससे पद्मसिंह की नहीं बनती। जैसे वह कर्म में कच्चे हैं वैसे ही विट्ठल दास विचार में कच्चे हैं। चंदा वसूल करने में कठिनाई, वारांगनाओं को शहर के बाहर जगह देने के प्रस्ताव का म्यूनिसिपैलिटी के मेंबरों द्वारा विरोध, इधर घर में मदनसिंह की ज्यादती, उधर सुमन की बहन शांता के साथ मदन सिंह के विवाह में विघ्न पड़ने की चोट-पद्मसिंह बिलकुल ढीले पड़ गए। परंतु विचार शक्ति में कमी नहीं पड़ी। उन्हीं के द्वारा लेखक महाशय ने भी अपना विचार प्रकट किया है कि वीर-नारियों को निकाल देने से ही सुधार नहीं हो जाएगा। क्यों न उनको और उनकी संतान को अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया जाए? इस विचार को विट्ठलदास ‘सेवासदन’ के रूप में परिणित करते हैं। परंतु पद्मसंह के हृदय में अंत तक भय की सत्ता बनी रहती है। झेंप के मारे वह सेवासदन में नहीं जाते, कहीं ऐसा न हो जो सुमन से आँखें चार हो जाएँ।
ऐसे और भी अनेक पात्र हैं। परंतु लेख बढ़ जाने के भय से हम उसका वर्णन न करेंगे। सरल शांता को अनेक कष्ट सहन करके भी, अंत में सौभाग्यवती गृहिणी का सुख भोगना बदा था। चंचला परंतु पतिव्रता सुभद्रा, अनेक आपदाएँ झेलकर भी पति के सामने हँसती ही रहती है। गृहस्थ गजाधर के संन्यास-आश्रमी अवतार गजानंद, अंत में बहन के घर से निकाली हुई किसी समय की अपनी पत्नी को शोक-सागर से उबारकर शांति प्रदान करते हैं। पुराने विचार के देहाती रईस मदन सिंह नाच कराने में अपनी मर्यादा समझते हैं। दुलार से बिगड़े हुए नवयुवक मदन सिंह का पतन और अपनी ही मेहनत द्वारा उद्धार, म्यूनिसिपैलिटी के मेंबरों में से कोई गान-विद्या और हिंदी का शौकीन है, किसी को अंग्रेजी बोले बिना चैन नहीं, किसी के दुर्व्यसन वैसे ही हैं जैसे उसके दुर्विचार-इन सब के लिए उपन्यास में स्थान है, सबके चित्र देखने को मिलते हैं, सबसे किसी-न-किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त होता है।
उपन्यास के पात्रों से दृष्टि हटाकर यदि वह उसके उद्देश्य की ओर प्रेरित की जाए तो एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रश्न सामने आ जाता है। क्या वह ‘सेवा-सदन’ जिसकी झलक हम इस उपन्यास में देखते हैं, कभी प्रत्यक्ष देखना भी नसीब होगा? प्रश्न कठिन है। शहरों की आबादी दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है। इस काम को नगरपालिकाओं के भरोसे छोड़ देने से सफलता होने की नहीं। देखें, हमारी व्यवस्थापक सभाएँ इस प्रश्न को क्योंकर हल करती हैं। लेखक के विचार यदि उपन्यास के बहाने पाठक जनता पर कुछ भी असर करें तो समाज एक बुरे रोग से मुक्त हो जाए।
उपन्यास में दोष दिखाने के लिए बहुत कम स्थल हैं। मुसलमान पात्रों की उर्दू बहुत क्लिष्ट है। यदि सरल हो सकती तो बहुत अच्छा था। टिप्पणी में कठिन शब्दों के अर्थ ही लिख दिए जाते तो पाठकों को बहुत सुविधा हो जाती।