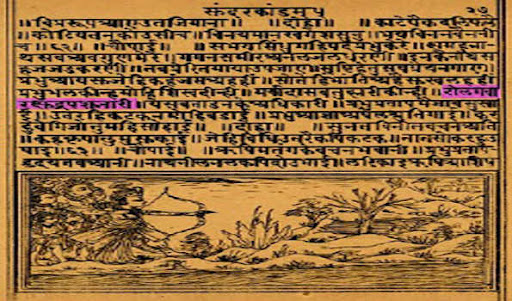प्राचीन काल में जब गद्य का उदय नहीं हुआ था तो कविता का नाम ही साहित्य था। हिंदी साहित्य के प्राचीन इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि साहित्य का अर्थ था ‘कविता’ जिसे समय-समय पर डिंगल’, ‘अवधी’ और ‘ब्रजभाषा’ में विविध शैलियों के अंतर्गत लिखा गया। साहित्य के विषय भी इने-गिने थे वीरगाथाएँ, भक्तिकाल में निर्गुण-भक्ति, सूफी प्रेम-साधना, राम कृष्ण भक्ति और रीति-काल में शृंगार साहित्य में न नाटक लिखे जाते थे और न कहानी और उपन्यास; न निबंध लिखे जाते थे और न ‘जीवनियाँ’ या और अन्य किसी विषय का साहित्य हो। इसलिए इस काल के कवि की सर्वांगीणता देखने के लिए हम उसकी कविता के सीमित क्षेत्र पर विचार करेंगे। ‘प्रसाद’ के काल की सर्वांगीणता पर नहीं।
गोस्वामी तुलसीदास का प्रादुर्भाव हिंदी साहित्य में सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में हुआ। तुलसीदास ने राम-भक्ति का विषय लेकर अपनी साहित्य-लहरी को प्रवाहित किया। जहाँ तक भाषा का संबंध है उस काल में ‘अवधी’ तथा ‘ब्रज’ यही दो भाषाएँ हिंदी की साहित्यिक भाषाएँ थीं। कविवर तुलसीदास का दोनों ही भाषाओं पर समान अधिकार था और दोनों ही भाषाओं को गोस्वामी तुलसीदास ने परिमार्जित और सुसंस्कृत रूप दिया। “हिंदी-काव्य का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले-पहल दिखाई दिया।” सधुक्कड़ी भाषा में साहित्य का सृजन न करके तुलसीदास जी ने भाषा का संस्कार किया और भाषा को उच्च कोटि के साहित्य के योग्य बनाया।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काल की प्रायः सभी प्रचलित शैलियों का अपने साहित्य में पूर्ण सफलता के साथ प्रयोग किया है। आपकी रचनाओं में जहाँ तक सौंदर्य, निपुणता और काव्यात्मकता का संबंध है वह शैली-निर्मा-ताओं से भी अधिक पाया जाता है। उस समय की प्रचलित काव्य-शैलियाँ थीं-
(1) वीरगाथाकाल की छप्पय पद्धति,
(2) विद्यापति और सूर की गीति-पद्धति,
(3) गंग इत्यादि भाटों की कवित-सवैया पद्धति,
(4) कबीरदास की नीति संबंधी दोहा-पद्धति और
(5) जायसी इत्यादि की दोहा चौपाई पद्धति।
इस प्रकार उस काल की यह पाँच प्रचलित शैलियाँ थीं, जिनमें कवि अपनी कविताएँ लिखकर साहित्य के भंडार को भर रहे थे। “तुलसीदास जी के रचना-विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपनी सर्वमुखी प्रतिभा के बल से सब के सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्यवाणी में दिखाकर साहित्यिक क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिंदी कविता के प्रेमी जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रजभाषा का जो माधुर्य हम सूर-सागर में पाते हैं वही माधुर्य और भी सुसंस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधी का जो मिठास हमें जायसी की ‘पद्मावत’ में मिलता है वही जानकी मंगल, पार्वती-मंगल, बरवै-रामायण और रामलला नहछू में मिलता है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधी पर अधिकार था ओर न जायसी का ब्रजभाषा पर।”
-आचार्य रामचंद्र शुक्ल
इस प्रकार हमने देखा कि तुलसीदास जी की सर्वांगीणता इस ऊपर दिए गए आधार से सर्वथा स्पष्ट हो जाती है। अभी तक हमने शैली और भाषा पर ही विचार किया है। जहाँ तक शैली और भाषा का संबंध है हम तुलसीदास जी को समस्त प्रगतियों में पूर्ण सफलता के साथ साहित्य का सुंदर और सुसंस्कृत रूप पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए पाते हैं। ब्रज और अवधी दोनों में रचना करने पर भी कभी भाषाओं में खिचड़ी हो जाने का दोष साहित्य में नहीं आ पाया है। साहित्यिक निर्मलता के साथ-साथ भाषा भी अत्यंत निर्मल है।
साहित्य के सब अंगों का समान अधिकारी महाकवि तुलसीदास, जीवन के सब अंगों से भी पूर्णतया परिचित था। जीवन के सभी पहलुओं पर कवि ने सुंदर रूप से प्रकाश डाला है। बाल-काल, यौवन और वृद्धावस्था का चित्रण हमें मानस में मिलता है। बालकांड में बाल-काल, अयोध्याकांड में दशरथ की वृद्धावस्था की दशा और यौवन का तो चित्रण आद्योपांत मिलता है। जीवन के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालने के साथ-साथ जीवन की विविध परिस्थितियों को भी कवि ने अपनी तूलिका द्वारा रंगा है। खेल विवाह, वन-गमन, मिलन, बिछोह, आनंद, कष्ट सभी भावनाओं का चित्रण कवि ने किया है। काव्य-शास्त्रों के प्रायः सभी गुण हमें तुलसीदास जी के साहित्य में मिलते हैं। नव-रसों पर आपने सुंदर रचनाएँ की हैं। आपने अनेकों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग अपनी रचना में किया।
हमने देखा कि भाषा, शैली और साहित्यिक दृष्टिकोण से महाकवि तुलसी दास का साहित्य सभी दिशाओं में पूर्णता की पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ है। अब साहित्य के विषय पर और विचार करना है। उस काल में साहित्य का विषय प्रधानतया भक्ति रहा है। भक्ति क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम भक्ति को अपनाया, परंतु राम भक्ति के साथ आपने सहिष्णुता से काम लिया और कृष्ण, शिव इत्यादि सभी के प्रति आदर प्रदर्शित किया है। इस प्रकार भारत के प्रचलित सभी धर्मों में आपने साहित्य द्वारा सम्मिलन की भावना को प्रचारित किया, जिससे भारत का जो हित हुआ उसे यहाँ नहीं लिखा जा सकता। तुलसीदास के साहित्य ने भक्ति क्षेत्र में जो कार्य किया वह जनसाधारण के दृष्टिकोण से वेद-शास्त्रों द्वारा किया भी प्रतीत नहीं होता।
इस प्रकार हमने पूर्ण रूप से परखकर देख लिया कि भाषा, शैली, काव्यात्मकता और विषय के आधार से तुलसीदास जी के साहित्य में पूर्ण रूपेण सर्वांगीणता पाई जाती है।