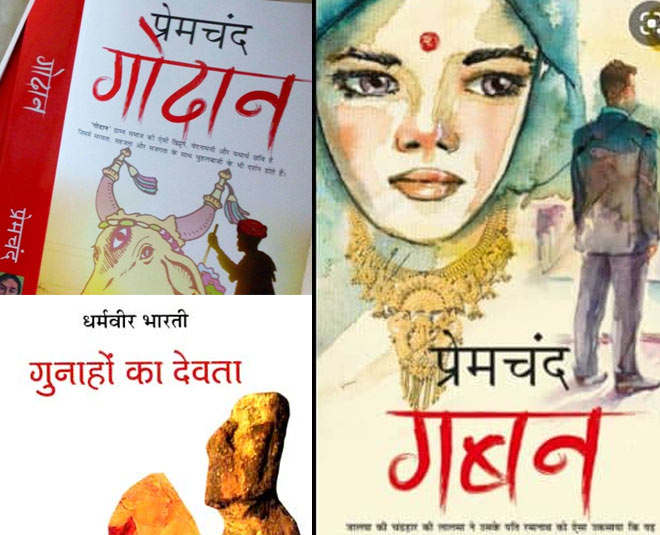उपन्यास की परिभाषा विद्वानों ने कई प्रकार से की है। कविता की परि-भाषा आज तक नहीं हो सकी। जितने विद्वान् हैं उतनी ही परिभाषाएँ हैं। किन्हीं दो विद्वानों की राय नहीं मिलती। उपन्यास के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। इसकी कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जिस पर सभी लोग सहमत हों। उपन्यास के विषय में मुंशी प्रेमचंद इस प्रकार लिखते हैं-
“मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व है।”
जैसे दो आदमियों की सूरतें नहीं मिलतीं, उसी भाँति आदमियों के चरित्र भी नहीं मिलते। यही चरित्र संबंधी समानता और विभिन्नता-अभिनय में भिन्नता और विभिन्नता में अभिन्नता दिखाना उपन्यास का मुख्य कर्त्तव्य है। हमारा चरित्राध्ययन जितना ही सूक्ष्म जितना ही विस्तृत होगा, उतनी ही सफलता से हम चरित्रों का चित्रण कर सकेंगे।
अब यहाँ प्रश्न उठता है कि उपन्यासकार को चरित्रों का चित्रण करके उनको पाठक के सामने रख देना चाहिए-उसमें अपनी तरफ़ से कांट-छाँट, कमी वेशी कुछ न करनी चाहिए, या किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चरित्रों में कुछ परिवर्तन भी कर देना चाहिए।
यहीं से उपन्यासकारों के दो वर्ग हो जाते हैं। एक आदर्शवादी वर्ग और दूसरा यथार्थवादी वर्ग।
यथार्थवादी चरित्रों को पाठक के सामने उनके यथार्थ नग्न रूप में रख देता है। उसे इससे कुछ मतलब नहीं कि सच्चरित्रता का परिणाम अच्छा होता है या कुचरित्रता का परिणाम बुरा-उसके चरित्र अपनी कमजोरियाँ दिखाते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। संसार में सदैव नेकी और बदी का फल बंद नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत हुआ करता है। नेक आदमी धक्के खाते हैं, यातनाएँ सहते हैं मुसीबतें झेलते हैं और अपमानित होते हैं। नेकी का फल उलटा मिलता है। बुरे आदमी चैन करते हैं, नामवर होते हैं। यशस्वी बनते हैं। उनको बदी का फल उलटा मिलता है। यथार्थवाद अनुभव की बेड़ियों से जकड़ा होता है और क्योंकि संसार में बुरे चरित्रों की ही प्रधानता है-यहाँ तक कि उज्ज्वल से उज्ज्वल चरित्र में भी कुछ दाग धब्बे रहते हैं, इसलिए यथार्थवाद हमारी दुर्बलताओं हमारी विषमताओं और हमारी क्रूरताओं का नग्न चित्र होता है और इस तरह यथार्थवाद हमको निराशावादी बना देता है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है और हमको अपने चरित्रों की बुराई नजर आने लगती है।
इसमें संदेह नहीं कि समाज की कुप्रथा की ओर उसका ध्यान दिलाने के लिए यथार्थवाद अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि इसके बिना, बहुत संभव है, हम उस बुराई को दिखाने में अत्युक्ति से काम लें और चित्र को उससे काला नहीं दिखाए जितना वह वास्तव में है, लेकिन जब वह दुर्बलताओं का चित्रण करने में शिष्टता की सीमाओं से आगे बढ़ जाता है, तो आपत्तिजनक हो जाता है। फिर, मानव स्वभाव की विशेषता यह भी है कि वह जिस छल और क्षुद्रता और कपट से घिरा हुआ है, उसी की पुनरावृत्ति उसके चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकती। वह थोड़ी देर के लिए ऐसे संसार में उड़कर पहुँच जाना जाता है, जहाँ उनके चित्त को ऐसे कुत्सित भावों से नजात मिले-वह भूल जाए कि मैं चिंताओं के बंधन में पड़ा हुआ हूँ; जहाँ उसे सज्जन, सहृदय, उदार प्राणियों के दर्शन हों; जहाँ छल और कपट, विरोध और वैमनस्य का ऐसा प्राधान्य न हो। उसके दिल में ख्याल होता है कि जब हमें किस्से-कहानियों में भी उन्ही लोगों से साबका है जिसके साथ आठों पहर व्यवहार करना पड़ता है, तब फिर ऐसी पुस्तक पढ़ें ही क्यों?
यथार्थवाद यदि हमारी आँखें खोल देता है, तो आदर्शवाद हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुँचा देता है। लेकिन जहाँ आदर्शवाद में यह गुण है वहाँ इस बात की शंका है कि हम ऐसे चरित्रों को न चित्रित कर बैठें जो सिद्धांतों की मूर्ति मात्र हों और जिनमें जीवन न हो। किसी देवता की कामना करना मुश्किल नहीं है लेकिन उस देवता में प्राण-प्रतिष्ठा करनी मुश्किल है।
इसलिए वही उपन्यास उच्च कोटि के समझे जाते हैं जहाँ यथार्थ और आदर्श दोनों का समावेश हो गया है। उसे आप आदर्शोंन्मुख यथार्थवाद कह सकते हैं। आदर्श को सजीव बनाने के लिए ही यथार्थ का उपयोग होना चाहिए और अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है।
“चरित्र को उत्कृष्ट और आदर्श बनाने के लिए यह जरूरी नहीं कि वह निर्दोष हो, महान् से महान् पुरुषों में भी कुछ न कुछ कमजोरियाँ होती हैं-चरित्र को सजीव बनाने के लिए उसकी कमजोरियों का दिग्दर्शन कराने में कोई हानि नहीं होती बल्कि यही कमजोरियाँ उस चरित्र को मनुष्य बना देती हैं। निर्दोष चरित्र तो देवता हो जाएगा और हम उसे समझ नहीं सकेंगे। उस चरित्र का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, केवल मनोरंजन मात्र हो सकता है। साहित्य का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ आत्म-परिष्कार भी है। साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। यह तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मसखरों का काम है। साहित्यकार हमारा पथ-प्रदर्शक होता है, वह हमारी मनुष्यता को जगाता है, हम में सद्भावों को भरता है और हमारी दृष्टि को फैलाता है।”
इस प्रकार मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यासों के दो भेद किए, एक यथार्थवादी और दूसरा आदर्शवादी। इन दो भेदों के अतिरिक्त भी उपन्यासों के अनेकों भेद और उपभेद होते हैं।
कथा प्रधान उपन्यास
कथा प्रधान उपन्यास में लेखक का ध्यान विशेष रूप से उपन्यास की कथा और घटनाचक्रों पर रहता है। वह पाठक को कथा के सौंदर्य में फँसाकर रखता है और उसी सौंदर्य से अपने उपन्यास को रोचक बनाने का प्रयत्न करता है। कथा का तारतम्य कहीं पर टूटने नहीं देता। जासूसी उपन्यासों में विशेष रूप से यह सौंदर्य मिलता है। इन उपन्यासों में घटनाओं का जमाव इतना रोचक और सुव्यवस्थित होता है कि पाठक एक बार कथा प्रारंभ करके फिर समाप्त करने से पूर्व छोड़ नहीं सकता। यह उपन्यास का प्रकार भी है और एक गुण भी इन उपन्यासों में घटनाओं की जादूगरी के लिए ही प्रधान स्थान रहता है। जीवन पर इन उपन्यासों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और यदि पड़ता भी है तो यह उपन्यास व्यसन के ही रूप में पड़ता है। क्योंकि जीवन के रहस्य के विषय में वह कुछ कहते ही नहीं हैं।
चरित्र-चित्रण-प्रधान उपन्यास-
चरित्र-चित्रण-प्रधान उपन्यासों में कथा और घटनाओं पर विशेष जोर न देकर चरित्र-चित्रण पर विशेष बल दिया जाता है। इन उपन्यासों में जीवन की समस्याओं को लेकर लेखक चलता है और उन्हीं के आधार पर चरित्रों का निर्माण करता है। उसके पात्र समाज के चरित्रों के प्रतीक बनकर चलते हैं और इस रूप में वह न केवल देश और समाज का ही वरन् मानव जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेखक अपने पात्रों में वह जीवन भरता है जिसकी मानव समाज को आवश्यकता होती है और साथ-साथ उन्हें उन पात्रों के साथ रखता है जिनके कारण समाज दूषित है, कलुषित है और निन्दित है। चरित्र चित्रण-प्रधान उपन्यासकार के सम्मुख एक बड़ा भारी उत्तरदायित्व रहता है और चरित्र चित्रण में जितनी स्वतंत्रता एक उपन्यास-कार को है उतनी अन्य किसी भी साहित्यकार को नहीं है। नाटककार, निबंध-कार, काव्यकार, कवि कोई भी इतनी स्वतंत्रता से अपने पात्रों का चित्रण नहीं कर सकता जितना एक उपन्यासकार। इसलिए उपन्यास का चरित्र चित्रण सबसे पूर्ण रहता है। इस कोटि के उपन्यास सबसे उत्तम कोटि के उपन्यास कहलाते हैं।
सामाजिक उपन्यास
सामाजिक उपन्यासों में समाज के यथार्थवादी चरित्र उपन्यासकार प्रस्तुत करता है। देश और समाज के हित के लिए ऐसे उपन्यास-कार हितकर सिद्ध होते हैं और ऐसे उपन्यासकारों को समाज में प्रसिद्धि भी अधिक मिलती है। इस प्रकार के उपन्यासों में क्योंकि समाज को अपने चित्र देखने को मिलते हैं इसलिए उसे सबसे अधिक प्रिय इसी प्रकार की रचनाएँ होती हैं। चरित्र चित्रण भी लेखक कई प्रकार से करते हैं। एक तो केवल ऊपरी परिस्थितियों को लेकर वर्णनात्मक रूप से करते हैं और दूसरे मनोवैज्ञानिक रूप से करते हैं। मूं० प्रेमचंद के उपन्यासों में मनोवैज्ञानिकता न मिलकर वर्णना-त्मकता अधिक मिलती है। आज के उपन्यासकारों में मनोवैज्ञानिकता दिन-प्रतिदिन बढती जा रही है।
ऐतिहासिक उपन्यास-
ऐतिहासिक उपन्यास कथा-प्रधान भी हो सकते हैं और चरित्र चित्रण प्रधान भी इन उपन्यासों में पात्र और कथा इतिहास में से ली जाती हैं। ऐतिहासिक कहने का अर्थ यह नहीं होता है कि उनमें इतिहास के आधार पर कोरी कथा मात्र का वर्णन होता है। उपन्यासकार अपनी कल्पना के आधार पर इसमें रोचकता पैदा करने के लिए उलट-फेर भी कर सकता है, परंतु वह उलट-फेर इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि जिससे प्रधान तथ्यों का अनुमान गलत लगने लगे। हिंदी में श्री वृंदावनलाल वर्मा ने इस प्रकार के सुंदर उपन्यास लिखे हैं।
इस प्रकार हमने उपन्यास साहित्य पर विचार किया और उपन्यास को किन-किन वर्गों में बाँटा जा सकता है इस भी विचार किया। चरित्र चित्रण का उप-न्यास में अन्य सभी प्रकार के साहित्य से अधिक क्षेत्र है, इसलिए जीवन की जितनी सुंदर विवेचना उपन्यास में हो सकती है उतनी न प्रबंध-काव्य में हो सकती है और न नाटक या मुक्तक कविता में निबंध और कहानी के तो क्षेत्र हो बहुत सीमित होते हैं इसलिए मानव जीवन की विवेचना का उपन्यास सबसे अच्छा और व्यापक माध्यम है।